-प्रकाशक
कर्म का मूलाधार
प्रश्न- कर्म के सिद्धान्त का मूलाधार क्या है ?
उत्तर- कर्म का सिद्धान्त दो दार्शनिक सिद्धान्तों पर आधारित है। प्रथम जीव कर्म करने में स्वतन्त्र और फल पाने में अपने कर्म के आश्रित है । दूसरा फल का दाता ईश्वर है, जो अपनी व्यवस्था के अनुसार जीव के किये हुए कर्मों के अनुपात से फल देता है ।
प्रश्न- संसार में बहुत से लोग हैं, जो कर्म के सिद्धान्त को भूल-भूलैयाँ कहते हैं और उस पर विश्वास नहीं रखते ।
उत्तर-मूल सिद्धान्तों से कोई इनकार नहीं करता सब मानते हैं कि जो जैसे कर्म करता है वह वैसा फल पाता है । नास्तिक से नास्तिक लोग भी सदाचार की इस मौलिक भित्ति का निषेध नहीं करते । यदि यह सिद्धान्त न माना जाय संसार का एक क्षण भी काम नहीं चल सकता हाँ शाखारूप में जो प्रश्न उठ खड़े होते हैं, उन प्रश्नों का भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न उत्तर देते हैं कुछ लोगों ने कुछ कल्पित धारणाएं बना रखी हैं। वे धारणाएं उनको ठीक सोचने में सहायता नहीं देतीं । अर्थात् यदि किसी ने पहले से यह मान रखा है कि ईश्वर नहीं है या जीव अजर, अमर या अजन्मा नहीं है या पुनर्जन्म नहीं होता तो इन कल्पनाओं की उपस्थिति में उसके आगे कर्म के सिद्धान्त को मानने में बाधा पड़ेगी परन्तु फिर भी उसे इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शुभ कर्म का फल अच्छा होता है और अशुभ का बुरा । सम्भव है कि शुभ-अशुभ कर्मों के लक्षणों में वह भेद करे, परन्तु कर्म-फल के मौलिक सिद्धान्त तो सर्वतन्त्र ही हैं। एक नास्तिक भी अपने पुत्र को खोटे कर्म करने पर सज़ा देता है और कहता भी है कि “तूने अपराध किया । तुझ को दण्ड मिलेगा ।" यह भी तो कर्म-फल ही है ।
ईश्वर न्यायकारी और दयालु है
प्रश्न-ईश्वर न्यायकारी है या दयालु ? और उसकी दया या न्याय का कर्म के सिद्धान्त से क्या सम्बन्ध है ?
उत्तर-ईश्वर न्यायकारी है, क्योंकि ईश्वर जीव के कर्मों के अनुपात से ही उनका फल देता है-न्यून या अधिक नहीं । परमेश्वर दयालु है, क्योंकि कर्मों के फल देने की व्यवस्था इस प्रकार की है जिससे जीव का हित हो सके । शुभ कर्मों का अच्छा फल देने में भी जीव का कल्याण है और अशुभ कर्मों का दण्ड देने में भी जीव का ही कल्याण है। इसलिये कर्म-फल का सिद्धान्त ईश्वर को दयालु भी प्रमाणित करता है और न्यायकारी भी । दया का अर्थ है जीव का हितचिन्तन । और न्याय का अर्थ है उस हितचिन्तन की ऐसी व्यवस्था करना कि उसमें तनिक भी न्यूनता या अधिकता न हो ।
इसको दूसरे प्रकार से सोचिये। यदि जीव के कर्मों की अपेक्षा अधिक फल दिया जाय तो जीव में आलस्य और प्रमाद बढ़ेगा। इससे जीव का अनिष्ट होगा। यह दया न होगी और न न्याय । क्योंकि इससे जीव का अहित होगा। जिस काम का परिणाम अहित हो, वह न तो दया है और न न्याय । अमुक कर्म का कितना फल होना चाहिये, इसका ठीक-ठीक परिगणन न्याय है और इस परिगणन का उद्देश्य जीव का हित है, यह है दया। न्यायाधीश दया से प्रेरित होकर न्याय करता है । वह समझता है कि यदि न्याय न करूंगा तो अहित होगा । यह अहित ही निर्दयता है ।
दुःख व सुख दोनों ही हितकर
कल्पना कीजिये कि एक परीक्षक परीक्षार्थी को उसके कर्मों से अधिक अंक देता है । मूर्ख लोग इसको "दया" कहेंगे । परन्तु प्रथम तो यह अन्य परीक्षार्थियों के साथ अन्याय है और उनके साथ निर्दयता भी। दूसरे इस परीक्षार्थी के साथ भी निर्दयता हुई, क्योंकि उसका स्वभाव बिगड़ गया । ईश्वर दयालु भी है और न्यायकारी भी। इसलिये वह कर्मों का फल उनके अनुपात से ही देता है, कम या अधिक नहीं ।
प्रश्न-परमात्मा दयालु होकर भी असह्य दुःखों को क्यों देता है ?
उत्तर-दयालु ईश्वर प्रिय जीव को अशुभ कर्मों से छुड़ाना चाहता है । जब दुःख असह्य हो जाते हैं तो जीव को मूर्च्छा आ जाती है । मूर्च्छा में असह्य से असह्य दुःख सह्य हो जाते हैं परन्तु दुःखों की विद्यमानता अशुभ कर्मों को छुड़ाने में सहायक होती । दुःख और सुख दोनों आत्म-विकास पर प्रभाव डालते हैं। यद्यपि यह प्रभाव बहुधा अदृष्ट और अमीमांसनीय रूप में होता है। इसको आप एक मोटे उदाहरण से जान सकते हैं। याद रखिये कि उदाहरण मोटा है । इसको इतना ही समझिये । शरीर में स्वस्थता और रोग दोनों ही जन्म के आरम्भ से ही लगे रहते हैं। इन दोनों का शरीर के विकास पर प्रभाव पड़ता है । स्वस्थता अपनी शैली शरीर का विकास करती है और रोग अपनी शैली से अनिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने में सहायक होते हैं। स्वस्थता और रोग दोनों ही शारीरिक विकास के लिये आवश्यक हैं। ऐसे ही सुख दुःख के ऊपर घटाइये ।
ईश्वर की व्यवस्था
प्रश्न जब समस्त सृष्टि ईश्वर की व्यवस्था के आधीन है और हम सब भी सृष्टि के अंग हैं तो सत्यासत्य कर्त्तव्याकर्त्तव्य, कर्म और भोग की विवेचना की उलझनों में क्यों पड़ना ? होगा तो वही जो ईश्वर की व्यवस्था के भीतर है ।
उत्तर-ईश्वर की व्यवस्था जड़ और चेतन के लिए एक सी नहीं है, सृष्टि की जटिलतम समस्या यह है कि जड़ और चेतन में भेद किया जाये । ईश्वर की व्यवस्था जहाँ जड़ चीज़ों पर पूरा आधिपत्य रखती है वहाँ चेतन चीज़ों को अपने कर्म क्षेत्र में पूरी पूरी स्वतन्त्रता भी है । सृष्टि के निर्माण में चेतन शक्तियों का पूरा पूरा साझा है । नैसर्गिक शक्तियों का चेतन शक्तियाँ निर्वचन पूर्वक प्रयोग किया करती हैं। चीटियों के चिटोंहर, बया के घोंसले, भेड़ियों की मांदें, और सहस्रों अन्य जीवों की बनाई हुई चीज़ें यही बताती हैं कि चेतन जीव ईश्वर-नियन्त्रित नियमों का निरन्तर विवेचना पूर्ण उपयोग किया करते हैं और सृष्टि में परिवर्तन किया करते हैं। सभ्य जातियों के नगर, सड़कें आदि इस बात की सूचना देते हैं कि जिस सृष्टि में हम रहते हैं वह केवल ईश्वर निर्मित ही नहीं है उसमें मनुष्य तथा अन्य प्राणियों का भी साझा है। बया जो घोंसला बनाती है उसमें घोंसला निर्माण की कला चाहे कितनी ही स्वाभाविक और स्वतन्त्रता शून्य अथवा शिक्षानपेक्षित क्यों न हो उसकी सामग्री के जुटाने आदि में पक्षी को पर्याप्त निर्वाचन करना पड़ता है। अतः जीव की कर्म करने में स्वतन्त्रता सुरक्षित है। सृष्टि के प्रयोजन ही दो हैं। जीव का भोग और जीव का कर्म । सृष्टि इन दोनों प्रयोजनों के लिये सर्वथा उपयुक्त है। भोग का परिणाम है बौद्धिक विकास । उस विकास का प्रभाव पड़ता है कर्त्तव्यता के निर्वाचन पर । उससे उत्पन्न होते हैं कर्म । कर्म के अनुकूल होता है भोग। यह शृङ्खला कल्पित नहीं है अपितु सहज ही में जानी जा सकती है । बच्चा उत्पन्न होते ही भोग पाता है। भोगों से उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसी के अनुसार यह निर्वचन करके कर्तुम्, अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं की स्वतन्त्रता का प्रयोग करता है, हर कर्म पीछे से भोग उत्पन्न करता है । उस भोग से आगे का विकास होता है । यह चक्र कभी बन्द नहीं होता, हम केवल इस चक्र से घबड़ाने या उस पर विश्वास न करने या उसकी ओर से आँख मूंद लेने मात्र से इस चक्र से छुटकारा नहीं पा सकते। हाँ इस चक्र को समझकर यदि हम ठीक रीति से अपने कर्त्तव्यों का पालन करें तो अवश्य ही हमारी उन्नति हो सकती है। परिस्थितियाँ कितनी ही निश्चित क्यों न हों उस निश्चितता के भीतर भी जीव की स्वतन्त्रता की गुञ्जाइश है। जेल में कैदी पूर्ण रूप से कैदी है फिर भी कैदी को कैद में करने के लिये जो काम दिया जाता है उसके करने में वह अपना विवेक प्रयुक्त कर सकता है। अच्छा करने पर अधिकारी सन्तुष्ट रहते हैं। अन्यथा उनकी अप्रसन्नता होती है और कभी कभी दण्ड भी प्राप्त होता है। अतः सिद्ध है कि जेल का कैदी भी कर्म करने में स्वतन्त्र और भोग में परतन्त्र है। स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्य की सीमाएं अवश्य भिन्न हैं और होनी भी चाहिये क्योंकि यह भी तो कर्मों का फल है । श्रेष्ठ पुरुषों को लोक में भी निकृष्ट लोगों की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता रहती है। पुलिस चोर पर दृष्टि रखती है साह पर नहीं, ये सब मानवी कार्य नैसर्गिक नियमों का अनुकरण मात्र हैं ।
जीव को बनाया ही क्यों ?
प्रश्न- परमात्मा ने ऐसा जीव क्यों बनाया जो कर्म करने में स्वतन्त्र है ? यदि हम को यह आज़ादी न होती तो हम पाप न करते और दुःखरूपी फल के भागीदार न होते ।
उत्तर-आपने अधूरी बात सोची । यदि स्वतन्त्र न होते तो पुण्य भी न करते और सुख भी नहीं मिलता। परीक्षार्थी स्वतन्त्र होता है तभी तो अच्छा परचा करने पर पुरस्कार पाता है अन्यथा पुरस्कार कैसा ? दूसरी सोचने और याद रखने वाली बात यह है कि कर्मवाद जीव को ईश्वर द्वारा उत्पन्न नहीं मानता । यदि ईश्वर ने जीव को बनाया होता तो बीसियों उल्झनें उत्पन्न हो जातीं अर्थात् जीव के अस्तित्त्व, उसके कर्मों, उसके स्वातन्त्र्य आदि का उत्तरदायित्व केवल ईश्वर के ही सिर होता । ईश्वर ने हम को पाप करने में सशक्त बनाया ही क्यों ? यदि ईश्वर हमारी जीभ को ऐसा बनाता कि वह सच्च बोलने के लिये ही खुलती, झूठ के लिये खुलती ही नहीं, तो हम झूठ बोल ही न सकते ।
प्रश्न- आपने तो ग़ज़ब कर दिया । क्या जीव ईश्वर का बनाया नहीं ? यह तो ईश्वर पर दोष लगाना है ।
उत्तर- गजब नहीं । तथ्य यही है । किसी युक्ति से इससे भित्र बात सिद्ध नहीं होती । यदि ईश्वर जीव को बनाता तो दोषी ठहरता । क्योंकि यह समस्त सृष्टि उसके बनाये हुए जीवों के लिये होती । प्रश्न होता कि जीव को बनाया ही क्यों ? अपने लिये या अन्य के लिये। अन्य कोई था नहीं अत: अपने लिये तो ईश्वर स्वार्थी सिद्ध होता । जो ऐसा मान बैठे हैं (बहुत से आस्तिक इसी भ्रम में हैं) । वे यह नहीं बता सकते कि ईश्वर ने ऐसी दुःखमयी सृष्टि क्यों बनाई ? इसी प्रकार जो लोग जीव को ईश्वर का केवल अंश मात्र मानते हैं वह भी कर्मवाद पर पूर्ण विचार नहीं करते । जीव को ईश्वर का अंश मानना तो ईश्वर को अखण्ड और अखण्डनीय मानने से इनकार करना है। यह दोष ईश्वर पर लागू होगा। ईश्वर का एक अंश पाप करे और दूसरा उसको दण्ड दे । बेटे ने दवात की स्याही फैला दी। बाप ने उसके चाँटा मारा। दोनों ही ईश्वर के अंश थे । ऐसी काल्पनिक बात तो कल्पना मात्र है । हम को वर्तमान सृष्टि की बात सोचनी चाहिये । काल्पनिक सृष्टि की नहीं।
प्रश्न- आपकी यह बात विचित्र सी लगती है ।
फिर सृष्टि की उत्पत्ति किसके लिये ?
उत्तर-विचित्र सी इसलिये लगती है कि लोगों ने विचित्र विचित्र कल्पनाएं कर रखी हैं। ये वातावरण में फैली हुई हैं। अत: उनसे भिन्न तथ्य को लोग विचित्र कहते हैं। आप सोचिये और शास्त्र का अध्ययन कीजिये तो आप सत्यता को जान सकेंगे । हम तो ऐसी बात कह रहे हैं जिसको आप युक्तियों के आधार पर सोच सकते हैं ।
क्या केवल एक ही सत्ता मानकर आप इस प्रपंच की व्याख्या कर सकते हैं। यदि आप अपनी सृष्टि बनाना चाहें तो जिस प्रकार हो सके अपने मन की सन्तुष्टि कर लें परन्तु यदि इस वर्तमान सृष्टि के मूलाधार में जो तत्त्व हैं उनकी खोज करना चाहते हैं तो आपको इस परिणाम पर पहुँचना पड़ेगा कि जीव एक अनादि अजन्मा सत्ता है । उसी के लिये सृष्टि रची जाती है। यदि जीव अल्पज्ञ न होता तो भी सृष्टि की आवश्यकता न होती । यदि अनादि न होता तो न जीव के निर्माण की आवश्यकता थी न सृष्टि की । यदि सर्वज्ञ ईश्वर न होता तो सृष्टि को जीवों की आवश्यकताओं की अपेक्षा से बनाता कौन ? अन्यान्य धर्म वालों ने जो ईश्वर से इतर किसी सत्ता को अनादि और अमर मानना ईश्वर का अपमान समझते हैं ईश्वर का स्वरूप भी अपने मन से घड़ा और सृष्टि का स्वरूप भी । अपने स्वरूप को तो वह भूल ही गये। उन्होंने ईश्वर-विश्वास के अत्युक्ति-पूर्ण अभिमान में यह भी न सोचा कि यदि हम न हुए तो धर्म की किसको और क्या आवश्यकता ? यदि मैं स्वतन्त्र अजर अमर और अजन्मा आत्मा नहीं तो अध्यात्म का क्या अर्थ ? जो लोग कर्मवाद में उलझनें पाते हैं वे इसी कारण कि उन्होंने जीव के अजरत्व और अमरत्व को नहीं समझा । यदि जीव की उत्पत्ति मान ली जाये तो उत्पत्ति का सहचर सुख या दुःख बिना किसी कर्म या कारण के प्राप्त हुआ मानना पड़ेगा। इससे कर्म-फलवाद की जड़ कट गई तो भविष्य में सदाचार की भी जड़ कट जायेगी। फिर शुभाशुभ का कोई आधार ही न रहेगा। सत्यं शिवं सुन्दरम् का न कोई स्वरूप रहेगा न आधार । ईसाई मुसलमान आदि धर्मों में यूनानी दर्शनकारों के अनुकरण से जीव को अनित्य और उत्पत्ति वाला मान लिया गया। इसके दुष्परिणाम यह हुए कि जीव की स्वतन्त्रता नष्ट हो गई। जीव ईश्वर के हाथ का खिलौना बन गया सृष्टि उत्पत्ति के लिये कोई युक्तियुक्त कारण नहीं रहा। ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है ऐसा मान लिया गया, फिर भी अपने कर्मों द्वारा सृष्टि उत्पत्ति तथा शुभाशुभ के पचड़े से छूट न पाये और मनघड़न्त युक्तियों से समाधान करना पड़ा । यह भी समाधान न था अपितु तसल्ली मात्र थी। न तो कर्म-फलवाद माने बिना आचार-शास्त्र की नींव सुदृढ़ हो सकती है और न जीव को अनादि और कर्म करने में स्वतन्त्र माने बिना कर्म-फलवाद की पुष्टि हो सकती है ।
क्या ईश्वरेच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता ?
प्रश्न- कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता ।
उत्तर-पत्ता हिले या न हिले परन्तु झूठे की जीभ तो बिना ईश्वर की इच्छा के ही हिल जाती है। यदि ईश्वर की इच्छा से ही झूठा झूठ बोलता हो तो उसको झूठ बोलने का पाप क्यों लगे ? यदि एक चोर किसी के बाग में चोरी करने जाय और आम के वृक्ष को हिलाकर आम तोड़ लावे तो आम के समस्त पत्ते भी ईश्वर की इच्छा के बिना हिल सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि पत्ते आदि जड़ चीजें स्वयं नहीं हिलतों किसी न किसी चेतन मनुष्य, पशु, पक्षी के हिलाने से हिलती हैं, तथापि यह कहना ठीक नहीं कि कोई पत्ता बिना ईश्वर की प्रेरणा या इच्छा के नहीं हिलता। जब कोई जड़ वस्तु किसी अन्य चेतन की प्रेरणा के बिना हिलती पाई जाय, तब समझ लेना चाहिये कि यह ईश्वर की प्रेरणा से हिली है ।
प्रश्न- यदि चेतन क्षुद्र जीव ईश्वर की प्रेरणा के विरुद्ध भी चीज़ों को हिला डुला सकते हैं तो ईश्वर की व्यवस्था कहाँ रही? उत्तर-इससे ईश्वर की व्यवस्था में बाधा नहीं पड़ती। हम पहले इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है कि किसी जीव के उचित स्वातन्त्र्य में बाधा न पड़े। यदि जीवों का उचित स्वातन्त्र्य बाधित हो गया तो मानो न्याय व्यवस्था भी नष्ट हो गई और यह सृष्टि कर्म-क्षेत्र न रहकर कठपुतली का खेल हो गया ।
प्रश्न- आपने 'उचित' स्वातन्त्र्य क्यों लिखा ? क्या अनुचित स्वातन्त्र्य भी होता है ? और क्या ईश्वर की व्यवस्था 'अनुचित' स्वातन्त्र्य को घटने नहीं देती ?
उत्तर- हाँ स्वातन्त्र्य अनुचित भी हो सकता है। उसको स्वातन्त्र्य न कहकर उच्छृङ्खलता या अनियन्त्रण अथवा अनियमता कहते हैं । इसका एक स्थूल उदाहरण देश के राजनीतिक शासन में दृष्टिगोचर होता है। हर शासन में जनता को कुछ न कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त है परन्तु ऐसे भी लोग हैं जो शासन भंजक (Lawless) हैं और उनको दण्ड मिलता है अथवा उनकी स्वतन्त्रता छीन ली जाती है। इसी नियम को सृष्टि के साथ भी लागू कर सकते हैं ।
जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है और फल पाने में परतन्त्र
प्रश्न-जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है और फल पाने में परतन्त्र है, इसका क्या अर्थ है ।
उत्तर- इसका अर्थ यह है कि किसी काम के करने में जीव को पूर्ण अधिकार है कि उसे करे, या न करे या उलटा करे । मैं बोलूँ या न बोलूँ या अपशब्द बोलूँ । इन तीनों बातों का मुझे अधि कार है, परन्तु जब बोल चुका तो काम हो चुका । परिस्थिति मेरे हाथ से निकल गई। उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। यदि मुझे कोई बात कहनी चाहिये थी और मैं समय आने पर चुप रहा तो भी मुझे उसकी हानि भोगनी पड़ेगी। यदि मैं झूठ बोला या किसी को गाली दे दी तो उसका भी दुष्परिणाम भोगने में मैं परतन्त्र हूँ । काम की पूर्ति के पहले तो मेरा अधिकार था । अब जगत् के व्यवस्थापक के हाथ में चला गया। मैं सर्वथा परतन्त्र हूँ । गीता में यही कहा है कि-
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्म-फलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥
अर्थात् मनुष्य का कर्म करने का अधिकार है। कर्म ज्यों ही समाप्त हुआ, उसका फल कर्म करने वाले के हाथ से निकल ईश्वर की व्यवस्था का अङ्ग बन जाता है। आपको अधिकार है कि आप आम बोवें या जामुन परन्तु जब आप बो चुके तो जगत् नियन्ता की व्यवस्थानुसार आम के बीज से आम के ही अंकुर, आम के ही पत्ते, आम के ही फूल और आम के ही फल निकलेंगे, जामुन के नहीं । आप तो काम करने पश्चात् ही परतन्त्र हो जाते हैं। अतः आपको चिन्ता उसी समय तक करनी है, जब तक काम समाप्त नहीं हुआ । उसके पश्चात् कर्मफल की चिन्ता व्यर्थ है। आम का बीज बोकर बीच में जामुन के पत्तों की इच्छा निरर्थक है । इसलिये न तो कर्म-त्याग से काम चलता है और न कर्म के पश्चात् फल की चिन्ता से । कर्त्तव्य का न करना भी अशुभ है और उलटा करना भी अशुभ ।
प्रश्न-मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र तो नहीं है। जगत् के बनाने वाले ने मनुष्य को परिस्थितियों से इतना जकड़ दिया है कि उनके विरुद्ध मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। अतः मनुष्य को 'स्वतन्त्र' कहना मिथ्या है। हम को व्यर्थ ही स्वतन्त्र कह कर हमारे कर्मों के लिये दण्ड दिया जाता है। मनुष्य प्रपंच के हाथ में खिलौना है। हम दैव के हाथ की कठपुतली हैं। वह जैसे चाहे नाच नचावे।
जीव कठपुतली नहीं--
उत्तर-यह ठीक नहीं । आप थोड़ा सा अपने जीवन पर विचार कीजिये । क्या कभी आप के मन में किसी काम के करने की भावना उठती है ? क्या कभी आप के हृदय में यह प्रश्न उठता है कि मैं अमुक काम करूं या न करूँ ? और क्या आप परिणामों पर विचार करके बुद्धि से तोल कर यह निश्चय नहीं करते कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा न करूंगा ? यदि ऐसा करते हैं तो सिद्ध है कि आप कर्म करने में स्वतन्त्र हैं। आप के समक्ष एक ही मार्ग नहीं अनेक मार्ग हैं और उनमें से निर्वाचन करके केवल एक ही मार्ग को ग्रहण करते हैं और शेष को छोड़ देते हैं ।
प्रश्न-आप तो स्वतन्त्रता और परतन्त्रता दोनों से चिपटे हुए हैं या तो यह मानिये कि संसार की समस्त चीजें किसी नियन्ता के वश में हैं, उसके विरुद्ध पत्ता भी नहीं हिल सकता या यह मानिये कि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है। दो परस्पर विरोधी बातें कैसे ठीक हो सकती हैं ?
उत्तर-जिनको आप परस्पर विरोधी बातें कहते हैं वह परस्पर विरोधी हैं नहीं । केवल समझ का फेर है । मित्रता और विरोध के अर्थों में भेद है। पीलापन और लाली परस्पर विरुद्ध नहीं परन्तु अंधेरा और उजाला परस्पर विरुद्ध हैं। जहाँ और जब उजाला होगा अंधेरा न होगा । इसी प्रकार जीव की स्वतन्त्रता की सीमा है और ईश्वर के नियन्त्रण की भी सीमा है ज़रा सा विचार कीजिये । आप बोलते हैं, आपकी जीभ आपके आधीन है, आप उस जीभ से शुभ और अशुभ दोनों बोल सकते हैं। कभी आजमा लीजिये। ईश्वर का जीभ पर इतना नियन्त्रण है कि आप उससे स्वतन्त्रता पूर्वक काम ले सकें । जीभ पर आपका तो कोई नियन्त्रण नहीं । आपने उसे बनाया नहीं न आपके हाथ में है कि उस जीभ में कोई दोष आ सके। फिर भी वह आपकी जीभ है। आप उसको अपनी इच्छा के अनुसार प्रयुक्त कर सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि आप किसी सीमा तक ईश्वर के नियन्त्रण में हैं और किसी सीमा तक स्वतन्त्र हैं। यह स्वातन्त्र्य आपकी स्वयम् अनुभूति है आपकी कल्पना नहीं। एक उदाहरण लीजिये-एक नदी है। उस पर पुल बंधा हुआ है। उस पुल के दोनों तरफ आदमी के कद के बराबर ऊँची बाड़ लगी हुई है । आप चलने में स्वतन्त्र भी है और परतन्त्र भी । उन बाड़ों के बीच आप मज़े से चल सकते हैं दौड़ सकते हैं परन्तु बाड़ों को पार नहीं कर सकते। जिसने पुल बनाया उसने आपको एक सीमा तक स्वतन्त्रता दी । उसके बाहर परतन्त्र कर दिया। यह सब आपकी भलाई को दृष्टि में रख कर किया गया । इसी प्रकार नियन्ता ने भी सृष्टि की ऐसी व्यवस्था कर दी कि आपके स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्य दोनों की सीमा बनी रहे। यह नियन्ता की बुद्धिमत्ता और कल्याण का सूचक है। आप सर्वथा परतन्त्र होते तो आपका विकास न होता। आपको अपनी बुद्धि के प्रयोग का केई अवसर न मिलता ? यदि आप सर्वथा स्वतन्त्र होते तो आप बुरा काम करके भी भला फल चाहते। दूसरी बात यह है कि जीव एक नहीं है । सब को पूर्ण स्वतन्त्रता देना कल्पना मात्र है एक की स्वतन्त्रता दूसरे की परतन्त्रता का कारण हो जाती है। सड़क पर यदि सभी यात्री पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें और उसका प्रयोग करने लगें तो एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी से टकरा जाये अतः स्वतन्त्रता की सीमा भी होती है ।
एक और उदाहरण लीजिये । परीक्षार्थी परीक्षा में बैठा हुआ है । प्रश्न-पत्र और उत्तर-पत्र उसके हाथ में है। वह स्वतन्त्र है कि किसी प्रश्न का जो चाहे उत्तर दे परन्तु दूसरे परीक्षार्थी से बात नहीं कर सकता, स्वतन्त्र भी है और परतन्त्र भी । स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्य की सीमाएं हैं। ये दोनों बातें परीक्षार्थी के हित को दृष्टि में रख कर नियत की गई हैं। परीक्षार्थी जो लिखेगा उसका फल अंक रूप में पाने में वह परतन्त्र है, परन्तु परीक्षा का समय भी नियत सीमा के भीतर है। आप क्या कहेंगे परीक्षार्थी पूर्णतया स्वतन्त्र है या पूर्णतया परतन्त्र ? दोनों में से एक भी नहीं। जब जीव अनेक हैं तो वे पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं हो सकते । हाँ केवल एक दशा में हो सकते हैं । अर्थात् जब उन जीवों का विकास इतना उच्चतम हो जाये कि वह तन्त्र या नियम को स्वयं समझने लगें और उनका उल्लंघन करें ही नहीं। यदि सब परीक्षार्थी अत्यन्त विश्वासपात्र हो जाएं तो निरीक्षकों की आवश्यकता न पड़े । यदि सभी जीव पूर्ण ज्ञानी या मुक्त हो जाए तो किसी को किसी से न रहे । यदि सभी नागरिक पूर्ण शिक्षित और विचारशील हो जाए तो सड़कों की मोड़ों पर पुलिस के पहरे की आवश्यकता न हो। फिर तो सृष्टि की ही आवश्यकता न पड़े परन्तु जिस सृष्टि की हम विवेचना कर रहे हैं उसमें अल्पज्ञ जीव हैं जो विकास के भित्र-भित्र स्तरों पर हैं, अतः उनको स्वतन्त्रता और परतन्त्रता की भी सीमाएं हैं और वे सीमाएं कर्मवाद को पुष्ट करती हैं उनको काटती नहीं ।
प्रश्न- स्वतन्त्रता कब उचित होती है कब अनुचित ?
उत्तर- सृष्टि निर्माण का उद्देश्य जीवों का विकास है। विकास के लिये ऐसी परिस्थिति चाहिये जिसमें जीव अपनी बुद्धि को लगा सके । अर्थात् जिसमें उसे यह सोचने का अवसर मिले कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये । यदि मनुष्य अपनी इस स्वतन्त्र बुद्धि को यथेष्ट रीति से प्रयुक्त करता है तो उसकी परिस्थिति शनैः शनैः विशद होती जाती है। परन्तु यदि वह बुद्धि को निकृष्ट रीति से प्रयुक्त करता है तो स्वतन्त्रता तो रहती है परन्तु वह स्वातन्त्र्य परिस्थिति को नित्य प्रति दूषित करता रहता है । इस सृष्टि की व्यवस्था में हर एक बात की सीमा है। जब स्वातन्त्र्य इस सीमा को पहुँच जाता है कि आगे जीव की स्वतन्त्रता अन्य जीवों की परतन्त्रता का कारण बन सके तो स्वतन्त्रता छीन ली जाती है। सृष्टि का नियम कहता है "बस यहीं तक ! आगे नहीं।" आप इसको कई प्रकार के उदाहरणों से जाँच सकते हैं। आप को मिठाई प्रिय है। आप खा सकते हैं। कितनी ? जितनी जी चाहें । आप स्वतन्त्र हैं । मिठाई की मात्रा को निर्धारण करने में एक लड्डू खाइये, दो खाइये, चार खाइये । आपके समक्ष लड्डूओं का थाल रक्खा है। आपको मज़ा आ रहा है। आप खाते चले जा रहे हैं। पेट तन गया परन्तु आपका खाना बन्द नहीं हुआ। सृष्टि का नियम आप को पूर्ण स्वतन्त्रता दे रहा है, आप को वह रोकता नहीं परन्तु एक ऐसी सीमा आ जाती है कि आप अति कर गये। भीतर से ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने लड्डू का मज़ा कम कर दिया है लड्डू वही हैं परन्तु मजा चला गया। अब आप चाहें तो भी नहीं खा सकते। सृष्टि के विधान ने आप को परतन्त्र कर दिया। इसलिये कि आपने अनुचित स्वतन्त्रता को काम में लाना चाहा ।
इतिहास बताता है कि बहुत से डाकुओं ने बचपन से छोटे छोटे कामों में स्वतन्त्रता का अनुचित प्रयोग किया। वे बढ़ते गये। पहले ठग बने, फिर छोटे डाकू, फिर बड़े आक्रमणकारी, फिर देशों को नष्ट करने वाले विजेता। यह सब स्वातन्त्र्य के कारण हुआ परन्तु एक सीमा आई । कुदरत ने कहा- "बस आपकी परीक्षा हो चुकी। अब हम आपको एक इंच बढने न देंगे।" अब उनका पतन आरम्भ हुआ। जो नैपोलियन कहा करता था कि “असम्भव" शब्द मूखों के कोष में ही मिल सकता है वह जब सेण्ट हैलीना के छोटे और कष्टप्रद टापू में कैद था तो उसे मनमाना खाना भी नहीं मिल सकता था । स्वतन्त्रता के प्रेम ने उसको उच्छृङ्खल कर दिया । वह बढ़ा तो देश की स्वतन्त्रता को हाथ में लेकर और मरा दीन होकर । इसी प्रकार छोटी बड़ी बहुत सी मिसालें हैं जो बताती हैं कि जीव स्वतन्त्र अवश्य है परन्तु स्वतन्त्रता की सीमा है । जब बच्चा चाकू से अपनी नाक काटने लगे तो पिता हाथ से चाकू छीनने के लिये मजबूर हो ही जायगा। परीक्षा-भवन में परीक्षार्थी परीक्षा-पत्र को लिखने में स्वतन्त्र है, मेज़ तोड़ने में नहीं। स्वतन्त्रता के भी नियम हैं ।
आप नहीं सब:-
प्रश्न-वह स्वतन्त्रता कैसी जिसकी सीमा निर्धारित हो ? वह तो आगे चल कर परतन्त्रता हो गई।
उत्तर-आप सोचें । जब हम कहते हैं कि आप कर्म करने में स्वतन्त्र हैं तो "आप" से हमारा तात्पर्य केवल आप से नहीं । सब जीवों से है। हर एक को पूर्ण स्वतन्त्रता मिल नहीं सकती जब तक स्वतन्त्रता की सीमा बांधी न जाये । कल्पना कीजिये कि हर मनुष्य को हर समय बिना रोक टोक सड़क पर से गुजरने की आज्ञा दी जाय और एक ही समय में दो मनुष्य उस अधिकार का प्रयोग करना चाहें, तो क्या परिणाम होगा ? आप दोनों परस्पर टकरा जाएंगे, और आप दोनों की स्वतन्त्रता आप दोनों की परतन्त्रता का कारण बन जायेगी। जिसको आप स्वतन्त्रता कहते हैं वह स्वतन्त्रता न रह कर घोर रूप होगा निकृष्टम परतन्त्रता का । सोहन कहेगा "मोहन मुझे चलने नहीं देता ।" मोहन कहेगा "सोहन मुझे चलने नहीं देता।" यह है स्वातन्त्र्य का दुरुपयोग और सृष्टि-क्रम आप के हित के लिये ऐसी स्वतन्त्रता की रोक करता है। इसलिये जब तक मनुष्य स्वतन्त्रता का सदुपयोग करता जाता है वह स्वतन्त्र ही रहता है ।
जीव शुभ कर्म या अशुभ कर्म क्यों करता है ?
प्रश्न-जीव शुभ या अशुभ कर्म क्यों करता है ? उत्तर-कर्तृत्व जीव का स्वाभाविक गुण है। यह बिना कुछ किये रह ही नहीं सकता। जैसे आग कभी अपनी गर्मी को छोड नहीं सकती ।
प्रश्न- जब कर्तृत्व जीव का गुण है तो वह अशुभ कर्म क्यों करता है ?
उत्तर- कर्म के लिये ज्ञान चाहिये। जीव स्वभाव से अल्पज्ञ है। उसको पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है। यथार्थ ज्ञान न होने से वह भूल कर बैठता है। जैसे छोटा बच्चा दीपक की लौ पकड़ कर अपना हाथ जला बैठता है ।
जीव का हित और कर्म फल-
प्रश्न- जीव का हित क्या है ? और उसके कर्मों का इस हित से क्या सम्बन्ध है ?
उत्तर-जीव का हित है अपने स्वरूप को पहचानना। जीव संसार में आकर अपने स्वरूप को भूल जाता है। वह अपने को जड़ या जड़ पदार्थों के आश्रित समझ लेता है। इस बेसमझी से जो कर्म किये जाते हैं, वे अशुभ होते हैं। क्योंकि जितने अधिक ऐसे कर्म होते हैं उतना ही जीव उनमें फँसकर अपने स्वरूप को अधिक भूल जाता है परन्तु जितने कर्म ऐसे हैं जिनसे उसको अपने स्वरूप का परिज्ञान हो, वे शुभ हैं । वं
प्रश्न ईश्वर की व्यवस्था जीव के कर्म-फल द्वारा उसके हित, अहित का कैसे सम्पादन करती है ? उत्तर-यह तो प्रत्यक्ष है कि हमारी भूलें हम को सचेत करती हैं। एक बार जल कर बच्चा दीपक की लौ नहीं पकड़ता क्योंकि उसके अज्ञान में कुछ कमी हो गई। ऐसा ही सब कर्मों का हाल है।
कर्म-फल का रूप
प्रश्न- परमेश्वर कर्मों का फल किस रूप में देता है ? उत्तर-कर्मों का फल तो अन्ततोगत्वा सुख या दु:ख के रूप
में ही होता है परन्तु इस सुख या दुःख को देने के अनेक निमित्त हैं । वह निमित्त न सुख है न दुःख, परन्तु सुख या दुःख के साधन अवश्य हैं। यह जानना कठिन है कि अमुक निमित्त कब दुःख का साधक है और कब सुख का । यह व्यवस्था जटिल है । पूर्ण रूप से उसे ईश्वर ही जानता है परन्तु विद्वान् भी अपने अनुभव से तर्क द्वारा या शास्त्र द्वारा इसको जान सकता है प्रश्न-बात स्पष्ट नहीं हुई । उदाहरण से समझाइये ? उत्तर-सिर दबाना एक निमित्त है। इससे सुख और दुःख दोनों हो सकते हैं । समय और परिस्थिति के अनुसार ही इसका निर्णय होगा। इसी प्रकार बहुत सी घटनाएं है, जो कभी एक मनुष्य के सुख का साधन होती हैं और कभी दुःख का और कभी एक मनुष्य के सुख का साधन होती हैं और कभी दूसरे के दुःख का। ऐसे उदाहरण सब को मालूम हैं
प्रश्न- ईश्वर जीव को उसके कर्मों का फल देता है अथवा अन्य के कर्मों का भी ?
उत्तर-ईश्वर जीव को उसी के कर्मों का फल देता है अन्य का नहीं । क्या परीक्षक परीक्षार्थी के अतिरिक्त किसी अन्य परीक्षार्थी के किये हुए कामों के लिये भी अंक देगा ? ऐसा करना तो अन्याय होगा । अर्थात् कर्म किया देवदत्त ने और उसका फल मिले यज्ञदत्त को । यह दया भी न होगी, क्योंकि जीव के भविष्य निर्माण का आश्रय दूसरे व्यक्ति पर होगा। यदि एक जीव के कर्मों का फल दूसरे को मिलने लगे तो व्यवस्था भी न रहेगी। अन्य जीव तो असंख्य हैं। किस किस के कर्मों का फल किस किस को दिया जायेगा? यदि सोहन के काम पर मोहन को अंक दिये गये तो सोहन के साथ अन्याय होगा। अतः ईश्वर किसी को उसी के कर्मानुसार फल देता है, दूसरे का नहीं । प्रश्न-कर्म का फल किस रूप में मिलता है ?
उत्तर-फल के केवल दो ही रूप हैं सुख या दुःख । शुभ कर्मों का फल सुख है अशुभ कर्मों का दुःख । चिरस्थायी और दुःखरहित सुख को आनन्द कहते हैं। स्वर्ग वह अवस्था है जिसमें सुख ही सुख हो, नरक वह अवस्था है जिसमें दुःख अत्यन्त अधिक हो।
कर्म-फल की व्यवस्था
प्रश्न- क्या ईश्वर की कर्म-फल के सम्बन्ध में कोई नियत व्यवस्था है या ईश्वर जब जैसा चाहे करता है ?
उत्तर-ईश्वर की सभी व्यवस्था नियत और अपरिवर्तनशील है। उसमें किञ्चित् भी अदल-बदल नहीं होती । समस्त जीवों को उसी व्यवस्था के अनुसार फल मिलता है ।
प्रश्न-यदि व्यवस्था-रूपी मशीन पूर्णतया नियत है तो ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता ? सृष्टि-क्रम हम को व्यवस्था की सूचना तो देता है; परन्तु ईश्वर को तो हम नहीं देखते ? हम को प्रयोजन व्यवस्था से है. व्यवस्थापक से नहीं, यदि ईश्वर को न भी मानें तो व्यवस्था वैसी ही रहेगी । उसमें परिवर्तन न होगा ।
उत्तर-यह ठीक है कि व्यवस्था निश्चित और अपरिवर्तनशील है परन्तु जो मनुष्य व्यवस्था को स्वीकार करता और व्यवस्थापक को छोड़ देता है, वह अज्ञान का दोषी है। अज्ञान बड़ा भारी दोष है । इसका परिणाम बुरा होता है । व्यवस्थापक को भूल जाने से व्यवस्थापक के गुणों के लिये भी प्रेम नहीं होता । जो मनुष्य व्यवस्थापक-शून्य जड़ व्यवस्था को मानते हैं वह अपने चेतन स्वरूप को भूल कर जड़-बुद्धि हो जाते हैं। उनमें व्यवस्थापक के शुभ गुणों का संचार नहीं होता ।
यह माना कि व्यवस्था के अनुसार जीव को अपने कर्मों का उतना ही फल मिलेगा, चाहे व्यवस्थापक के माने या न माने व्यवस्थापक के न मानने से अथवा उसे भुला देने से सब से बड़ी हानि यह होगी कि जीव की गुण-शीलता कम हो जायेगी और जीव के भावी ज्ञान तथा कर्म पर उसका प्रभाव पड़ेगा । न्यायाधीश तो न्याय ही करेगा, चाहे दूसरा उसके व्यक्तित्त्व को स्वीकार करें या न करे परन्तु तात्कालिक कर्म-फल की प्राप्ति के अतिरिक्त न्यायाधीश के व्यक्तित्त्व का सम्पर्क भी एक चीज़ है, जिससे वह मनुष्य वञ्चित रह जायेगा जो केवल तात्कालिक न्याय से ही सम्बन्ध रखना चाहता है और न्याय की पृष्ठ पर न्यायाधीश को देखना नहीं चाहता ।
कालिदास के काव्यों से कालिदास बड़ा है काव्यों से कालिदास की उस महत्ता का भी परिचय मिलता है, जो काव्यों से कहीं उच्चतर है । जो मनुष्य काव्यों मात्र को जड़ समझकर कालिदास के निज गुणों का पता लगाना नहीं चाहता. वह अधूरा है और प्रमुख लाभ से वञ्चित रह जाता है। यह ठीक है कि ईश्वर हमारे किये हुए कर्मों का उतना ही फल देगा कम या अधिक नहीं, परन्तु ईश्वर के व्यवस्थापक होने का विश्वास जीव में अन्य गुणों के धारण करने की योग्यता भी प्राप्त करायेगा. जो उसके भावी कर्मों पर प्रभाव डालेगी । ईश्वर को भूल कर केवल जड़ व्यवस्था को मानने वाले जड़वादी होकर अन्ततोगत्वा जड़ात्मक हो जाते हैं। और उनमें आध्यात्मिक सम्पर्क की कमी हो जाती है।
यदि हम ईश्वर को व्यवस्थापक न मानकर केवल व्यवस्था तक ही अपने को सीमित रखेंगे तो ऐसी व्यवस्था एक ज्ञान शुन्य जड़ यन्त्र के समान हो जायेगी और चेतन जीवन अचेतन यन्त्र के आधीन हो जायेगा। इससे व्यवस्था शब्द ही निरर्थक हो जायेगा । चेतन सर्वज्ञ व्यवस्थापक पर विश्वास करने से हमारे आत्मा में अध्यात्मभाव की जागृति होती है, हम समझने लगते हैं कि एक महाचेतन सत्ता ने हमारे हित को ध्यान में रखकर ही एक अटल और निश्चित व्यवस्था की स्थापना की है ।
कुछ लोग समझते हैं कि यदि ईश्वर की व्यवस्था निश्चित है और उसमें किसी परिवर्तन की सम्भावना नहीं तो ईश्वर की चेतनता नष्ट हो गई परन्तु यदि व्यवस्था को परिवर्तनशील माना जाय तो ईश्वर में उच्छृङ्खलता का दोष आयेगा। इस दोष से बचने का यही मार्ग है कि ईश्वर की व्यवस्था को ज्ञानानुकूल तथा निश्चित माना जाये। व्यवस्था को निश्चित करना भी तो ज्ञान का ही फल है। क्योंकि कर्म करने वाले के कर्म के शुभ या अशुभ होने की जाँच के बाद ही तो फल की व्यवस्था होगी ।
निमित्त और कारण
प्रश्न- निमित्त और कारण का भेद समझ में नहीं आया। जो घटना किसी कार्य से ठीक पूर्व हो उसको निमित्त भी कह सकते हैं और कारण भी ।
उत्तर-ऐसा मानना भूल है। हर एक कार्य से पहिले असंख्य घटनाएं हुआ करती हैं। उन को कोई कारण नहीं मानता । कल्पना कीजिये कि दत्तू डाकू को कई हत्याओं के फलस्वरूप फाँसी दी गई । फाँसी लगी १० अक्टूबर को ८ बजे प्रातः काल । हत्याएं हुईं तीन साल पूर्व । फाँसी के क्षण से पूर्व उस फाँसी के स्थान में तथा अन्य स्थानों में लाखों घटनाएं हुई। फाँसी देने वाले ने गले में रस्सी डाली, कई सम्बन्धी रोने लगे । जेल के डाक्टर ने परीक्षा के लिये तैयारी की। और बीसियों घटनाएं तत्क्षण हुई। क्या उनको आप फाँसी का कारण कहेंगे ? कदापि नहीं । फाँसी देने वाले ने जो क्रियाएं कीं वह फाँसी का कारण नहीं । हाँ निमित्त अवश्य हैं। जो फाँसी का मूल कारण है वह फाँसी के क्षण से बहुत पुरानी बात है। अन्य बहुत सी घटनाएं हैं जैसे-कौवे का बोलना या जेल के किसी कुत्ते का भोंकना जो न निमित्त हैं न कारण। अतः किसी क्रिया से पूर्व जो घटनाएं घटित हुईं वे तीन प्रकार की हो सकती है। कारण हों, निमित्त हों या न कारण हों न निमित्त; अपितु उस कार्य से सर्वथा असम्बद्ध हो ।
एक और दृष्टान्त लीजिये। मोहन डाकिये ने आप को ५०) का एक मनीआर्डर दिया। उसी क्षण या केवल एक क्षण पूर्व आपका कुत्ता भौंक पड़ा। अब प्रश्न यह है कि आप की धन प्राप्ति का कारण क्या है ? कुत्ते के भोंकने का धन प्राप्ति से कोई सम्बन्ध नहीं। मोहन का आना निमित्त मात्र है। मनीआर्डर भेजने वाले का काम मनीआर्डर की प्राप्ति का मूल कारण है
प्रश्न- क्या निमित्त बदल सकते हैं ? अर्थात् क्या एक कार्य के कई निमित्त हो सकते हैं ?
उत्तर- अवश्य ! यह सम्भव धा कि मनीआर्डर मोहन डाकिया न लाता बलदेव डाकिया लाता। इससे आप के कर्म-फल में कोई बाधा न पड़ती। पचास रुपये के दस दस के पाँच नोट न होते, पाँच पाँच के दस या एक एक के पचास नोट होते। आप के लिये एक सा ही था। निमित्त और कारण को एक ही समझ लेने से बहुत सी भ्रान्तियाँ पैदा हो जाती हैं प्रश्न-हिरोशिमा में अमेरिका वालों का बम गिरा ओर लाखों मर गये। बम इनकी मृत्यु का कारण था या निमित्त ? उत्तर-कारण तो मरने वालों के कर्म ही थे। बम निमित्त था।
प्रश्न- फिर अमेरिका वालों का क्या दोष ?
उत्तर-दोष यही है कि उन्होंने निमित्त को कारण समझा। यदि कारण न समझते तो बम फेंकने का इरादा भी न करते ।
प्रश्न- तो क्या इन सब लाखों आदमियों ने पाप किये थे जिनका फल एक साथ मृत्यु हुई ?
उत्तर-सम्भव है कि किसी के शुभ कर्म हों और किसी के अशुभ । इसका परिणाम तो मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है यह कोई निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकता कि जितने मरने वाले थे उन सब को अच्छी योनियाँ मिली या बुरी ही। जो जीव की नित्यता पर विश्वास नहीं रखते उनको तो यही मानना चाहिये कि मरने वाले झंझट से छूट गये । वे अभाव को प्राप्त हो गये । यद्यपि है यह सिद्धान्त अयुक्त ही परन्तु जो मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात् जीव रहता है उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि मरने वालों का भविष्य बुरा हुआ या भला । सम्भव है कि बहुत सों का बुरा हुआ हो और बहुत सों का भला । रही एक साथ अचानक मृत्यु की बात ! यह प्रश्न भी हमारी अल्पदर्शिता के कारण होता है। संसार में करोड़ों प्राणी हर समय मरते रहते हैं। एक नगर के बूचड़खाने में एक ही दिन प्रातः काल हज़ारों जानवरों की मृत्यु हो जाती है । और एक दिन में एक देश में न जाने कितने मनुष्य मर जाते हैं। भेद केवल इतना है कि एक स्थान पर जो हुआ वह हमारी आँखों के समक्ष हुआ ? और हम भयभीत हो गये ।
प्रश्न-कर्म-फल के सिद्धान्त और कारणकार्य के सिद्धान्त या भिन्न ? यदि भित्र हैं तो इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध भी एक हैं है या नहीं है तो क्या ? नहीं तो कैसे ?
उत्तर-कारण-कार्य का सिद्धान्त और कर्म फल का सिद्धान्त एक नहीं परन्तु उनमें सादृश्य अवश्य है। जिस प्रकार विशेष कारण से विशेष कार्य होता है और विशेष कार्य का विशेष कारण होता है, उसी प्रकार विशेष कर्म का विशेष फल होता है और विशेष फल विशेष कर्म का ही परिणाम होता है । तथापि कारण-कार्य का सम्बन्ध विशेषत: जड़ जगत् से है। और कर्म-फल के सिद्धान्त का जड़ जगत् से कोई सम्बन्ध नहीं। जड़ जगत् में गति या क्रिया होती है परन्तु हम उस को कर्म नहीं कह सकते। न उसके विषय में गीता के वे श्लोक लागू कर सकते हैं, जैसे 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इत्यादि और न योगदर्शन के 'सति मूले तद्विपाक: आदि सूत्र। आग से धुँआ उत्पन्न होता है। आग कारण है धुँआ कार्य । मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, मिट्टी कारण है घड़ा कार्य, परन्तु आग से धुँआ उत्पन्न होगा ही और मिट्टी से घड़ा बनेगा ही। यह नहीं कहा जा सकता है कि आग को धुँआ बनाने का अधिकार है या मिट्टी को घड़ा बनाने का। आग के वश में नहीं है कि धुँआ न बनावे। मनुष्य के वश में है कि चोरी करे या न करे। अतः चोरी मनुष्य का कर्म है और चोरी का दण्ड उस कर्म का फल । कार्य में कारण व्यापक रहता है, जैसे घड़े में मिट्टी या कंगन में सुवर्ण या धुँए में आग परन्तु फल में कर्म व्यापक नहीं होता। कारण और कार्य का घनिष्ठ सानिध्य है, कर्म और फल का नहीं । जहाँ जहाँ धुँआ है वहाँ वहाँ आग है परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जहाँ कर्म है वहाँ फल है। कारण में कार्य फिर लीन हो जाता है जैसे घड़ा टूट कर मिट्टी हो जाता है, परन्तु फल समाप्ति पर कर्म में लीन नहीं होता ।
सादृश्य यह है कि कारण कार्य से पूर्व होता है और कर्म भी फल से पूर्व। जैसे कार्य से पूर्व होने वाली प्रत्येक घटना उस कार्य का कारण नहीं इसी प्रकार से फल से पूर्व होने वाली प्रत्येक क्रिया भी उस फल का कर्म नहीं है। एक मनुष्य मर गया । यह दुर्घटना एक कार्य है। उसके मरने से ठीक पूर्व लाखों अन्य घटनाएं हुईं। कुत्ता भौंका, वृक्ष के पत्ते हिले, घड़ी का घण्टा बजा, रेलगाड़ी आई. छत गिरी परन्तु मृत्यु का कारण केवल एक था छत का गिरना। दूसरी सैकड़ों घटनाएं मृत्यु के कारण न थीं। इसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु रूपी फल छत गिरने रूपी कर्म का फल था। क्योंकि छत का गिरना मरने वाले का कर्म नहीं था । मृत्यु रूपी फल किसी अन्य कर्म का ही रहा होगा, जो उसी मरने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित होगा
न विज्ञान, न दर्शन
कारण-कार्य और कर्म-फल के सिद्धान्तों में इतना सादृश्य है कि बहुधा हम एक दूसरे को मिला देते हैं । कारण-कार्य के निर्धारित करने में भी बहुधा भूलें होती हैं। बहुधा हम पहली किसी घटना को पिछली घटना का कारण समझ लेते हैं। जैसे हम किसी मुकदमे के लिये कचहरी जा रहे थे। घर से चलते समय किसी ने छींक दिया। हम मुकदमा हार गये । हम कहते हैं छींक हार का कारण थी। यह सर्वथा गलत है। सम्भव है कचहरी का फैसला बहुत पहले ही हो चुका हो और हम को केवल पता न हो। इसी प्रकार किसी शत्रु ने कहा "अमुक का बेटा मर जाय" अकस्मात् बेटा मर गया। उसने सोचा कि शत्रु का कोसना कर्म था और बेटे का मरना फल। इस प्रकार के टोने-टोटके, कोसा कासी प्रायः होते रहते हैं। साधारण जनता में और काव्यों में इनका प्राचुर्य है। राजा दिलीप ने कामधेनु को या स्वर्गीय गौ को प्रणाम नहीं किया । गौ ने शाप दिया। इसका फल हुआ यह कि दिलीप के सन्तान नहीं हुई । यहाँ न तो कार्य कारण का सम्बन्ध दीखता है, न कर्म फल का। जैसे बहुधा सार्वजनिक कल्पनाएं अवैज्ञानिक अथवा अदार्शनिक होती हैं, उसी प्रकार कवियों की कल्पनाएं भी। राजा पुरूरवा उर्वशी के वियोग में विलाप करता हुआ हंस को चलते देखता है और कहता है "रे हंस तू उर्वशी की चाल को चुरा लाया है। बता तो कि उर्वशी कहाँ है ?" यह काव्य कल्पना ही तो है मोह, है, अज्ञान है। न विज्ञान है, न दर्शन ।
क्रियमाण कर्म के आरम्भ से लेकर उसके पकते पकते प्रारब्ध तक पहुँचने और फलीभूत होने तक बहुत सी घटनाओं का सिलसिला रहता है, जिनमें कारण कार्य सम्बन्ध रहता है एक दूसरे का फल नहीं होतीं ।
परन्तु वे उदाहरण के लिये नीचे लिखी घटनाओं पर विचार कीजिये
१-मोहन ने गोपाल के घर में चोरी की ।
२- दो सौ रुपये उसके हाथ लगे ।
३-उसने इन रुपयों के बदले आटा, घी, शक्कर खरीदे
४- उसके परिवार ने उसको खाया ।
५- सब ने मिलकर इस सुख को भोगा ।
६-गोपाल ने पुलिस में रिपोर्ट को । ७-पुलिस ने जाँच के लिये आदमी लगाये।
८-जाँच चार मास तक होती रही, तब पता चला कि मोहन ने चोरी की है ।
९-उस पर अभियोग चला जो चार महीनों तक जारी रहा।
१०- अन्त में अभियोग सिद्ध हुआ और न्यायाधीश ने उसे एक साल का दण्ड दिया ।
११-मोहन को पुलिस के लोगों ने कारावास में भेज दिया। संक्षेप के लिये हमने सैकड़ों घटनाओं के केवल ११ विभाग कर दिये हैं। वस्तुत: चोरी कर्म है और कारागार फल । शेष सैकड़ों घटनाओं में से कुछ तो कुछ का कारण थीं कुछ असम्बद्ध भी रही होंगी। जैसे परिवार का हलवा खाना और पुलिस की रिपोर्ट परन्तु इनमें से किसी का कर्म और फल का सम्बन्ध नहीं था
कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य
प्रश्न- कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है ?
उत्तर- एक उदाहरण पर सोचिये राजभक्ति क्या है और राजद्रोह क्या है ? राज्य का शासन जिन मूल तत्त्वों के आधीन है। उनका सहयोग करना राजभक्ति और उनके विपरीत आचरण करना राजद्रोह है। राज्य कर्मचारियों को अनुचित रिश्वत देना राजद्रोह है क्योंकि यह उन उन मूल तत्त्वों के विपरीत है जिन पर शासन आधारित है। राजा की खुशामद करना राजद्रोह है। क्योंकि शासन का मूल तत्त्व राजा के स्वेच्छाचरण की संतृप्ति पर आधारित नहीं है। कमजोर और स्वार्थी राजे कभी कभी असली राज्यभक्ति को राजद्रोह और राजद्रोह को राजभक्ति समझ लेते हैं परन्तु है यह समझ का फेर ।
इसी उदाहरण को विश्व पर घटाइये। विश्व के शासन के कुछ मूल तत्त्व हैं । और उनका असली प्रयोजन है जीवों का हित अतः उन मूल तत्त्वों के साथ सहयोग करना कर्त्तव्यता या शुभ कर्म है। और उनमें विघ्न डालने का विचार करना अकर्त्तव्यता या अशुभ कर्म है। इसी को पुरुषार्थी और अपुरुषार्थी कहेंगे पुरुषार्थी का शाब्दिक अर्थ यह है 'पुरुष का अर्थ' अर्थात् 'जीव का हित'। जीव का हित भी वह नहीं जो जीव चाहे । मनुष्य चाहता तो बुरा भी है और भला भी। हित है अन्तिम आध्यात्मिक उन्नति का विकास। अत: यह सिद्ध हुआ कि हमारा जो कर्म हमारे विश्व के आध्यात्मिक विकास में सहायक हो वही पुरुषार्थ है ओर जो बाधक हो वह अपुरुषार्थ । बच्चा रोग में अनिष्ट चीजें खाना चाहता है । उनको जुटाना न तो बच्चे का हित है न अर्थ । अत: जो बच्चे की इच्छा पूर्ति को ही उसका हित समझता है वह भूल करता है ।
जीव और बुद्धि
प्रश्न-हमारी बुद्धि हम को सदा सन्मार्ग पर तो नहीं ले जाती ।
उत्तर-इससे क्या ? यह तो आपका काम है कि बुद्धि को किस प्रकार प्रयुक्त करें। केवल बुद्धि का प्रयोग मात्र ही आप की स्वतन्त्रता का द्योतक है ।
प्रश्न-क्या ईश्वर ने किसी को अच्छी और किसी को बुरी बुद्धि देकर हम से विवेक की स्वतन्त्रता छीन नहीं ली ? यदि हम को श्रेष्ठ बुद्धि मिलती तो हम कभी असन्मार्ग का अवलम्बन न कर सकते ।
उत्तर-परमात्मा ने अकारण ही आपको बुरी बुद्धि नहीं दी। आपने अपने विवेक शून्य कर्मों से भी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। जो तराजू आपको मिली है, यदि वह आपकी असावधानी से टूट जाय तो दोष किस का ? फिर भी आपकी तराजू आपके हाथ में । आप बुद्धि के प्रयोग करने के अधिकार से कभी वञ्चित नहीं किये जाते । जब आपको मालूम हो जाय कि तराजू में बिगाड़ आ गया है तो आप उसे बना या सुधार सकते हैं। हर मनुष्य अपनी बुद्धि को ज्ञान, क्रिया तथा सावधानी से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट बना सकता या बिगाड़ सकता है। शराब पीने से बुद्धि बिगड़ती और घी दूध आदि के उचित प्रयोग से बढ़ती है। अतः बुद्धि के तारतम्य का दोष जगत् के नियन्ता पर लगाना दोष है।
प्रश्न-जब हमारी बुद्धियाँ भिन्न-भिन्न है तो कर्म भी भित्र-भिन्न होंगे और फल भी भित्र-भित्र फिर स्वतन्त्रता कैसी ? निर्वाचन के कई मार्ग।
उत्तर-यह ठीक है कि तीव्र बुद्धि वाला मनुष्य जो कर्म कर सकता है उसे मन्दबुद्धि नहीं कर सकता परन्तु मन्दबुद्धि वाले या तीव्र बुद्धि वाले मनुष्य के समक्ष निर्वाचन करने के लिये कई मार्ग खुले होते हैं या नहीं ? यदि होते हैं तो स्वतन्त्रता सिद्ध है। एक चींटी भी जानती है कि उसके समक्ष कई मार्ग हैं। वह सोचती है और एक मार्ग पर चल देती है । इसी प्रकार पशु-पक्षियों का हाल है। आपके आँगन में आने वाले कौए या अन्य पक्षी भी सोचते और एक मार्ग को छोड़ कर दूसरे का अवलम्बन करते हुए प्रतीत होते हैं। अतः सिद्ध है कि वे कार्य करने में स्वतन्त्र हैं। आप किसी कुत्ते को अपने स्वामी के साथ सड़क पर चलता हुआ देखें और निरीक्षण करें। आप को ज्ञात होगा कि कुत्ता निरन्तर सोच रहा है। कि अब क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये
भाग्य प्रबल है या पुरुषार्थ
प्रश्न- भाग्य प्रधान है या पुरुषार्थ ?
उत्तर-पुरुषार्थ प्रधान है क्योंकि भाग्य भी तो पुरुषार्थ का ही फल है। जब तक कर्म न हो तो तब तक फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती ।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।
जो जस करहिं सो तस फल चाखा ॥
पुरुषार्थ कर्म है, भाग्य फल !
प्रश्न-तो पुरुषार्थ करते रहना चाहिये ।
उत्तर-यह ठीक है, परन्तु प्रश्न यह है कि पुरुषार्थ क्या है और क्या पुरुषार्थ नहीं। हर एक कर्म जो मनुष्य करता है पुरुषार्थ नहीं है न पारिभाषिक अर्थ में कर्म ही है । किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
विश्व में एक भ्रान्ति
बहुत से लोग कुकर्मों को भी पुरुषार्थ समझते हैं। एक परीक्षार्थी का उदाहरण लीजिये। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना फल है जिसके पाने के लिए उसे यत्न करना है। उसका समस्त विहित विधान के अनुसार सावधानी से निरन्तर अध्ययन करना पुरुषार्थ है। अनिष्ट विधियों से परीक्षा भवन में नकल करना, परीक्षक को धमकी देना उस पर दबाव डालना या अन्य चालाकियाँ करना क्रियाएं (कर्म) तो हैं परन्तु उनको शुभ कर्म या पुरुषार्थ में नहीं गिन सकते। संसार में यह बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि प्रत्येक चालाकी, मक्कारी और दगाबाज़ी को पुरुषार्थ समझकर लोग बुरे कर्मों में उलझे रहते हैं। उनका फल बुरा होता है। प्राय: सर्वसाधारण में तदबीर तकदीर के विवाद चलते रहते हैं। प्राय: चालाकी से की हुई दौड़ धूप को तदबीर या पुरुषार्थ समझ लिया जाता है। रिश्वत देना तदबीर, झूठ बोलना तदबीर, चालाकी चलना तदबीर। जो रिश्वत न दे या चालाकी न चले उसको कहेंगे कि “यह सोता रहा, इसने तदबीर तो की ही नहीं । बिना पुरुषार्थ किये भी फल मिल सकता है क्या ?" इस प्रकार संसार में शुभ कर्म को पुरुषार्थ नहीं समझा जाता । इसी कारण पाप में पवृत्ति बढ़ती है और वह दुःखमूलक भी होती है । वस्तुतः कर्तव्य परायणता पुरुषार्थ है। अन्य सब अपुरुषार्थ या असली तदबीर का उल्टा मात्र ।
योगदर्शन और कर्म
प्रश्न-योगदर्शन में कर्म के विषय में दो सूत्र दिये हैं -
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ॥
कर्म का मूल रहने पर जब वह पकता है तो जाति या जन्म, आयु और भांग के रूप में आविर्भूत होता । यह जन्म आयु और भोग, पुण्य और पाप की अपेक्षा से सुख और दुःख रूपी फल वाले होते हैं ।
यहाँ प्रश्न उठता है कि कर्म का फल सुख या दुःख है या जन्म (जीवन) की इयत्ता और भोग। दूसरा प्रश्न यह है कि भोग सुख और दुःख से इतर क्या वस्तु है ? अथवा भोग का ही नाम सुख और दुःख है ? तीसरा प्रश्न यह है कि यदि कर्म का फल सुख या दुःख ही है तो 'जाति' और 'आयु' कहने की क्या आवश्यकता थी ? चौथा प्रश्न यह है कि क्या जाति, आयु और भोगों के पिछले कर्मों के अनुसार नियत होने पर आगे को स्वतन्त्र कर्म करने का कोई अवसर रहता है या नहीं ? क्या हमारा प्रत्येक कर्म केवल भोगों के भोगने का ही एक प्रकार मात्र है ? इनको समझाइये ।
जाति, जन्म, आयु व भोग क्या ?
उत्तर-जाति, आयु और भोग ये तीनों तो 'जीवन' के ही एक प्रकार के अङ्ग-प्रत्यङ्ग हैं। मैंने मनुष्य, कुत्ता, या बिल्ली के रूप में जन्म लिया । यह हुई जाति अर्थात् एक विशेष योनि में मुझे डाला गया । कुछ समय इसी योनि में रहूँगा । यह हुई आयु । दस वर्ष या साठ सत्तर वर्ष । इस आयु में मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होंगी । ये हुए भोग । भोगों के हुए दो रूप सुख या दुःख परन्तु हमारी सब अनुभूतियाँ दु:ख या सुख ही नहीं हैं। यद्यपि उनमें दुःख और सुख का समावेश रहता है। जीव केवल दुःख और सुख का ही भोक्ता मात्र तो है नहीं। कर्तृत्व और ज्ञातृत्व भी उसके गुण हैं। हम कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। वह ज्ञान सुख या दुःख से इतर वस्तु है, यद्यपि एक ही प्रकार के ज्ञान से हम को कभी सुख और कभी दुःख होता है। एक मोटा उदाह लीजिये। कल्पना कीजिये मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मेरे खेत में दस मन गहूँ उत्पन्न हुआ। इस ज्ञान से मुझे दुःख और सुख दोनों हो सकते हैं। यदि मैंने सुना कि समस्त गाँव वाले किसानों के खेत में केवल पाँच मन ही हुआ और मेरे में दस मन तो मुझे सन्तोष होगा कि मेरे खेत की उपज कम नहीं है। यदि यह पता चले कि मेरे पड़ोसियों के खेत में १५ मन हुआ तो मुझे कुछ दुःख होगा कि मैं पीछे क्यों रह गया। यह "दस मन उपज" का ज्ञान तो एक सा ही रहा, परन्तु उसने कभी सुख और कभी दुःख उत्पन्न कर दिया। इसके अतिरिक्त हम कर्म भी निरन्तर ही करते रहते हैं और उनसे कभी सुख और कभी दुःख होता है। हमारे शरीर में पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । भोगेन्द्रिय कोई अलग नहीं फिर भी हर कर्म और हर ज्ञान कभी सुख और कभी दुःख रूपी फल वाला होता है। इस प्रकार यद्यपि पुराने कर्म हम को जाति. आयु और भोग के रूप में फलित दृष्टिगत होते हैं परन्तु यह तो जीवन का ही विस्तार है । इनके अतिरिक्त जीवन स्वयम् एक अलग उद्देश्य रखता है। वह है कर्म और ज्ञान का कहा गया है कि ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती । (ऋते ज्ञानात्र मुक्ति:) ज्ञान का अर्थ है ज्ञान या अविद्या का नाश। इसकी दूसरी अर्थापत्ति है-अपने स्वरूप का ज्ञान या अपने स्वरूप के विषय में अज्ञान की निवृत्ति । यह ज्ञान की उपलब्धि और अज्ञान की निवृत्ति बिना कर्म किये तो होगी नहीं । कुछ कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अत: जीवन का मुख्य उद्देश्य हुआ स्वतन्त्र कर्म और उनसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान या ज्ञानशक्ति। इसलिये जहाँ कर्म के विपाक का रूप जाति, आयु और भोग बताया वहाँ यह तो जीवन-रूपी साधन के अङ्गों का वर्णन किया । जीवन के उद्देश्य का वर्णन नहीं किया । इसलिये योगदर्शन में शिष्य को सतर्क करने के लिये अगला सूत्र पढ़ा-
परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दु:खमेव सर्वं विवेकिनः ।
अर्थात् ज्ञानी मनुष्य के लिये तो यह सुख-दुःख फल वाले जाति, आयु और भोग भी दुःख हो है । अर्थात् ज्ञानी इनसे सन्तोष नहीं करते। इस सन्तोषाभाव के चार कारण बताये गये
(१) परिणाम-अर्थात् ये सदा एक रस रहने वाले नहीं। इनका ठीक ही क्या है जो इनको सन्तोष का साधन समझा जाये।
(२) ताप-इनका सुख भी दुःख-मिश्रित है ।
(३) संस्कार-यह मन पर प्रभाव छोड़ते हैं और मन की वृत्तियों को रंजित करते हैं ।
(४) दुःख-इनसे साक्षात् दुःख होता है। इनके अतिरिक्त आयु का समस्त वस्तुओं के साथ सतोगुण, रजोगुण, और तमोगुण सम्बन्धी प्राकृतिक गुण विरोध लगा हुआ है। अतः मनुष्य को इनसे सन्तुष्ट न रह कर कुछ ऊपर उठना और अन्तिम ध्येय की ओर सोचना है। साधनपाद में आगे चलकर सूत्रकार ने विभिन्न साधनों का उल्लेख किया है, जिससे मनुष्य यहीं तक न रह जाये ।
कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और उपासनाकाण्ड
प्रश्न- प्राय: हम कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और उपासनाकाण्ड रूपी तीन काण्डों का नाम सुनते हैं। इन काण्डों का 'कर्म के सिद्धान्त' से क्या सम्बन्ध है ?
उत्तर- जीव का यह लक्षण हैं-कर्तृत्वज्ञातृत्व भोक्तृत्ववानणुः जीव इत्युच्यते । जिसमें कर्तृत्व, ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व ये तीनों गुण पाये जावें वह जीव या चेतन है। जड़ वस्तुओं और चेतन पदार्थों अर्थात् कीट पतंग से लेकर मनुष्यों तक में ज्ञान, क्रिया और सुख दुःख (भाव) पाये जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी मानवी मस्तिष्क की तीन विशेषताएं बताई हैं ज्ञान (Knowing या Cognition) सुख या दुःख या भाव (Feeling या Affection), क्रिया या इच्छा शक्ति (Will या Volition) इनके तीन विभाग अलग अलग हैं। इन्हीं का नाम ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड है। उपासनाकाण्ड को भाव काण्ड भी कहते हैं। ये काण्ड तीन तो हैं परन्तु ऐसे नहीं हैं कि सर्वथा अलग अलग और असम्बद्ध हों। मानवी मस्तिष्क की ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व शक्तियों को सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक ही पदार्थ के तीन गुण हैं। इसी प्रकार ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और भावनाकाण्डों को भी सर्वथा अलग नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक प्राणी के जीवन में ये काण्ड मिलेंगे। वह कुछ न कुछ जानने का यत्न करेगा यह हुआ ज्ञानकाण्ड वह कुछ न कुछ करेगा यह हुआ कर्मकाण्ड। उसे कुछ न कुछ दु:ख या सुख होगा यह हुआ उपासनाकाण्ड या भावनाकाण्ड । जिस प्रकार दीवार की लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई को दीवार से अलग करके नहीं दिखा सकते इसी प्रकार चेतन संज्ञाओं के ज्ञान, कर्म और सुख दुःख रूपी भावों को अलग करके नहीं दिखा सकते । फिर भी जैसे लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई को समझ सकते हैं कि ये तीन गुण हैं इसी प्रकार ज्ञान, कर्म और भाव को भी समझ सकते हैं
ज्ञानकाण्ड में सम्यक् ज्ञान, अधूरा ज्ञान, उलटा ज्ञान आदि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि सभी आ जाते हैं भ्रममूलक ज्ञान भी ज्ञानकाण्ड का ही भाग है। कर्मकाण्ड में मन तथा कर्म-इन्द्रियों द्वारा किये गये सभी शुभ और अशुभ कर्म शामिल हैं। अनेक प्रकार के दुःख, सुख तथा सर्वोत्कृष्ट आनन्द भी उपासना काण्ड या भाव काण्ड में सम्मिलित हैं। 1
'कर्म के सिद्धान्त' में इन तीनों का समावेश है। अर्थात् जब हम स्वतन्त्रता से कर्म करते हैं तो हम विचार करते हैं कि कौन क्रिया करनी चाहिये, कौन न करनी चाहिये । इसमें ज्ञान या ज्ञातृत्वशक्ति का प्रयोग करना पड़ता है और जब सुख या दुःख रूपी फल मिलता है तो यह भावकाण्ड या उपासना- काण्ड के अन्तर्गत आता है। ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सर्वोत्कृष्ट विषय को विद्या या विज्ञान कहते हैं। जिसमें भ्रम या अविद्या का कुछ भी अवशेष न रहे कर्मकाण्ड के सर्वोत्कृष्ट विषय का नाम परोपकार है। जिसमें स्वार्थ का लेश मात्र भी न रहे। और भावना काण्ड के सर्वोत्कृष्ट विषय का नाम आनन्द है जिसमें दुःख किञ्चित् मात्र भी न रहे ।
ईश्वर के तीन काण्ड -
जीव भी चेतन है और ईश्वर भी चेतन है । ईश्वर में ये भी तीन काण्ड समझे जा सकते हैं। परन्तु ईश्वर पूर्ण ज्ञानी या सर्वज्ञ है। उसमें अविद्या है ही नहीं। उसका ज्ञानकाण्ड सर्वशुद्ध-ज्ञानमय है। मनुष्य के ज्ञानकाण्ड में उतनी शुद्धता नहीं पाई जाती । कुछ न कुछ अज्ञान, विपरीत ज्ञान या अधूरा ज्ञान रहता है। ईश्वर के कर्मकाण्ड में शुद्ध परोपकार है। स्वार्थ का लवलेश भी नहीं। उसके काम तो असंख्य हैं परन्तु स्वार्थ के लिये एक भी नहीं। सब दूसरों के लिये हैं। अतः शुभ और अशुभ का प्रश्न नहीं उठता। ईश्वर शुभ ही करता है। अशुभ करता ही नहीं। अत: उन कर्मों के सुख या दु:ख रूपी फलों का भी प्रश्न नहीं उठता । उसका भावकाण्ड या उपासना काण्ड भी पूर्णतया शुद्ध और निर्मल है। उसके आनन्द में कभी कमी नहीं होती । अतः दुःख भी नहीं होता । मनुष्य को सुख होते हुए भी यह विचार करके कि यह सुख नष्ट हो सकता है दुःख की भावना बनी रह सकती है। इसलिये योगदर्शन में अन्य चेतनों से ईश्वर विलक्षण है। इस बात को दर्शाने के लिये यह सूत्र कहा गया
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः ।
अर्थात् ईश्वर के कर्म शुभ और अशुभ दो भागों में नहीं बाँटे जा सकते । अतः उसके कर्मों के सञ्चित, क्रियमाण और प्रारब्ध भेद भी नहीं होते । अतः कर्म विपाक भी नहीं होता । अतः कर्म का सिद्धान्त ईश्वर पर लागू नहीं होता । जैसे शासन का दण्ड विधान (Criminal code) केवल शुभ कर्म वालों के लिये नहीं है । अपितु उनके लिये ही है जो अशुभ कर्म करते या कर सकते हैं। उसी प्रकार कर्म के सिद्धान्त ईश्वर पर लागू नहीं होते । जो मनुष्य इन तीनों काण्डों के पारस्परिक सम्बन्धों को जानता हुआ अपने ज्ञान, अपने कर्म, और अपने भावों को सर्वोत्कृष्ट या लगभग ईश्वर के जैसा बना लेता है वह कर्म के बन्धन से छूट कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।
उपनिषद् में कहा है---
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ||
अर्थात् जब ईश्वर को सर्वव्यापक भाव से मनुष्य देख लेता है तो उसके हृदय की गाँठ खुल जाती है। सब संशय निवृत्त हो जाते हैं अर्थात् उसका ज्ञानकाण्ड अविद्याशून्य निर्मल हो जाता है। अशुभ कर्मों की सम्भावना नहीं रहती और सब कर्म (अर्थात् विपाक वाले) कर्म क्षीण हो जाते हैं। जब कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड निर्मल हो गये तो भावकाण्ड या उपासनाकाण्ड भी निर्मल हो जाता है । इसी को कैवल्य या मोक्ष कहते हैं।
प्रश्न-लोग उसी को कर्मकाण्डी कहते हैं जो होम, यज्ञ आदि करता है। क्या अन्य कर्म जैसे कृषि, व्यापार व्यवसाय भी कर्मकाण्ड का भाग है।
उत्तर-इस विषय में जनता में भ्रान्ति है । होम आदि तो कर्म का एक भाग मात्र हैं। हमारे जीवन के सभी शुभ और अशुभ कर्म कृषि, व्यवसाय, यहाँ तक कि चोरी, जारी आदि भी कर्मकाण्ड के अन्तर्गत हैं। जिनको पञ्चयज्ञ कहा जाता है उनमें केवल होम या हवन ही नहीं है। अन्य शुभ कर्म भी हैं। और उनमें ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का समावेश है। मनुष्य के जीवन की कोई क्रिया या घटना इन तीनों काण्डों से बाहर नहीं है। कर्म का सिद्धान्त इन्हीं तीनों विभागों के संतुलन पर बल देता है। और अन्ततोगत्वा यह सब मोक्ष प्राप्ति के लिये है।
कर्म और आत्म-विकास
प्रश्न- यदि आत्मा का विकास या उन्नति सृष्टि का प्रयोजन है तो सुख या दुःख का आत्म विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर- सुख-आत्मा का भोजन है, और दुःख औषध । सुखी होकर आत्मा इष्ट काम करने में उत्साहित होता है और दुःख उसको अनिष्ट काम करने से रोकते हैं। इस प्रकार सुख या दुःख दोनों आत्म विकास के साधन हैं ।
प्रश्न- क्या सुख पाकर मनुष्य आलसी, घमण्डी, असावधान तथा प्रमादी नहीं बन जाता और क्या दुःखों से मनुष्य को निराशा, मनोदौर्बल्य तथा आत्मग्लानि नहीं होती ।
उत्तर-कभी कभी ऐसा होता है परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य अपने को इस दुर्गुण से बचाता है परन्तु यदि सुख का सर्वथा अभाव हो तो जीवन कठिन हो जाये । दुःख भी एक सीमा से बाहर असह्य हो जाता है। दुःख का मुख्य उद्देश्य तो पाप की प्रवृत्ति को रोकना ही है और सुख का मुख्य उद्देश्य है पुण्य की प्रवृत्ति को विकसित करना परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य ही परिस्थिति का ठीक लाभ उठा सकता है । इसीलिये कर्म करने के लिये बुद्धि के विकास की आवश्यकता है ।
सुख-दुःख का ज्ञान-स्तर से सम्बन्ध-
प्रश्न-सुख और दुःख का जीव के ज्ञान-स्तर से भी सम्बन्ध है या नहीं ?
उत्तर-है । आत्मा केवल सुख या दुःख का बण्डल ही तो है नहीं। आत्मा के गुण तो छ: हैं। सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान तथा प्रयत्न । आप इनके द्वन्द्वों को एकीकरण करके तीन भाग कर सकते हैं । अर्थात् कर्तृत्व, ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व । जीव ज्ञाता भी है, कर्त्ता भी है और भोक्ता भी । ज्ञातृत्व ज्ञान का सूचक है। कर्तृत्व कर्म या प्रयत्न का. सुख और दुःख भोक्तृत्व का' इच्छा और द्वेष को सीमान्त प्रदेश समझिये । अर्थात् उनमें सुख के भोगने का ज्ञान और प्रयत्न दोनों विचित्र रूपेण सम्मिश्रित रहते हैं। इन छओं से मिलकर एक स्तर (level) बनता है। यह स्तर उत्तरोत्तर वृद्धि या ह्रास को प्राप्त हुआ करता है, जो जीव के ज्ञान और प्रयत्न के स्तर पर निर्भर रहता है। परन्तु ज्ञान और प्रयत्न दोनों पर सुख और दुःख का प्रभाव पड़ता हैं
प्रश्न-प्राणी को किस चीज़ से दु:ख होता है और किस से सुख ?
सुख और दुःख आन्तरिक हैं, बाह्य नहीं
उत्तर- दुःख सुख सुख और और दु:ख के साधनों में भेद है। इसी प्रकार के साधनों में भी भेद है । एक वस्तु न दुःखदायक है और न सुखदायक । उसी से सुख भी मिलता है और दुःख भी । संसार में यह भी एक भूल है कि जिसके पास सुख के साधन अधिक हों उसे सुखी समझ लिया जाय और जिसके पास वे साधन नहीं हैं उसको दुःखी प्राणी झोपड़ी में सुखी और महलों में दु:खी देखा जाता है । अत्यन्त रोगी को भी सुख की नींद सोता पाते हैं और पूर्ण स्वस्थ को भी चिन्ता-ग्रस्त देखा जाता है। अतः ऊपरी उपकरणों को देखकर सुखो या दु:खी समझ लेना भूल है। सुख और दुःख आन्तरिक हैं, बाह्य नहीं । एक ही घटना एक प्राणी को सुख देती है और दूसरे को दुःख। 'अ' की मृत्यु से उसके मित्र दु:खी होते हैं और शत्रु सुखी एक प्रकार की घटना कभी मुझे दुःख देती है और कभी सुख । अतः बाह्य साधनों को जुटाना ही पर्याप्त नहीं है । आन्तरिक वृत्ति भी होनी चाहिये । इन वृत्तियों के निर्माण में ज्ञान प्रयत्न और सुख दुःख सब का हाथ है।
प्रश्न- यदि सुख का उपकरण सदा सुख नहीं देता अथवा दु:ख का उपकरण सदा दुःख नहीं देता तो उनको सुख का उपकरण या दुःख का उपकरण क्यों कहते हैं ?
उत्तर-इसका कारण यह है कि साधारण परिस्थिति में यदि वृत्तियां सामान्य रहें तो उन उपकरणों को सुख या दुःख की उपलब्धि में लागू किया जा सकता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो ही जाय । रोटी से पेट भरता है और स्वास्थ्य उपलब्ध होता है। परन्तु रोग भी हो सकता है । अत: कारण और उपकरणों में सदा विवेक करना आवश्यक है। केवल उपकरणों को जुटाने मात्र से सुख या दुःख नहीं मिल जाता । अतः उपकरणों को जुटाते समय यह भी देख लेना चाहिये कि उनसे सुख मिलता है या नहीं। इसी प्रकार दुःख के उपकरणों की प्राप्ति मात्र से घबरा नहीं जाना चाहिये। दुःखों के घोर उपकरणों को भी अपनी मानसिक वृत्तियों द्वारा सुख का साधन बनाया जा सकता है। जैसे विष यद्यपि मृत्यु का उपकरण है, तथापि बुद्धि के प्रयोग से वह रोग की निवृत्ति का उपकरण बन सकता है
क्या समाज के कर्मों का फल भोगना पड़ता है ?
प्रश्न- क्या ईश्वर मेरे समाज के किये हुए शुभ या अशुभ कर्मों का मुझ को फल नहीं देता ?
उत्तर-समाज तो आपका स्वयं नियत किया हुआ है आपकी अपनी कल्पना या व्यवस्था के अनुसार आपके समाज की भी सीमा है। समाज में तो अनेकों व्यक्ति होते हैं। अत: यदि समाज के शुभ या अशुभ कर्मों का आपको फल मिलने लगे तो घोर अन्याय हो जाय । प्रथम तो हर व्यक्ति का वश नहीं कि समाज के अन्य व्यक्तियों पर आधिपत्य कर सके। जिस पर मेरा वश नहीं, उस के कर्मों का फल मुझे क्यों मिले? ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर के न्याय और ईश्वर की दया तीनों में ऐसी बात बाधक होगी। अत: कर्म-फल का सिद्धान्त यही बताता है कि तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। 'तुम' का अर्थ है 'तुम व्यक्ति' न कि तुम से अन्य व्यक्ति। चाहे वह आपके समाज या देश के हों चाहे बाहर के ।
प्रश्न- क्या हम नहीं देखते कि हमारे मित्र हम को विपत्ति में सहायक होते हैं और हमारे शत्रु हमारे दुःखों को बढ़ाते हैं ?
उत्तर-यदि आप ईश्वर की व्यवस्था और ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखते हैं तो मानना पड़ेगा कि आपको आपके ही कर्मों का फल मिलेगा, अन्य किसी का नहीं। वह व्यवस्था व्यवस्था नहीं कहलायी जा सकती. जिसके भीतर बिना दोष के कोई आपको सताने 47


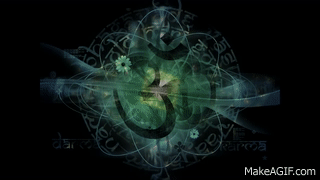




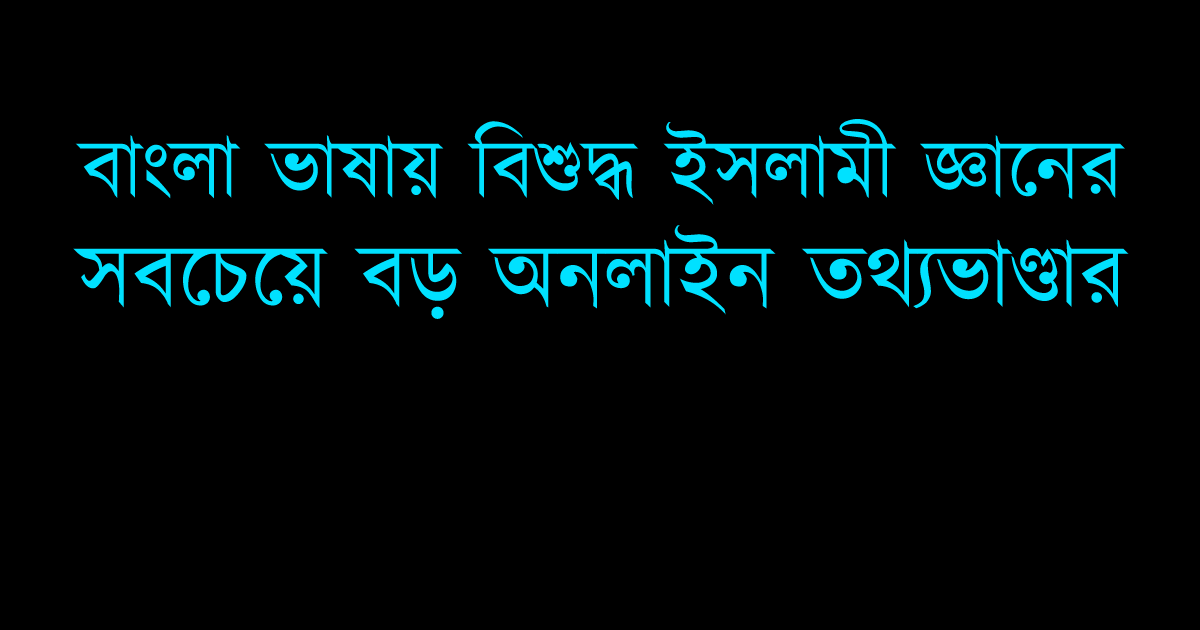

















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ