तदण्डं अभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम् ।
तस्मिञ् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । ।1/9
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
तब वह बीज स्वर्ण और सू्य्र्य के समान अष्ठाकार बन गया, फिर उससे ब्रह्माजी अर्थात् वेदों के ज्ञाता अयोनिज ऋषि जो समग्र सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, अपने आप उत्पन्न हुए।
आपो नरा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः । ।1/10
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
संस्कृत में ’अप’ मनुष्य की संतान को कहते हैं और मनुष्य की सन्तान के हृदय में परमात्मा का प्रकाश होता है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
जीव ‘नारा’ कहलाते हैं, क्योंकि वे नर (नायक परमात्मा) से प्रेरित होने के कारण उसके सूनु अर्थात् पुत्र हैं। यतः, ये ‘नारा’ नामक जीव इस नर के प्रथम अयन अर्थात् उत्तम निवास स्थान हैं, अतः सब जीवों में व्यापक होने से परमात्मा का नाम नारायण है।१ १. नाराः जीवाः अयनं निवासस्थानं अस्य सः नारायणः जीवेषु व्यापकः। -स०प्र०, स० १
यत्तत्कारणं अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते । ।1/11
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जो परमात्मा जगत् का उपादान है और छिपा हुआ है और नित्य सत्-असत् का कत्र्ता है, उसने जिस मनुष्य को संसार में सबसे पहिले चारों वेदों का ज्ञाता उत्पन्न किया, उसी को सब लोग ’ब्रह्मा’ कहते हैं।
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् ।
स्वयं एवात्मनो ध्यानात्तदण्डं अकरोद्द्विधा । ।1/12
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
ब्रह्मा अर्थात् वेद के जानने वाले ने उस अण्डे अर्थात् विराट् में एक वर्ष तक रह कर और परमात्मा का ध्यान करके उस अण्डे अर्थात् विराट् को दो भागों में विभक्त किया।
टिप्पणी :
* यहाँ पर एक वर्ष अण्डे में रहने से यह तात्पर्य है कि ब्रह्माजी ने वेदों के ज्ञान और सृष्टि के नियम की तुलना की और उस तुलना के पश्चात् तम (अन्धकार) और प्रकाश (अग्नि और पृथ्वी) दोनों के गुणों का ज्ञान संसार में फैलाया।
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ।
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् । ।1/13
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
उन दो टुकड़ों से ब्रह्म ने सतोगुण और पृथ्वी अर्थात् तमोगुण को बनाया, फिर उन दोनों के बीच में आकाश अर्थात् रजोगुण और आठों दिशायें-जीवों के रहने का स्थान-बनाया।
उद्बबर्हात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् ।
मनसश्चाप्यहंकारं अभिमन्तारं ईश्वरम् । ।1/14
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
फिर ब्रह्म ने परमात्मा से संकल्प-विकल्प रूप मन को उत्पन्न किया, और मन से सामथ्र्य और अभिमान करने वाले अहंकार को बनाया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(च) और फिर उस परमात्मा ने (आत्मनः एव) अपने आश्रय से अथवा स्वाश्रयस्थित प्रकृति से ही (सद् - असद् - आत्मकम) जो कारणरूप में विद्यमान रहे और विकारी अंश से कार्यरूप में जो अविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले (मत्) ‘महत्’ नामक तत्त्व को (च) और (मनसः अपि) महत्तत्त्व से (अभिमन्तारम्) ‘मैं हूँ’ ऐसा अभिमान करने वाले (ईश्वरम) सामथ्र्यशाली (अंहकारम्) ‘अहंकार’ नामक तत्त्व को (च) और फिर उससे (सर्वाणि त्रिगुणानि) सब त्रिगुणात्मक पांच तन्मात्राओं - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध को (च) तथा (आत्मानं एव महान्तम्) आत्मोपकारक अथवा निरन्तरगमनशील ‘मन’ इन्द्रिय को (च) और (विषयाणां ग्रहीतणि) विषयों को ग्रहण करने वाली (पंच्चेन्द्रियाणि) दोनों वर्गों की पांचों ज्ञानेन्द्रियों - आंख, नाक, कान, जिह्वा , त्वचा एवं कर्मेन्द्रियों - हाथ, पैर, वाक्, उपस्थ, पायु को (२।८९-९२) (शनैः) यथाक्रम से (उद्बबर्ह) उत्पन्न कर प्रकट किया ।
महान्तं एव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च ।
विषयाणां ग्रहीतॄणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च । ।1/15
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
और अहंकार से पहले आत्मा का उपकार करने वाले महत्तत्त्व अर्थात् बुद्धि को पैदा किया, तथा विषय को, भोग करने वाले-पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय एवं तन्मात्रा को बनाया।
टिप्पणी :
*पांच ज्ञानेन्द्रिय-आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा और पांच कर्मेन्द्रिय हाथ, पाँव, वाणी, मूत्रेन्द्रिय और मलद्वार।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(च) और फिर उस परमात्मा ने (आत्मनः एव) अपने आश्रय से अथवा स्वाश्रयस्थित प्रकृति से ही (सद् - असद् - आत्मकम) जो कारणरूप में विद्यमान रहे और विकारी अंश से कार्यरूप में जो अविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले (मत्) ‘महत्’ नामक तत्त्व को (च) और (मनसः अपि) महत्तत्त्व से (अभिमन्तारम्) ‘मैं हूँ’ ऐसा अभिमान करने वाले (ईश्वरम) सामथ्र्यशाली (अंहकारम्) ‘अहंकार’ नामक तत्त्व को (च) और फिर उससे (सर्वाणि त्रिगुणानि) सब त्रिगुणात्मक पांच तन्मात्राओं - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध को (च) तथा (आत्मानं एव महान्तम्) आत्मोपकारक अथवा निरन्तरगमनशील ‘मन’ इन्द्रिय को (च) और (विषयाणां ग्रहीतणि) विषयों को ग्रहण करने वाली (पंच्चेन्द्रियाणि) दोनों वर्गों की पांचों ज्ञानेन्द्रियों - आंख, नाक, कान, जिह्वा , त्वचा एवं कर्मेन्द्रियों - हाथ, पैर, वाक्, उपस्थ, पायु को (२।८९-९२) (शनैः) यथाक्रम से (उद्बबर्ह) उत्पन्न कर प्रकट किया ।
तेषां त्ववयवान्सूक्ष्मान्षण्णां अप्यमितौजसाम् ।
संनिवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे । ।1/16
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
और इन बड़े शक्तिमानों के सूक्ष्म अवयवों को अपने विकार में मिलाकर समस्त सृष्टि को बनाया। प्रकृति और परमात्मा के सम्बन्ध से सब तन्मात्रा अहंकार इन्द्रिय पैदा हुए हैं, अर्थात् परमात्मा और प्रकृति के योग से पैदा हुए हैं।
टिप्पणी :
*जब परमात्मा ने प्रकृति को संचालित किया, तब वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से आकाश उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसके बिना आकाश नहीं हो सकता। जब आकाश हुआ तब उसमें वायु संचालित हुई। वायु के संचालन के कारण अग्नि परमाणु एकत्रित हो गये। अग्नि-परमाणुओं के एकत्रित होने से जल-परमाणुओं के मध्य की रूकावट दूर हुई। जल-परमाणुओं के एकत्रित होने से पृथ्वी के परमाणु एकत्रित हो गए, इसी प्रकार सृष्टि की रचना हुई।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(औजसाम्) अनन्त शक्तिवाले (षण्णां अपि) छहों तत्त्वों के (सूक्ष्मान् अवयवान्) सूक्ष्म अवयवों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पांच तन्मात्रायें तथा छठे अहंकार के सूक्ष्म अवयवों) को (आत्ममात्रासु) उनके आत्मभूत तत्त्वों के विकारी अंशों अर्थात् कारणों में मिलाकर (सर्वभूतानि) सब पांचों महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी , की (निर्ममे) सृष्टि की ।
यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तानीमान्याश्रयन्ति षट् ।
तस्माच्छरीरं इत्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः । ।1/17
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
प्रकृति महत्ब्रह्म के शरीर के छः सूक्ष्म अवयव अर्थात् तन्मात्रा और अहंकार और इन्द्रियों के पैदा करने वाली है।
तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः ।
मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदव्ययम् । ।1/18
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
फिर उस अविनाशी और जगत् को रचने वाले परब्रह्म ने अपने-अपने कामों के साथ आकाश आदि सृष्टि तथा सूक्ष्म अवयवों के साथ मन को उत्पन्न किया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(तदा) तब जगत् के तत्त्वों की सृष्टि होने पर (सह कर्मभिः) अपने - अपने कर्मों के साथ (महान्ति भूतानि) शक्तिशाली सभी सूक्ष्म महाभूत (च) और (सूक्ष्मैः अवयवैः मनः) अपने सूक्ष्म अवयवों - इन्द्रियों और अहंकार के साथ मन (सर्वभूतकृद् अव्ययम्) सब प्राणियों को जन्म देने वाले अविनाशी आत्मा को (आविशन्ति) आवेष्टित करते हैं (और इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की रचना होती है ।)
तेषां इदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम् ।
सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्व्ययम् । ।1/19
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
इसके पश्चात् अविनाशी ब्रह्म ने उन सात बड़े पराक्रम रखने वाले महत्तत्त्व अहंकार और पांच तन्मात्राओं के सूक्ष्म भाग से इस नाश होने वाले जगत् को बनाया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
. (इस प्रकार) (अव्ययात्) विनाशरहित परमात्मा से (तेषां तु) उन्हीं (१४,१५ में वर्णित) (महौजसाम्) महाशक्तिशाली (सप्तानां पुरूषाणाम्) सात तत्त्वों - महत् , अहंकार तथा पाँच तन्मात्राओं के (सूक्ष्माभ्यः मूर्तिमात्राभ्यः) जगत् के पदार्थों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म विकारी अंशों से (इदम् व्ययम्) यह दृश्यमान विनाशशील समस्त जगत् (सम्भवति) उत्पन्न होता है ।
आद्याद्यस्य गुणं त्वेषां अवाप्नोति परः परः ।
यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मृतः । ।1/20
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
इन महाभूतों में पूर्व-पूर्व के गुणों को अगला-अगला ग्रहण करता है। जिसकी जैसी योग्यता है, उसमें वैसा गुण होता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(एषाम्) इन (२० वें में चर्चित) पंच्चमहाभूतों से (आद्य - आद्यस्य गुणं तु) पूर्व - पूर्व के भूतों के गुण को (परः परः) परला - परला अर्थात् उत्तरोत्तर बाद में आने वाला भूत प्राप्त करता है (च) और (यः यः) जो - जो भूत (यावतिथः) जिस संख्या पर स्थित है (सः सः) वह - वह (तावद्गुणः) उतने ही अधिक गुणों से युक्त (स्मृतः) माना गया है ।
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक् ।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे । ।1/21
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
फिर परमात्मा ने सब चीजों के नाम और कर्म पृथक्-पृथक्, जैसे पहिली सृष्टि में थे वैसे ही, वेद के द्वारा संसार में प्रकट किये।
टिप्पणी :
इससे यह प्रकट होता है कि यह संसार अब की ही बार नहीं बना, वरन् पहिले भी कई बार बन चुका है। जैसे दिन के पश्चात् रात और रात के पश्चात् दिन होता है, वैसे ही सृष्टि के पश्चात् प्रलय और प्रलय के पश्चात् सृष्टि होती है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
. (सः) उस परमात्मा ने (सर्वेषां तु नामानि) सब पदार्थों के नाम (यथा - गो - जाति का ‘गौ’, अश्वजाति का ‘अश्व’ आदि) (च) और (पृथक् - पृथक् कर्माणि) भिन्न - भिन्न कर्म (यथा - ब्राह्मण के वेदाध्यापन, याजन; क्षत्रिय का रक्षा करना; वैश्य का कृषि, गोरक्षा, व्यापार आदि (१।८७-९१) अथवा मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के हिंस्त्र - अहिंस्त्र आदि कर्म (१।२६-३०)) (च) तथा (पृथक् संस्थाः) पृथक् - पृथक् विभाग (जैसे - प्राणियों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि (१।४२-४९)) या व्यवस्थाएं (यथा - चारवर्णों की व्यवस्था (१।३१, १।४७-९१)) (आदौ) सृष्टि के प्रारम्भ में (वेदशब्देभ्यः एव) वेदों के शब्दों से ही (निर्ममे) बनायीं ।
टिप्पणी :
इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ने वेदों का अनुकरण करके जो व्यवस्था की, वह सर्वत्र प्रचलित है । उदाहरणार्थ - सब जगत् में सात ही बार हैं, बारह ही महीने हैं और बारह ही राशियां हैं, इस व्यवस्था को देखो (पू० प्र० ८९) (स्वामी जी ने उक्त श्लोक के बाद ये वाक्य कहे हैं) ।’’ वेद में भी कहा है - शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।। (यजु० ४०।८) ‘‘अर्थात् आदि सनातन जीवरूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ।’’ (स० प्र० अष्टम स०) उपसंहार रूप में समस्त जगत् की उत्पत्ति का वर्णन - १।२१ वें श्लोक की व्याख्या में कुल्लूकभट्ट ने पृथक् संस्थाः - पृथक् व्यवस्थाओं के उदाहरण में कुम्हार का घड़ा बनाना, जुलाहे का कपड़ा बनाना आदि उदाहरण दिये हैं, वे मनु के आशय से विरूद्ध हैं । क्यों कि मनु ने चार वर्णों की व्यवस्था ही मानी है । घड़ादि बनाना, कपड़ा बुननादि कार्य शिल्पकार्य के अन्तर्गत होने से वश्यवर्ण के ही विभिन्न कार्य हैं । अतः कुम्हारादि उपजातियों की मान्यता मनुसम्मत नहीं है । १।२१ वां श्लोक कभी मूल क्रम से पृथक् होकर स्थानान्तरित हो गया है । क्यों कि वेदों की उत्पत्ति १।२३ में बताई है । उसके पश्चात् ही इस श्लोक की संगति उचित हो सकती है । अन्यथा वेदों की उत्पत्ति से पूर्व ही वेदों से सब मनुष्यों के कर्मों का वर्णन करना कैसे संगत हो सकता है ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
उस नारायण ने सृष्टि की आदि में वेद के शब्दों से ही सब के पृथक्-पृथक् नाम और कर्म निर्मित किये तथा उनके पृथक-पृथक स्वरूप बनाए। अर्थात् उस प्रभु ने प्रत्येक पदार्थ के नाम, रूप, और कर्म का सत्य ज्ञान सृष्टि की आदि में वेद द्वारा उपदिष्ट किया।१ १. श्लोक ४ से २० तक के लिए ऋ० भू० वेदोत्पत्ति देखें।
कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः ।
साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् । ।1/22
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
वेद की उत्पत्ति के पश्चात् परमात्मा ने वेद के ज्ञाता देवऋषि और उनके सूक्ष्म अवयव शरीर और यज्ञ को बनाया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(इस प्रकार १।५-१२ श्लोकों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार) (सः प्रभुः) उस परमात्मा ने (कर्मात्मनां च देवानाम्) कर्म ही स्वभाव है जिनका ऐसे सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवों के (प्राणिनाम्) मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सामान्य प्राणियों के (च) और साध्यानाम् साधक कोटि के विशेष विद्वानों के (गणम्) समुदाय को (१।२३ में वर्णित) (च) तथा (सनातनं सूक्ष्म यज्ञम् एव) सृष्टि - उत्पत्ति काल से प्रलयकाल तक निरन्तर प्रवाहगमन सूक्ष्म संसार अर्थात् महत् अहंकार पंच्चतन्मात्रा आदि सूक्ष्म रूपमय और सूक्ष्मशक्तियों से युक्त संसार को (असृजत्) रचा ।
टिप्पणी :
. १।२२ वें श्लोक की व्याख्या में कुल्लूकभट्ट ने ‘साध्यानां च गणम्’ के साथ ‘सूक्ष्मम्’ पद को मिलाकर ‘सूक्ष्म देवयोनिविशेष’ अर्थ किया है । यह मनु के आशय से विरूद्ध तथा अशास्त्रीय मान्यता है । यथार्थ में मनुष्यों के ही देव, पितर, साध्य, ऋषि आदि ज्ञान - स्तर से भेद हैं । स्वंय मनु ने कर्म फल - व्यवस्था में लिखा है - ‘पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ।’ अर्थात् जो मध्यम सतोगुणी जीव होते हैं, वे मानवयोनि में पितर तथा साध्य कहलाते हैं । इसी प्रकार श्लोक - पठित ‘सूक्ष्मं यज्ञम्’ के अभिप्राय को न समझकर ‘द्रव्यमय हवन अर्थ भी असंगत है । यहाँ इस जगत् को भी ‘यज्ञ’ शब्द से कहा गया है परमात्मा ने इस यज्ञ - जगत् की सूक्ष्म रचना तथा चकार से स्थूल सर्वविध पदार्थों को रचा है । वेद के पुरूषसूक्त में सृष्टि - रचना को स्पष्ट रूप में ‘यज्ञ’ शब्द से ही कहा है । भगवान् मनु ने भी सृष्ट्युत्पत्ति प्रकरण में यज्ञ शब्द का ही प्रयोग किया है । और ‘सनातनम्’ विणेषण देकर प्रवाह से अनादि जगदू्रप यज्ञ की पुष्टि की है । और १।२३ श्लोक में वेदज्ञान का प्रयोजन ‘यज्ञसिद्धयर्थम् - जगत् के सब धर्मादिव्यवहारों की सिद्धि बताकर मनु ने ‘यज्ञ’ शब्दार्थ को स्पष्ट किया है । क्यों कि वेद का ज्ञान केवल द्रव्यमय हवन के लिये नहीं है । अतः कुल्लूकभट्ट की व्याख्या असंगत है ।’’
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुःसामलक्षणम् । ।1/23
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
फिर यज्ञ को पूरा कराने के लिए अग्नि, वायु आदि देवऋषियों के मन में वेद का प्रकाश किया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
. उस परमात्मा ने (यज्ञसिद्धयर्थम्) जगत् में समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए अथवा जगत् की सिद्धि अर्थात् जगत् के समस्त रूपों के ज्ञान के लिए (यज्ञे जगति प्राप्तव्या सिद्धिः यज्ञसिद्धिः, अथवा यज्ञस्य सिद्धिः यज्ञसिद्धिः) (अग्नि - वायु - रविभ्यः तु) अग्नि, वायु और रवि से (ऋग्यजुः सामलक्षणं त्रयं सनातनं ब्रह्म) ऋग् - ज्ञान, यजुः - कर्म , साम - उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले नित्य वेदों को (दुदोह) दुहकर प्रकट किया ।
टिप्पणी :
जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग्यजु साम और अथर्व का ग्रहण किया ।’’ (स० प्र० सप्तम स०) ‘‘अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्धयर्थ ऋग्यजुः सामलक्षणम् । १।२३ अध्यापयामास पितन् शिशुरांगिरसः कविः । २।१५१ (इस संस्करण में २।१२६) अर्थात् इसमं मनु के श्लोकों की भी साक्षी है कि पूर्वोक्त अग्नि, वायु, रवि और अंगिरा से ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था । जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि और हम लोगों की तो कथा क्या ही कहनी है ।’’ (ऋ० भू० वेदोत्पत्ति वि०) ‘‘मनु ने लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अग्नि, वायु, आदित्य, और अंगिरा इन चार ऋषियों से वेद सीख फिर आगे वेद का प्रचार किया ।’’ (पू० प्र० ४५) धर्म - अधर्म सुख - दुःख आदि का विभाग -
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
१. ‘पुरुषो वाव यज्ञः’ आदि प्रकरण में छान्दोग्य उपनिषद् ने पुरुष को यज्ञ कहा है। २. मनुस्मृतियों में यह श्लोक २ य अध्याय का १५१ वां है। ब्रह्मा ने यज्ञ की सिद्धि के लिए, अर्थात् मनुष्य-जीवन की सफलता के लिए अग्नि वायु तथा आदित्य ऋषियों से तो ऋग् यजु और साम नामक तीन सनातन वेदों को दुहा;
टिप्पणी :
२अध्यापयामास पितृन् शिशुराङ्गिरसः कविः। पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्॥ ६॥ और, अङ्गिरस् वेद के ज्ञाता बालक आङ्गिरस ऋषि ने उन ब्रह्मा आदि पितरों को अङ्गिरस् वेद (अथर्ववेद) पढ़ाया। एवं, ज्ञान के कारण उन्हें शिष्यभाव से ग्रहण करके पुत्र नाम से पुकारा।
कालं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा ।
सरितः सागराञ् शैलान्समानि विषमानि च । ।1/24
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
फिर काल और काल के भाग अर्थात् वर्ष, महीने, नक्षत्र और सूर्य आदि नवग्रह और नदी और समुद्र, सम-विषम स्थल उत्पन्न किये।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
(१।२४-२५) ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं । क्यों कि इनकी संगति इस प्रकरण से तथा मनु की शैली से विपरीत है । यहाँ प्रकरण वेदों के द्वारा कर्मों का ज्ञान कराने का (१।२१-२२ में) चल रहा था, २३ वें श्लोक में प्रसंगवश वेदोत्पत्ति को बताया गया और १।२६ श्लोक में फिर कर्मों का ही विवेचन किया गया है । अतः कर्मविवेक प्रकरण के बीच में नदी, सागर, नक्षत्र , ग्रहादि की सृष्टि की बात असंगत है । और प्राणियों की उत्पत्ति प्रथम कही जा चुकी है, फिर ‘स्त्रष्टुमिच्छन् इमाः प्रजाः’ कहने की क्या संगति है ? और काम, क्रोध, रति , तप आदि की रचना कहना भी निरर्थक ही है । अतः कतिपय दोषात्मक भावों के कथन की शैली मनु की प्रतीत नहीं होती । और मनु ने १।२९ वें श्लोक में हिंस्त्र - अहिंस्त्र, मृदु क्रूर, धर्म - अधर्म, तथा सत्य - असत्य प्राणियों के स्वभावों का वर्णन कर दिया है, अतः यहां पुनरक्त होने से भी यह मनु की रचना प्रतीत नहीं होती ।
तपो वाचं रतिं चैव कामं च क्रोधं एव च ।
सृष्टिं ससर्ज चैवेमां स्रष्टुं इच्छन्निमाः प्रजाः । ।1/25
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
इसके बनाने के बाद तप अर्थात् ¬प्रजापति इत्यादि गैर वाणी, रति अर्थात् चित्तों का सन्तोष, इच्छा, काम, क्रोध आदि प्रजा इन सबको बनाया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
(१।२४-२५) ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं । क्यों कि इनकी संगति इस प्रकरण से तथा मनु की शैली से विपरीत है । यहाँ प्रकरण वेदों के द्वारा कर्मों का ज्ञान कराने का (१।२१-२२ में) चल रहा था, २३ वें श्लोक में प्रसंगवश वेदोत्पत्ति को बताया गया और १।२६ श्लोक में फिर कर्मों का ही विवेचन किया गया है । अतः कर्मविवेक प्रकरण के बीच में नदी, सागर, नक्षत्र , ग्रहादि की सृष्टि की बात असंगत है । और प्राणियों की उत्पत्ति प्रथम कही जा चुकी है, फिर ‘स्त्रष्टुमिच्छन् इमाः प्रजाः’ कहने की क्या संगति है ? और काम, क्रोध, रति , तप आदि की रचना कहना भी निरर्थक ही है । अतः कतिपय दोषात्मक भावों के कथन की शैली मनु की प्रतीत नहीं होती । और मनु ने १।२९ वें श्लोक में हिंस्त्र - अहिंस्त्र, मृदु क्रूर, धर्म - अधर्म, तथा सत्य - असत्य प्राणियों के स्वभावों का वर्णन कर दिया है, अतः यहां पुनरक्त होने से भी यह मनु की रचना प्रतीत नहीं होती ।
कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मौ व्यवेचयत् ।
द्वन्द्वैरयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः । ।1/26
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
कर्मों के विवेक के लिये यज्ञ इत्यादि धर्म और ब्रह्महत्या आदि अधर्म अलग करके उनके सुख-दुःख देने वाले फल को प्रजा के पीछे बनाया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(च) और फिर (कर्मणां विवेकार्थम्) कर्मों के विवेचन के लिए (धर्म - अधर्मो) धर्म - अधर्म का (व्येचयत्) विभाग किया (च) तथा (इमाः प्रजाः) इन प्रजाओं को (सुख दुःखादिभिः द्वन्द्वैः) सुख - दुःख आदि द्वन्द्वों (दो विरोधी गुणों या अवस्थाओं के जोड़ों) से (अयोजयत्) संयुक्त किया । सूक्ष्म से स्थूल के क्रम से सृष्टि का वर्णन -
अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः ।
ताभिः सार्धं इदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः । ।1/27
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
क्रमशः सूक्ष्म अविनाशी तन्मात्रा वही हैं, उनके साथ इस सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(दशार्धानाम् तु) दश के आधे अर्थात् पांच महाभूतों की ही (याः) जो (विनाशिन्यः) विनाशशील अर्थात् अपने अहंकार कारण में लीन होकर नष्ट होने के स्वभाव वाली (अण्व्यः मात्राः स्मृताः) सूक्ष्म तन्मात्राएं कही गई हैं (ताभिः) उनके (सार्धं) साथ अर्थात् उनको मिलाकर ही (इदं सर्वम्) यह समस्त संसार (अनुपूर्वशः) क्रमशः - सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर, स्थूलतर से स्थूलतम के क्रम से (संभवति) उत्पन्न होता है ।
टिप्पणी :
१।२७ वां श्लोक भी किसी समय स्थानभ्रष्ट हो गया है । क्यों कि इससे पूर्व श्लोक १।२६ में कर्मों का विवेचन किया गया है । और १।२८ में भी कर्मों का कथन है । इनके बीच में सूक्ष्म मात्राओं के साथ जगदुत्पत्तिवर्णन कैसे संगत हो सकता है । इस श्लोक की संगति सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में १।१९ श्लोक के पश्चात् १।२१ से पूर्व ही होनी चाहिये । क्यों कि जगत्, मानव तथा वेदों की उत्पत्ति के बाद सूक्ष्ममात्राओं का वर्णन संगत नहीं हो सकता ।
यं तु कर्मणि यस्मिन्स न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः ।
स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः । ।1/28
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
परमात्मा ने जिस-जिस प्राणी को सृष्टि के आदि में जिस-जिस कर्म में लगाया, वह आज तक वैसे ही कर्म करता है, मनुष्य के अतिरिक्त सब भोग योनि कहलाते हैं।
टिप्पणी :
यथा इस संसार में प्राणी परतंत्र अथवा स्वतन्त्र है और स्वतन्त्र मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करता है और उन कर्मों के हानि-लाभ का भोक्ता होता है। परतंत्र न अपनी इच्छानुसार कर्म करता है और न उनके हानि लाभ का उत्तरदाता है। वैसे ही स्वतन्त्र मनुष्य अपनी इच्छानुसार कर्म करता है और उनके फल को भोगता है जबकि पशु आदि न अपनी इच्छा से कर्म करते हैं और न उनके फल भोगते हैं। अर्थात् पशु आदि शरीर जीवों के लिए बन्दीगृह हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(सः प्रभुः) उस परमात्मा ने (प्रथमम्) सृष्टि के आरम्भ में (यं तु) जिस प्राणी को (यस्मिन् कर्मणि) जिस कर्म में (न्ययुड्क्त) लगाया (सः) वह फिर (पुनः पुनः) बार - बार (सृज्यमानः) उत्पन्न होता हुआ (तदेव) उसी कर्म को ही (स्वयम्) अपने आप (भेजे) प्राप्त करने लगा ।
हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृतानृते ।
यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे तत्तस्य स्वयं आविशत् । ।1/29
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
हिंस्र और अहिंस्र, मृदु और कठोर आदि गुण वाले पशुओं में ये गुण अनादि काल से चले आते हैं, केवल कर्मों का परिवर्तन मनुष्य को दिया है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(हिंस्त्र - अहिंस्त्रे) हिंसा (सिंह, व्याघ्र आदि का) अहिंसा (मृग आदि का) (मृदु - क्रूरे) दयायुक्त और कठोरतायुक्त (धर्म - अधर्मो) धर्म तथा अधर्म (अनृत - ऋते) असत्य और सत्य (यस्य) जिस प्राणी का (यत्) जो कर्म (सर्गे) सृष्टि के प्रारम्भ में (सः अदधात्) उस परमात्मा ने धारण कराना था (तस्य तत्) उसको वही कर्म (स्वयम्) अपने आप ही (आविशत्) प्राप्त हो गया ।
यथा र्तुलिङ्गान्यृतवः स्वयं एव र्तुपर्यये ।
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः । ।1/30
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जैसे बसन्त आदि ऋतु अपने-अपने समय पर अपने गुणों को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सब प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
. (यथा) जैसे (ऋतवः) ऋतुएं (ऋतुपर्यये) ऋतु - परिवर्तन होने पर (स्वयम् एव) अपने आप ही (ऋतुलिंगानि) अपने - अपने ऋतुचिन्हों - जैसे, वसन्त आने पर कुसुम - विकास, आम्रमंज्जरी आदि को (अभिपद्यन्ते) प्राप्त करती हैं (तथा) उसी प्रकार (देहिनः) देहधारी प्राणी भी (स्वानि - स्वानि कर्माणि) अपने - अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं ।
लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहूरुपादतः ।
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् । ।1/31
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर के चार हिस्से गुण-कर्म से अलग-अलग हैं, ऐेसे ही सारे जगत् में मनुष्य जाति के चार विभाग गुण-कर्म से अलग-अलग हैं। जिस तरह मुख वाले हिस्से में पाँचों ज्ञानेन्द्रिय और उपदेश करने के लिए वाणी कर्मेन्द्रिय है, ऐसे ही ब्राह्मण को उपदेश का काम दिया गया, बाहु अर्थात् क्षत्रिय को रक्षा का काम दिया गया, उरु अर्थात् वैश्य को व्यापार का एवं पाद अर्थात् शूद्र को सेवा का काम दिया गया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(फिर उस परमात्मा ने) (लोकानां तु) प्रजाओं अर्थात् समाज की (विबृद्धयर्थम्) विशेष वृद्धि - शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए (मुखबाहु - ऊरू - पादतः) मुख, बाहु, जंघा और पैर की तुलना के अनुसार क्रमशः (ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं च शूद्रम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण को (निरवर्तयत्) निर्मित किया ।
टिप्पणी :
. १।३१ वें श्लोक की व्याख्या में कुल्लूकभट्ट ने पौराणिक - प्रभाव वश सृष्टि - क्रम से विरूद्ध एक अविश्वसनीय कल्पना की है । अर्थात् ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैर से शूद्र पैदा हुआ । और इस मिथ्या कल्पना को बल देने के लिये यह भी लिख दिया कि ‘दैव्या च शक्त्या मुखादिभ्यो ब्राह्मणादिनिर्माणं ब्रह्मणों न विशंकनींय श्रुतिसिद्धत्वात्’ अर्थात् ब्रह्मा के मुखादि से ब्राह्मणादि की उत्पत्ति में किसी प्रकार की आशंका न करनी चाहिये । क्यों कि दिव्य - शक्ति से ऐसा भी सम्भव है और इसमें वेद का प्रमाण भी है । वस्तुतः वेद के ‘ब्राह्माणोऽस्य मुखमासीद्०’ इत्यादि मन्त्र के आलंकारिक वर्णनों को न समझकर ऐसी कल्पना की गई है । यहाँ शरीर की उपमा से ब्राह्मणादि वर्णों के विभाग तथा कर्मों को ही समझाया गया है । और यदि मुखादि से उत्पत्ति का क्रम माना जाये तो अनेक दोष आते हैं -- जैसे - १।१६,१९,२२ श्लोकों में जो मनुष्यादि की उत्पत्ति कही है, फिर यहाँ कहने की क्या आवश्यकता है क्या पूर्वकथित मानवादि की उत्पत्ति ब्राह्मणादि से भिन्न है ? उनको क्या वर्ण होंगे ? यदि मुखादि अवयवों से उत्पत्ति हुई , तो प्रथम तो परमात्मा का शरीर ही नहीं है, मुखादि अवयव कैसे हो सकते हैं । और दुर्जनतोष न्याय से अवयवों से उत्पत्ति मान भी लो तो मुख से उत्पन्न होने से ब्राह्मण गोलाकार, क्षत्रिय हाथ की भांति लम्बा , वैश्य उदर की तरह गोल - मटोल , शूद्र पैर की भांति ऊपर से मोटा नीचे से पतला लम्बा होना चाहिये । कुछ तो उत्पत्ति - भेद से इनकी बनावट में भेद होना चाहिये ? अतः मुखादि से उत्पत्ति की बात न तो बुद्धिसंगत है और न सृष्टिक्रम से अनुकूल । और जन्ममूलक वर्णव्यवस्था के पक्ष में यह भी दोष है कि ब्रह्मा के शरीर से ही उत्पन्न चारों, वर्णों का भेद ही क्यों माना जाये ? सभी को एक वर्ण का मानना चाहिये, चाहे वह मुख से हुआ, अथवा दूसरे अंगों से । क्यों कि सब की उत्पत्ति एक ब्रह्मा से मानी गई है । अतः इस प्रकार की व्याख्या सर्वथा असंगत है ।
द्विधा कृत्वात्मनो देहं अर्धेन पुरुषोऽभवत् ।
अर्धेन नारी तस्यां स विराजं असृजत्प्रभुः । ।1/32
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
फिर परमात्मा ने मनुष्य जाति को स्त्री और पुरुष के रूप में, दो भागों में विभक्त किया। दोनों को मिलाकर विराट् अर्थात् मनुष्य जाति भी कह सकते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
तपस्तप्त्वासृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट् ।
तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः । ।1/33
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
मनुजी कहते हैं कि हे ऋषियों ! उस विराट् ने तपस्या करके जिसको बनाया, वह मैं हूँ और मैं सबका पैदा करने वाला हूँ, यह बात आप लोग जानिये।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् ।
पतीन्प्रजानां असृजं महर्षीनादितो दश । ।1/34
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
फिर मैंने सृष्टि को पैदा करने की इच्छा से घोर तपस्या करके दस ऋषियों को, जो प्रजा के पति हैं, पैदा किया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
मरीचिं अत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् ।
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदं एव च । ।1/35
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलात्य, पुलह, कृतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
एते मनूंस्तु सप्तान्यानसृजन्भूरितेजसः ।
देवान्देवनिकायांश्च महर्षींश्चामितौजसः । ।1/36
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
इन ऋषियों ने सात बड़े तेजस्वी मनु और देवताओं और देवताओं के स्थान अर्थात् स्वर्ग और महाप्रतापी बड़े-बड़े ऋषियों को उत्पन्न किया।
टिप्पणी :
मनु से तात्पर्य मन्वन्तर अर्थात् जगत के चैदहवें भाग से है और उसमें जो सबसे बड़ा और बुद्धिमान् उत्पन्न होता है, वह मनु कहलाता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् ।
नागान्सर्पान्सुपर्णांश्च पितॄणांश्च पृथग्गणम् । ।1/37
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
और यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, असुर, साँप, गरूड़ और पितरों के वर्ग बनाये।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च ।
उल्कानिर्घातकेतूंश्च ज्योतींष्युच्चावचानि च । ।1/38
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
तत्पश्चात् विद्युत् (बिजली), मेघ (बादल), रोहित, धनुष, हल्का (लक का टूटना), स्थिति और परिभ्रमण करने वाले नक्षत्र, केतु और ध्रुव आदि को बनाया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान् ।
पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः । ।1/39
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
फिर किन्नर, वानर, मत्स्य (मछली) भाँति-भाँति के पक्षी, हशु, मृग, मनुष्य और दो दांत वाले व्याल (साँप) को रचा।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
कृमिकीटपतङ्गांश्च यूकामक्षिकमत्कुणम् ।
सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् । ।1/40
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
कृमि व कीट (बड़े 2 और 2 कीड़े), पतंग (शलभ), खटमल, मक्षिक (मक्खी), दंश, मशक (डास) और भाँति-भाँति के स्थाबरों (अचल वृक्षों) को बनाया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
एवं एतैरिदं सर्वं मन्नियोगान्महात्मभिः ।
यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम् । ।1/41
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
मनुजी कहते हैं कि इस प्रकार बड़े 2 ऋषियों ने अपने तप और योग के प्रभाव से हमारी आज्ञा पाकर जीवों को कर्मानुसार स्थावर (अचर) और जड्गम (चर) बनाया।
टिप्पणी :
यहां बड़े 2 ऋषियों से तात्पर्य सांकल्पिक सृष्टि के दो ऋषियों से है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
येषां तु यादृषं कर्म भूतानां इह कीर्तितम् ।
तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि । ।1/42
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जिन जीवों को जैसा कर्म इस संसार से पहिले प्राचार्यों ने कहा है उन जीवों का वैसा ही कर्म और जन्म-मरण का भी कर्म हम आप सबसे कहेंगे।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(इह) इस संसार में (येषां भूतानाम्) जिन मनुष्यों का - वर्णंगत मनुष्यों का (यादृशं कर्म) जैसा कर्म (कीर्तितम्) वेदों में कहा है (तत्) उसे (तथा) वैसे ही (१।८७-९१) (च) और (जन्मनि) उत्पन्न होने में (क्रमयोगम्) जीवों का जो एक निश्चित प्रकार रहता है , उसे (वः) आप लोगों को (अभिधास्यामि) कहूँगा ।
पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः ।
रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः । ।1/43
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
पशु, मृग (हिरन), दो दाँत धारी व्याल (साँप), राक्षस, पिशाच, मनुष्य यह सब जरायुज (गर्भ से उत्पन्न होने वाले) हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(पशवः) ग्राम्यपशु गौ आदि (मृगाः) अहिंसक वृत्ति वाले वन्यपशु हिरण आदि (च) और (उभयोदतः व्यालाः) दोनों ओर दांत वाले हिंसक वृत्तिवाले पशु सिहं, व्याघ्र आदि (च) तथा (रक्षांसि) राक्षस (पिशाचाः) पिशाच (च) तथा (मनुष्य) (जरायुजाः) ये सब ‘जरायुज’ अर्थात् झिल्ली से पैदा होने वाले हैं ।
अण्डाजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः ।
यानि चैवंः प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च । ।1/44
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
पक्षी, साँप, मछली, कछुवा यह सब अण्डज (अंडे से उत्पन्न होने वाले) हैं। इसी प्रकार जो स्थल (पृथ्वी) तथा उदक (जल) से उत्पन्न होते हैं। वे भी सब अण्डज हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(पक्षिणः) पक्षी (सर्पाः) सांप (नक्राः) मगरमच्छ (मत्स्याः) मछलियां (च) तथा (कच्छपाः) कछुए (च) और (यानि) अन्य जो एवं (प्रकाराणि) इस प्रकार के (स्थलजानि) भूमि पर रहने वाले (च) और (औदकानि) जल में रहने वाले जीव हैं, वे सब (अण्डजाः) ‘अण्डज’ अर्थात् अण्डे से उत्पन्न होने वाले हैं ।
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम् ।
ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किं चिदीदृषम् । ।1/45
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
डंश (दंश), मशक (मच्छर), जुँआ (डील, यूक), मक्खी व खटमल, यह सब स्वेद (पसीना) से उत्पन्न होते हैं। अतः इन्हें स्वेदज कहते हैं और जो ऐसे ही गर्मी से उत्पन्न होते हैं, वह भी स्वेदज कहलाते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(दशंमशकम्) डंक से काटने वाले मच्छर आदि (यूका) जूं (मक्षिक) मक्खियां (मत्कुणम्) खटमल (यत् च अन्यत् किंच्चित् ईदृशम्) जो और भी कोई इस प्रकार के जीव हैं जो (ऊष्मणः) ऊष्मा अर्थात् सीलन और गर्मी से (उपजायन्ते) पैदा होते हैं, वे सब (स्वेदजम्) ‘स्वेदज’ अर्थात् पसीने से उत्पन्न होने वाले कहाते हैं ।
उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः ।
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः । ।1/46
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
सब स्थावर उदिभज कहाते हैं। कोई बीज से उत्पन्न होता है कोई कलम लगाने से होता है।
टिप्पणी :
जो पृथ्वी फोड़कर निकलते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(बीजकाण्डप्ररोहिणः) बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले (सर्वे स्थावराः) सब स्थावर (एक स्थान पर टिके रहने वाले) जीव वृक्ष आदि (उद्भिज्जाः) ‘उद्भिज’ - भूमि को फाड़कर उगने वाले कहाते हैं । इनमें - (फल - पाकान्ता) फल आने पर पककर सूख जाने वाले और (बहुपुष्पफलोपगाः) जिन पर बहुत फूल - फल लगते हैं , वे ‘ओषधि’ कहलाते हैं ।
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ।
पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः । ।1/47
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
फल-फूल वाले जो पकने पर नाश होते हैं, औषध कहलाते हैं। जिनमें फूल नहीं लगता, केवल फल ही लगता है उन्हें वनस्पति कहते हैं। जिनमें फल-फूल दोनों लगते हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(ये अपुष्पाः फलवन्तः) जिन पर बिना फूल आये ही फल लगते हैं (ते) वे (वनस्पतयः स्मृताः) ‘वनस्पतियाँ’ कहलाती हैं (जैसे - बड़ (वट), पीपल, गलूर आदि) (च) और (पुष्पिणः फलिनः एव) फूल लगकर फल लगने वाले (उभयतः) दोनों से युक्त होने के कारण (वृक्षाः) वे उद्धिज्ज स्थावर जीव ‘वृक्ष’ (स्मृताः) कहलाते हैं ।
गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः ।
बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च । ।1/48
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
गुच्छ* और गुल्म** बहुत प्रकार के होते हैं और तृण कोई तो बीज लगाने से होते हैं, कोई शाखा लगाने से होते हैं जैसे प्रताना बल्ली*** आदि।
टिप्पणी :
*जिनमें जड़ लता से निकलती है और शाखा बड़ी नहीं होती। ** जिनमें जड़ एक है परन्तु रेशे (जड़ के डोरे) बहुत निकलते हैं। *** जिनमें सोत होता है यथा लौकी, कुम्हड़ा आदि।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
विविधम्) अनेक प्रकार के (गुच्छ) जड़ से गुच्छे के रूप में बनने वाले ‘झाड़’ आदि (गुल्मम्) एक जड़ से अनेक भागों में फूटने वाले ‘ईख’ आदि (तथैव) उसी प्रकार (तृणजातयः) घास की सब जातियां, (बीज - काण्डरूहाणि) बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले (प्रतानाः) उगकर फैलने वाली ‘दूब’ आदि (च) और (वल्ल्यः) उगकर किसी का सहारा लेकर चढ़ने वाली बेलें (एव) ये सब स्थावर भी ‘उद्धिज्ज’ कहलाते हैं ।
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः ।
घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि । ।1/50
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
इस नाशवान् संसार में ब्रह्मा से चींटी पय्र्यनत जीवों की जो दशा है, वह हमने आप लोगों से वर्णन कर दी।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।५०-५१ श्लोक निम्नकारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक ब्रह्मा की उत्पत्ति से सम्बद्ध होने से असंगत हैं, क्यों कि ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन पहले प्रक्षिप्त सिद्ध हो चुका है । और जब परमात्मा द्वारा सृष्टि रचने की प्रक्रिया का वर्णन १।८० तक चल रहा है, उसके बीच में ही ब्रह्मा का अन्तर्धान बताकर सृष्टि - रचना के क्रम की समाप्ति बताना कैसे संगत हो सकता है ? इससे यह स्पष्ट है कि ये श्लोक किसी ने बाद में मिलाये हैं । ब्रह्मा कौन है ? क्या परमात्मा से भिन्न है, जो शरीर धारणकर सृष्टि - रचना करके अन्तर्धान हो जाता है । अवयक्त परमात्मा सृष्टि रचयिता है, ब्रह्मा नहीं । दोनों को मानने में दोनों बातें सत्य नहीं हो सकतीं । और परमात्मा ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण नहीं कर सकता, क्यों कि वह अकाय - शरीर रहित तथा अज - अजन्मा है । और मनु में १।५२-५४ श्लोकों में सृष्टि के वर्तमान को जागृत - दशा तथा प्रलय को परमात्मा की निद्रावस्था बताया है । किन्तु इन श्लोकों में सृष्टि को बनाकर ही उसका अन्र्धान लिखा है, यह परस्पर विरूद्ध होने से मान्य नहीं हो सकता । और १।६८-७३ श्लोकों में ४ अरब ३२ करोड़ वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन माना है, यदि ब्रह्मा शब्द से पूर्वोक्त शरीरधारी ब्रह्मा लिया जाये, तब भी उसे दिन भर जागना चाहिये, फिर उसका अन्तर्धान क्यों ? यथार्थ में ब्राह्मदिन आदि शब्द वर्ष - प्रमाण के वाची हैं , ब्रह्म के नहीं ।
एवं सर्वं स सृष्ट्वेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः ।
आत्मन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन् । ।1/51
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
इस प्रकार ब्रह्माजी अचिन्त्य पराक्रमी मुझको और सृष्टि को रच कर प्रलय के समय सब को नाश करके ब्रह्म में मिल जाते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।५०-५१ श्लोक निम्नकारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक ब्रह्मा की उत्पत्ति से सम्बद्ध होने से असंगत हैं, क्यों कि ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन पहले प्रक्षिप्त सिद्ध हो चुका है । और जब परमात्मा द्वारा सृष्टि रचने की प्रक्रिया का वर्णन १।८० तक चल रहा है, उसके बीच में ही ब्रह्मा का अन्तर्धान बताकर सृष्टि - रचना के क्रम की समाप्ति बताना कैसे संगत हो सकता है ? इससे यह स्पष्ट है कि ये श्लोक किसी ने बाद में मिलाये हैं । ब्रह्मा कौन है ? क्या परमात्मा से भिन्न है, जो शरीर धारणकर सृष्टि - रचना करके अन्तर्धान हो जाता है । अवयक्त परमात्मा सृष्टि रचयिता है, ब्रह्मा नहीं । दोनों को मानने में दोनों बातें सत्य नहीं हो सकतीं । और परमात्मा ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण नहीं कर सकता, क्यों कि वह अकाय - शरीर रहित तथा अज - अजन्मा है । और मनु में १।५२-५४ श्लोकों में सृष्टि के वर्तमान को जागृत - दशा तथा प्रलय को परमात्मा की निद्रावस्था बताया है । किन्तु इन श्लोकों में सृष्टि को बनाकर ही उसका अन्र्धान लिखा है, यह परस्पर विरूद्ध होने से मान्य नहीं हो सकता । और १।६८-७३ श्लोकों में ४ अरब ३२ करोड़ वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन माना है, यदि ब्रह्मा शब्द से पूर्वोक्त शरीरधारी ब्रह्मा लिया जाये, तब भी उसे दिन भर जागना चाहिये, फिर उसका अन्तर्धान क्यों ? यथार्थ में ब्राह्मदिन आदि शब्द वर्ष - प्रमाण के वाची हैं , ब्रह्म के नहीं ।
यदा स देवो जागर्ति तदेवं चेष्टते जगत् ।
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलति । ।1/52
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जब तक जीवात्मा जाग्रत रहता है, तब तक यह जगत् दृष्ठिगोचर होता है और जब वह शान्त पुरुष अर्थात् जीवात्मा निद्रा के वशीभूत हो जाता है तब प्रलय हो जाता है।
टिप्पणी :
वह नित्य प्रलय कहलाता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(यदा) जब (सः देवः) वह परमात्मा (१।६ में वर्णित) (जागर्ति) जागता है अर्थात् सृष्ट्युत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता है (तदा) तब (इदं जगत् चेष्टते) यह समस्त संसार चेष्टायुक्त (प्रकृति से समस्त विकृतियों की उत्पत्ति पुनः प्राणियों का श्वास - प्रश्वास चलना आदि चेष्टाओं से युक्त) होता है, (यदा) और जब (शान्तात्मा) यह शान्त आत्मावाला सभी कार्यों से शान्त होकर (स्वपिति) सोता है अर्थात् सृष्टि - उत्पत्ति, स्थिति से निवृत्त हो जाता है (तदा) तब (सर्वम्) यह समस्त संसार (निमीलति) प्रलय को प्राप्त हो जाता है ।
तस्मिन्स्वपिति तु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः ।
स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिं ऋच्छति । ।1/53
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जीवात्मा जब प्रगाढ़ निद्रा में अचिन्त्य दशा को प्राप्त हो जाता है, तब इन्द्रिय और मन अपने कर्म से मुक्त हो जाते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(सुस्थे) सृष्टि - कर्म से निवृत्त हुए (तस्मिन् स्वपिति तु) उस परमात्मा के सोने पर (कर्मात्मानः) कर्मों - श्वास - प्रश्वास, चलना - सोना आदि कर्मों में लगे रहने का स्वभाव है जिनका, ऐसे (शरीरिणः) देहधारी जीव भी (स्वकर्मभ्यः, निवर्तन्ते) अपने - अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं (च) और (मनः) ‘महत्’ तत्त्व (ग्लानिम्) उदासीनता - सब कार्य - व्यापारों से विरत होने की अवस्था को या अपने कारण में लीन होने की अवस्था को (ऋच्छति) प्राप्त करता है ।
युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि ।
तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वृतः । ।1/54
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जब सब इन्द्रियाँ और मन जीवात्मा में लय हो जाते हैं, तब यह पंचभूतों का आत्मा आनन्द से सोता है अर्थात् तब महाप्रलय होता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(तस्मिन् महात्मनि) उस सर्वव्यापक परमात्मा के आश्रय में (यदा) जब (युगपत् तु प्रलीयन्ते) एक साथ ही सब प्राणी चेष्टाहीन होकर लीन हो जाते हैं (तदा) तब (अयं सर्वभूतात्मा) यह सब प्राणियों का आश्रयस्थान परमात्मा (निर्वृतः) सृष्टि - संचालन के कार्यों से निवृत्त हुआ - हुआ (सुखं स्वपिति) सुख पूर्वक सोता है ।
तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः ।
न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूर्तितः । ।1/55
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
अब मृत की दशा लिखते हैं कि यह जीव चिरकाल के इन्द्रियों के संसर्ग से मूढ़ दशा में रहता है और जब प्राण निकल जाता है तो जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।५५-५६ श्लोक निम्न - आधार से प्रक्षिप्त हैं - इन दोनों श्लोकों में नवीन - वेदान्त की मिथ्या मान्यता का वर्णन है अर्थात् यह जीवात्म अज्ञानवश इन्द्रियसहित शरीर में रहता है, यह स्वयं कुछ भी कर्म नहीं करता, अणुमात्रिक होकर स्थावर - जंगम - जगत् में बीज रूप में प्रवेश करता है, इत्यादि । मनु की मान्यता अद्वैतवाद की कहीं भी नहीं हैं । और पूर्वापर प्रसंग से भी ये श्लोक असंगत हैं । १।५२-५४ तक जागृत तथा सुषुप्तिदशाओं का वर्णन है और १।५७ श्लोक में उन्हीं दशाओं का उपसंहार किया है, अतः बीच में उनसे असम्बद्ध श्लोकों की क्या संगति हो सकती है ?
यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च ।
समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिं विमुञ्चति । ।1/56
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
और जब वह पंचभूत (पंचतत्त्व), इन्द्रियों, हृदय, बुद्धि, इच्छा, कर्म और मूढ़ता इन आठ वस्तुओं के संसर्ग से अचल बीज में जाता है, तब वृक्षादि की योनि पाता है और जब चल बीज में जाता है, तब मनुष्यादि की योनि अर्थात् शरीर पाता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।५५-५६ श्लोक निम्न - आधार से प्रक्षिप्त हैं - इन दोनों श्लोकों में नवीन - वेदान्त की मिथ्या मान्यता का वर्णन है अर्थात् यह जीवात्म अज्ञानवश इन्द्रियसहित शरीर में रहता है, यह स्वयं कुछ भी कर्म नहीं करता, अणुमात्रिक होकर स्थावर - जंगम - जगत् में बीज रूप में प्रवेश करता है, इत्यादि । मनु की मान्यता अद्वैतवाद की कहीं भी नहीं हैं । और पूर्वापर प्रसंग से भी ये श्लोक असंगत हैं । १।५२-५४ तक जागृत तथा सुषुप्तिदशाओं का वर्णन है और १।५७ श्लोक में उन्हीं दशाओं का उपसंहार किया है, अतः बीच में उनसे असम्बद्ध श्लोकों की क्या संगति हो सकती है ?
एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यां इदं सर्वं चराचरम् ।
संजीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः । ।1/57
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
इसी प्रकार ब्रह्माजी जाग्रत् और निद्रित दशा में होने से सब चर और अचर जीवधारियों को बार बार उत्पन्न करते और नाश करते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(सः अव्ययः) वह अविनाशी परमात्मा (एवम्) इस प्रकार (५१-५४ के अनुसार) (जाग्रत् - स्वप्नाभ्याम्) जागने और सोने की अवस्थाओं के द्वारा (इदं सर्वं चर - अचरम्) इस समस्त जड़ चेतन जगत् को क्रमशः (अजस्त्रं संज्जीवयति) प्रलयकाल तक निरन्तर जिलाता है (च) और फिर (प्रमापयति) मारता है अर्थात् कारण में लीन करता है ।
इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मां एव स्वयं आदितः ।
विधिवद्ग्राहयां आस मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् । ।1/58
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
ब्रह्मा ने इस शास्त्र को बनाकर पहले हमको बुद्धि के अनुसार बतलाया। फिर हमने मरीचि आदि ऋषियों को सिखलाया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।५८-६३ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।५२-५७ तक श्लोकों में परमात्मा की जाग्रत - सुषुप्ति दशाओं का वर्णन है और १।६४-७३ तक श्लोकों में इन अवस्थाओं की अवधि (दिन - रात - सृष्टि - प्रलय के परिमाण वर्षों का) का वर्णन है । इस प्रकार पूर्वापर का प्रसंग है, उससे विरूद्ध इन बीच के श्लोकों का अप्रासंगिक वर्णन किया गया है । और मनुस्मृति के रचयिता मनु हैं, किन्तु इन श्लोकों में ‘इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ’ कहकर ब्रह्मा को मूल रचयिता बताया है । यह ब्रह्मा से सृष्टि रचना मानने वालों ने बाद में प्रसंग को जोड़ने का ही दुस्साहस किया है । जब ऋषियों ने ।१-४ श्लोकों में मनु से धर्म के लिये प्रार्थना की है, तो ब्रह्मा कहाँ से आ गये ? यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान मनु को प्राप्त होता तो मनु अवश्य ही इसकी चर्चा कहीं तो करते ? अतः इस शास्त्र के मूल - प्रवक्ता मनु ही हैं । और इन श्लोकों में मनुस्मृति को ‘शास्त्र’ नाम से लिखा है, यह व्यवहार भी यथार्थ में अर्वाचीन है । मनुस्मृति तो प्रवचन रूप ही थी, जैसे - वक्तुमर्हसि (१।२) श्रूयताम् (१।४२) तं निबोधत (६।१२०) विधानं श्रूयताम् (३।२८६) इत्यादि श्लोकों से स्पष्ट है । अतः इसका ‘शास्त्र’ नाम बाद में प्रचलित हुआ, जब इसको संकलन करके ग्रन्थरूप में निबद्ध कर दिया गया । और १।६३ श्लोक में मनुओं द्वारा चराचर जगत् की उत्पत्ति का कथन भी पूर्वापर से विरूद्ध है । जब पीछे अव्यक्त परमात्मा से जगदुत्पत्ति कही जा चुकी है, तो यह पुनरूक्ति क्यों ? और क्या कोई शरीरधारी जीव चराचर जगत् की रचना कर सकता है ? यह सब शास्त्रों से विरूद्ध मान्यता है । और मनु सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए, वे अपने से बाद में होने वाले स्वायम्भुवादि सात मनुओं का वर्णन कैसे कर सकते हैं ?
एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेसतः ।
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वं एषोऽखिलं मुनिः । ।1/59
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।५८-६३ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।५२-५७ तक श्लोकों में परमात्मा की जाग्रत - सुषुप्ति दशाओं का वर्णन है और १।६४-७३ तक श्लोकों में इन अवस्थाओं की अवधि (दिन - रात - सृष्टि - प्रलय के परिमाण वर्षों का) का वर्णन है । इस प्रकार पूर्वापर का प्रसंग है, उससे विरूद्ध इन बीच के श्लोकों का अप्रासंगिक वर्णन किया गया है । और मनुस्मृति के रचयिता मनु हैं, किन्तु इन श्लोकों में ‘इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ’ कहकर ब्रह्मा को मूल रचयिता बताया है । यह ब्रह्मा से सृष्टि रचना मानने वालों ने बाद में प्रसंग को जोड़ने का ही दुस्साहस किया है । जब ऋषियों ने ।१-४ श्लोकों में मनु से धर्म के लिये प्रार्थना की है, तो ब्रह्मा कहाँ से आ गये ? यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान मनु को प्राप्त होता तो मनु अवश्य ही इसकी चर्चा कहीं तो करते ? अतः इस शास्त्र के मूल - प्रवक्ता मनु ही हैं । और इन श्लोकों में मनुस्मृति को ‘शास्त्र’ नाम से लिखा है, यह व्यवहार भी यथार्थ में अर्वाचीन है । मनुस्मृति तो प्रवचन रूप ही थी, जैसे - वक्तुमर्हसि (१।२) श्रूयताम् (१।४२) तं निबोधत (६।१२०) विधानं श्रूयताम् (३।२८६) इत्यादि श्लोकों से स्पष्ट है । अतः इसका ‘शास्त्र’ नाम बाद में प्रचलित हुआ, जब इसको संकलन करके ग्रन्थरूप में निबद्ध कर दिया गया । और १।६३ श्लोक में मनुओं द्वारा चराचर जगत् की उत्पत्ति का कथन भी पूर्वापर से विरूद्ध है । जब पीछे अव्यक्त परमात्मा से जगदुत्पत्ति कही जा चुकी है, तो यह पुनरूक्ति क्यों ? और क्या कोई शरीरधारी जीव चराचर जगत् की रचना कर सकता है ? यह सब शास्त्रों से विरूद्ध मान्यता है । और मनु सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए, वे अपने से बाद में होने वाले स्वायम्भुवादि सात मनुओं का वर्णन कैसे कर सकते हैं ?
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना भृगुः ।
तानब्रवीदृषीन्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूयतां इति । ।1/60
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जब इस प्रकार मनुजी ने भृगु ऋषि से कहा, तब भृगु ऋषि ने प्रसन्न हो ¬ प्रीतिपूर्वक सब ऋषियों से कहा कि सुनिये -
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।५८-६३ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।५२-५७ तक श्लोकों में परमात्मा की जाग्रत - सुषुप्ति दशाओं का वर्णन है और १।६४-७३ तक श्लोकों में इन अवस्थाओं की अवधि (दिन - रात - सृष्टि - प्रलय के परिमाण वर्षों का) का वर्णन है । इस प्रकार पूर्वापर का प्रसंग है, उससे विरूद्ध इन बीच के श्लोकों का अप्रासंगिक वर्णन किया गया है । और मनुस्मृति के रचयिता मनु हैं, किन्तु इन श्लोकों में ‘इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ’ कहकर ब्रह्मा को मूल रचयिता बताया है । यह ब्रह्मा से सृष्टि रचना मानने वालों ने बाद में प्रसंग को जोड़ने का ही दुस्साहस किया है । जब ऋषियों ने ।१-४ श्लोकों में मनु से धर्म के लिये प्रार्थना की है, तो ब्रह्मा कहाँ से आ गये ? यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान मनु को प्राप्त होता तो मनु अवश्य ही इसकी चर्चा कहीं तो करते ? अतः इस शास्त्र के मूल - प्रवक्ता मनु ही हैं । और इन श्लोकों में मनुस्मृति को ‘शास्त्र’ नाम से लिखा है, यह व्यवहार भी यथार्थ में अर्वाचीन है । मनुस्मृति तो प्रवचन रूप ही थी, जैसे - वक्तुमर्हसि (१।२) श्रूयताम् (१।४२) तं निबोधत (६।१२०) विधानं श्रूयताम् (३।२८६) इत्यादि श्लोकों से स्पष्ट है । अतः इसका ‘शास्त्र’ नाम बाद में प्रचलित हुआ, जब इसको संकलन करके ग्रन्थरूप में निबद्ध कर दिया गया । और १।६३ श्लोक में मनुओं द्वारा चराचर जगत् की उत्पत्ति का कथन भी पूर्वापर से विरूद्ध है । जब पीछे अव्यक्त परमात्मा से जगदुत्पत्ति कही जा चुकी है, तो यह पुनरूक्ति क्यों ? और क्या कोई शरीरधारी जीव चराचर जगत् की रचना कर सकता है ? यह सब शास्त्रों से विरूद्ध मान्यता है । और मनु सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए, वे अपने से बाद में होने वाले स्वायम्भुवादि सात मनुओं का वर्णन कैसे कर सकते हैं ?
स्वायंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे ।
सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महौजसः । ।1/61
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
ब्रह्माजी से जो मुनि उत्पन्न हुए, उनके वंश में छह मुनि और भी हैं, इन महातेजस्वी महात्माओं ने अपने-अपने तपोबल से अपनी-अपनी सन्तानें उत्पन्न कीं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।५८-६३ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।५२-५७ तक श्लोकों में परमात्मा की जाग्रत - सुषुप्ति दशाओं का वर्णन है और १।६४-७३ तक श्लोकों में इन अवस्थाओं की अवधि (दिन - रात - सृष्टि - प्रलय के परिमाण वर्षों का) का वर्णन है । इस प्रकार पूर्वापर का प्रसंग है, उससे विरूद्ध इन बीच के श्लोकों का अप्रासंगिक वर्णन किया गया है । और मनुस्मृति के रचयिता मनु हैं, किन्तु इन श्लोकों में ‘इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ’ कहकर ब्रह्मा को मूल रचयिता बताया है । यह ब्रह्मा से सृष्टि रचना मानने वालों ने बाद में प्रसंग को जोड़ने का ही दुस्साहस किया है । जब ऋषियों ने ।१-४ श्लोकों में मनु से धर्म के लिये प्रार्थना की है, तो ब्रह्मा कहाँ से आ गये ? यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान मनु को प्राप्त होता तो मनु अवश्य ही इसकी चर्चा कहीं तो करते ? अतः इस शास्त्र के मूल - प्रवक्ता मनु ही हैं । और इन श्लोकों में मनुस्मृति को ‘शास्त्र’ नाम से लिखा है, यह व्यवहार भी यथार्थ में अर्वाचीन है । मनुस्मृति तो प्रवचन रूप ही थी, जैसे - वक्तुमर्हसि (१।२) श्रूयताम् (१।४२) तं निबोधत (६।१२०) विधानं श्रूयताम् (३।२८६) इत्यादि श्लोकों से स्पष्ट है । अतः इसका ‘शास्त्र’ नाम बाद में प्रचलित हुआ, जब इसको संकलन करके ग्रन्थरूप में निबद्ध कर दिया गया । और १।६३ श्लोक में मनुओं द्वारा चराचर जगत् की उत्पत्ति का कथन भी पूर्वापर से विरूद्ध है । जब पीछे अव्यक्त परमात्मा से जगदुत्पत्ति कही जा चुकी है, तो यह पुनरूक्ति क्यों ? और क्या कोई शरीरधारी जीव चराचर जगत् की रचना कर सकता है ? यह सब शास्त्रों से विरूद्ध मान्यता है । और मनु सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए, वे अपने से बाद में होने वाले स्वायम्भुवादि सात मनुओं का वर्णन कैसे कर सकते हैं ?
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा ।
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च । ।1/62
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
उन महातेजस्वियों के नाम यह हैं-1-स्वारोचिप, 2-उत्तम, 3-तामस, 4-रैवत, 5-चाक्षुप, 6-वैवरवत।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।५८-६३ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।५२-५७ तक श्लोकों में परमात्मा की जाग्रत - सुषुप्ति दशाओं का वर्णन है और १।६४-७३ तक श्लोकों में इन अवस्थाओं की अवधि (दिन - रात - सृष्टि - प्रलय के परिमाण वर्षों का) का वर्णन है । इस प्रकार पूर्वापर का प्रसंग है, उससे विरूद्ध इन बीच के श्लोकों का अप्रासंगिक वर्णन किया गया है । और मनुस्मृति के रचयिता मनु हैं, किन्तु इन श्लोकों में ‘इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ’ कहकर ब्रह्मा को मूल रचयिता बताया है । यह ब्रह्मा से सृष्टि रचना मानने वालों ने बाद में प्रसंग को जोड़ने का ही दुस्साहस किया है । जब ऋषियों ने ।१-४ श्लोकों में मनु से धर्म के लिये प्रार्थना की है, तो ब्रह्मा कहाँ से आ गये ? यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान मनु को प्राप्त होता तो मनु अवश्य ही इसकी चर्चा कहीं तो करते ? अतः इस शास्त्र के मूल - प्रवक्ता मनु ही हैं । और इन श्लोकों में मनुस्मृति को ‘शास्त्र’ नाम से लिखा है, यह व्यवहार भी यथार्थ में अर्वाचीन है । मनुस्मृति तो प्रवचन रूप ही थी, जैसे - वक्तुमर्हसि (१।२) श्रूयताम् (१।४२) तं निबोधत (६।१२०) विधानं श्रूयताम् (३।२८६) इत्यादि श्लोकों से स्पष्ट है । अतः इसका ‘शास्त्र’ नाम बाद में प्रचलित हुआ, जब इसको संकलन करके ग्रन्थरूप में निबद्ध कर दिया गया । और १।६३ श्लोक में मनुओं द्वारा चराचर जगत् की उत्पत्ति का कथन भी पूर्वापर से विरूद्ध है । जब पीछे अव्यक्त परमात्मा से जगदुत्पत्ति कही जा चुकी है, तो यह पुनरूक्ति क्यों ? और क्या कोई शरीरधारी जीव चराचर जगत् की रचना कर सकता है ? यह सब शास्त्रों से विरूद्ध मान्यता है । और मनु सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए, वे अपने से बाद में होने वाले स्वायम्भुवादि सात मनुओं का वर्णन कैसे कर सकते हैं ?
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
उन छह मन्वन्तरों के नाम क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और महातेजस्वी वैवस्वत हैं।
स्वायंभुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः ।
स्वे स्वेऽन्तरे सर्वं इदं उत्पाद्यापुश्चराचरम् । ।1/63
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
स्वायम्भू आदि सातों मुनि जो बड़े तेजवान् हैं, अपने तपोबल से सारे चर और अचर प्राणियों (जीवधारियों) को उत्पन्न करके पालने लगे।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।५८-६३ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।५२-५७ तक श्लोकों में परमात्मा की जाग्रत - सुषुप्ति दशाओं का वर्णन है और १।६४-७३ तक श्लोकों में इन अवस्थाओं की अवधि (दिन - रात - सृष्टि - प्रलय के परिमाण वर्षों का) का वर्णन है । इस प्रकार पूर्वापर का प्रसंग है, उससे विरूद्ध इन बीच के श्लोकों का अप्रासंगिक वर्णन किया गया है । और मनुस्मृति के रचयिता मनु हैं, किन्तु इन श्लोकों में ‘इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ’ कहकर ब्रह्मा को मूल रचयिता बताया है । यह ब्रह्मा से सृष्टि रचना मानने वालों ने बाद में प्रसंग को जोड़ने का ही दुस्साहस किया है । जब ऋषियों ने ।१-४ श्लोकों में मनु से धर्म के लिये प्रार्थना की है, तो ब्रह्मा कहाँ से आ गये ? यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान मनु को प्राप्त होता तो मनु अवश्य ही इसकी चर्चा कहीं तो करते ? अतः इस शास्त्र के मूल - प्रवक्ता मनु ही हैं । और इन श्लोकों में मनुस्मृति को ‘शास्त्र’ नाम से लिखा है, यह व्यवहार भी यथार्थ में अर्वाचीन है । मनुस्मृति तो प्रवचन रूप ही थी, जैसे - वक्तुमर्हसि (१।२) श्रूयताम् (१।४२) तं निबोधत (६।१२०) विधानं श्रूयताम् (३।२८६) इत्यादि श्लोकों से स्पष्ट है । अतः इसका ‘शास्त्र’ नाम बाद में प्रचलित हुआ, जब इसको संकलन करके ग्रन्थरूप में निबद्ध कर दिया गया । और १।६३ श्लोक में मनुओं द्वारा चराचर जगत् की उत्पत्ति का कथन भी पूर्वापर से विरूद्ध है । जब पीछे अव्यक्त परमात्मा से जगदुत्पत्ति कही जा चुकी है, तो यह पुनरूक्ति क्यों ? और क्या कोई शरीरधारी जीव चराचर जगत् की रचना कर सकता है ? यह सब शास्त्रों से विरूद्ध मान्यता है । और मनु सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए, वे अपने से बाद में होने वाले स्वायम्भुवादि सात मनुओं का वर्णन कैसे कर सकते हैं ?
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
स्वयम्भू परमेश्वर द्वारा निर्मित इस पूर्ववर्ती स्वायम्भुव मन्वन्तर के पश्चात् छह अन्य उसी श्रेणी के मन्वन्तर हुए। उन दीर्घकाल-शरीर धारी तथा महाशक्तिशाली मन्वन्तरों ने अपनी-अपनी सृष्टि सिरजन की। १. महात्मानः=महाशरीराः, यहां आत्मा शब्द शरीरवाची है। मन्वन्तर के बदलने पर सृष्टि के नैमित्तिक गुणों में भी कुछ-कुछ बदली हो जाती है इसलिए मन्वन्तर संज्ञा बांधी गयी है। (ऋ० भू० वेदोत्पत्ति)
निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कला ।
त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः । ।1/64
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
अठारह पल का एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन-रात होता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(दश च अष्टौ च) दश और आठ मिलाकर अर्थात् अठारह (निमेषाः) निमेषों (पलक झपकने का समय) की (काष्ठा) १ काष्ठा होती है (ताः त्रिंशत्तु) उन तीन काष्ठाओं की (कला) १ कला होती है (त्रिंशत्कलाः) तीस कलाओं का (मुहूत्र्त स्यात्) एक मुहूत्र्त (४८ मिनट का) होता है , और (तावतः तु) उतने ही अर्थात् ३० मुहूत्र्तों के (अहोरात्रम्) एक दिन - रात होते हैं ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
१०+८=१८ निमेषों (आंख का मीचना) की १ काष्ठा, ३० काष्ठाओं की १ कला, ३० कलाओं का १ मुहूर्त, और ३० मुहूर्तों का एक अहरोत्र (दिनरात) होता है।१ १. इसके अनुसार आजकल के काल विभाग की तुलना इस प्रकार बैठती है- सैकण्ड का १ निमेष, सैकण्ड की १ काष्ठा, १ मि० ३६ सै० की १ कला, ४८ मिनिट का मुहूर्त, और २४ घण्टे का १ अहरोत्र।
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके ।
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणां अहः । ।1/65
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
मनुष्य और देवताओं के रात्रि दिवस की पहिचान सूय्र्य के कारण से होती है। सब जीवधारियों के विश्राम के हेतु रात्रि और काय्र्य के हेतु दिवस नियत हुआ।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(सूय्र्यः) सूर्य (मानुष - दैविके) मानुष - मनुष्यों के और दैवी - देवताओं के (अहोरात्रे) दिन - रातों का (विभजते) विभाग करता है, उनमें (भूतानां स्वप्नाय रात्रिः) प्राणियों के सोने के लिए ‘रात’ है और (कर्मणां चेष्टायें अहः) कामों के करने के लिए ‘दिन’ होता है ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
सूर्य मानुष और दैविक दिनरात का विभाग करता है। जिसमें प्राणियों के सोने के लिये रात और कामों के करने के लिए दिन है।
पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः ।
कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी । ।1/66
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
मनुष्यों के एक मास के तुल्य पितरों का एक-रात्रि दिवस होता है। इसमें कृष्णपक्ष काय्र्य करने के हेतु दिन है और शुक्लपक्ष सोने के हेतु रात्रि है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।६६ वाँ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त है - यह श्लोक पूर्वापर - प्रसंग से विरूद्ध है । दिन - रात - सृष्टि - प्रलय के परिमाण के वर्णन में पितरों के मास, रात - दिनादि की कोई संगति नहीं है । ज्योतिषादि शास्त्रों में भी दो प्रकार से काल - गणना की गई है - देववर्ष तथा मानव वर्ष । मनु को भी वे ही अभिप्रेत हैं । पितरों की काल - गणना के वर्ष मनु ने दिखाये भी नहीं हैं । अन्यथा दिन - रात - मास दिखाकर पितरों के वर्षों की गणना भी वैसे ही करते, जैसे देव - मानववर्ष गिनाये हैं । और १।६५ श्लोक की १।६७ से पूर्णत् संगति है, बीच में इस विषय का केवल एक ही श्लोक है, जिससे किसी भी प्रकार की संगति नहीं है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है । और यह पितरों की एक योनि - विशेष मानने वालों की भावना से अनुप्राणित है । और यह व्यवहारिक भी नहीं है । पितरों के रात - दिन १५-१५ मानव दिन के होते हैं , और इस श्लोक में कहा है कि कृष्ण दिन काम करने के लिये, और शुक्ल दिन सोने के लिये हैं । इसका आशय लोकव्यवहार से विपरीत है । रात सोने तथा दिन काम करने के लिये प्रसिद्ध है, पितरों के रात - दिन विपरीत ही हैं । और इन पितरों के रात - दिन को दिखाने की कोई संगति भी नहीं है ।
दैवे रात्र्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः ।
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद्दक्षिणायनम् ॥1/67
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
मनुष्यों के एक वर्ष के तुल्य देवताओं का एक रात्रि-दिन होता है। जब तक *सूर्य उत्तरायण रहते हैं तब तक दिन रहता है और जब तब सूर्य **दक्षिणायन रहते हैं तब रात्रि होती है।
टिप्पणी :
*माघ की संक्रांति से सावन की संक्रांति तक उत्तरायण होता है।** सावन की संक्रांति से माघ की संक्रांति तक दक्षिणायन होता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(वर्षम्) मनुष्यों का एक वर्ष (दैवे रात्र्यहनी) देवताओं के एक दिन - रात होते हैं (तयोः पुनः प्रविभागः) उनका भी फिर विभाग है (तत्र उदगयनम् अहः) उनमें ‘उत्तरायण’ देवों का दिन है, और (दक्षिणायनम् रात्रिः स्यात्) ‘दक्षिणा-यन’ देवों की रात है ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
मानुष वर्ष दैविक रातदिन है। पुनः उन दैविक दिनरातों का विभाग इस प्रकार है कि मानुष वर्ष में उत्तरायण काल दैविक दिन है और दक्षिणयान काल दैविक रात है।
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः ।
एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत । ।1/68
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
ब्रह्मा के रात्रि-दिन की संख्या और प्रत्येक युग की संख्या क्रम से स्पष्ट सुनिये-
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(मनु महर्षियों से कहते हैं कि) (ब्राह्मस्य तु क्षपा - अहस्य) परमात्मा के दिन - रात का तु तथा एकैकशः युगानाम् एक - एक युगों का यत् प्रमाणम् जो कालपरिमाण है तत् उसे क्रमशः क्रमानुसार और समासतः संक्षेप से निबोधत सुनो ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
मानुष और दैविक काल-ज्ञान के पश्चात् अब ब्राह्म (ईश्वरीय) रात दिन का तथा एक एक (प्रत्येक) युग का जो प्रमाण है, संक्षेपतः क्रमशः उसे सुनिए-
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्साणां तत्कृतं युगम् ।
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः । ।1/69
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
देवताओं के चार सहस्र (हजार) वर्ष का सतयुग होता है। युग के प्रथम चार सौ वर्ष की देवताओं की सन्ध्या कहलाती है, और युग के अन्त पर उतना ही सन्ध्यांश कहलाता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
तत् चत्वारि सहस्त्राणि वर्षाणां कृतं युगम् आहुः उन देवताओं ६७ वें में जिनके दिन - रातों का वर्णन है के चार हजार दिव्य वर्षों का एक ‘सतयुग’ कहा है (तस्य) इस सतयुग की यावत् शती सन्ध्या उतने ही सौ वर्ष की अर्थात् ४०० वर्ष की संध्या होती है और तथाविधः उतने ही वर्षों का अर्थात् संध्यांशः संध्याशं का समय होता है ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
४००० दैविक वर्षों का कृतयुग (सत् युग) कहलाता है। और उसके उतने ही सैंकड़े अर्थात् ४०० वर्षों की सन्ध्या तथा उसी तरह ४०० वर्षों का सन्ध्यांश होता है।
इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु ।
एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च । ।1/70
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
तीनों युगों अर्थात् त्रेता, द्वापर, कलियुग की संध्या और सन्ध्यांश की संख्या एक सहस्र (हजार) और एक सौ वर्ष* के घटाने से होती है।
टिप्पणी :
3000 वर्ष का त्रेता युग और 300 वर्ष की सन्ध्या और 300 वर्ष का सन्ध्यांश, 2000 वर्ष का द्वापर 200 वर्ष की सन्ध्या और 200 वर्ष का सन्ध्यांश, 1000 वर्ष का कलियुग, 100 वर्ष की सन्ध्या और 100 वर्ष का सन्ध्यांश।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
च और इतरेषु त्रिषु शेष अन्य तीन - त्रेता, द्वापर, कलियुगों में ससंध्येषु संसध्यांशेषु ‘संध्या’ नामक कालों में तथा ‘संध्यांश’ नामक कालों में सहस्त्राणि च शतानि एक - अपायेन क्रमशः एक हजार और एक - एक सौ घटा देने से वर्तन्ते उनका अपना - अपना कालपरिमाण निकल आता है अर्थात् ४८०० दिव्यवर्षों का सतयुग होता है, उसकी संख्याओं मं एक सहस्त्र और संध्या व संध्यांश में एक - एक सौ घटाने से ३००० दिव्यवर्ष + ३०० संध्यावर्ष + ३०० संध्यांशवर्ष - ३६०० दिव्यवर्षों का त्रेतायुग होता है । इसी प्रकार - २०००+२००+२००- २४०० दिव्यवर्षों का द्वापर और १०००+१००+१०० - १२०० दिव्यवर्षों का कलियुग होता है ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
सन्ध्या और सन्ध्यांश सहित अन्य तीनों युगों में हजार और सैंकड़े क्रमशः एक एक कम होते हैं।१ १. एवं, युग-गणना इस प्रकार होगी- कृत ४०००+४००+४०० ४८०० दैविक वर्ष त्रेता ३०००+३००+३०० ३६०० दैविक वर्ष द्वापर २०००+२००+२०० २४०० दैविक वर्ष कलि १०००+१००+१०० १२०० दैविक वर्ष इस का मानुष वर्ष में परिवर्तन ३६० से गुणा करने पर इस प्रकार होगा- कृत १७२८००० मानुष वर्ष त्रेता १२९६००० मानुष वर्ष द्वापर ८६४००० मानुष वर्ष कलि ४३२००० मानुष वर्ष ४३,२०,०००
यदेतत्परिसंख्यातं आदावेव चतुर्युगम् ।
एतद्द्वादशसाहस्रं देवानां युगं उच्यते । ।1/71
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
यह जो चार युगों की संख्या कही है, इसका बारह सहस्र गुण अधिक देवताओं का युग होता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
यद् एतत् जो यह आदौ पहले (६९-७० में) चतुर्युगम् चारों युगों को परिसंख्यातम् कालपरिमाण के रूप में गिनाया है एतद् यह द्वादश- साहस्त्रम् बारह हजार दिव्य वर्षों का काल मनुष्यों का एक चतुर्युगी का काल देवानाम् देवताओं का युगम् एक युग उच्यते कहा जाता है ।
टिप्पणी :
स्पष्टीकरण - १२००० दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है । उसे मानुष वर्षों में बदलने के लिए ३६० से गुणा करने पर १२००० × ३६० त्र ४३,२०,००० मानुष वर्षों की एक चतुर्युगी होती है । दोनों श्लोकों के कालपरिमाण को तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है - दिव्यवर्ष संध्यावर्ष संध्यांशवर्ष कुल दिव्यवर्षों का गुणा करने से मानुष वर्षो का युगनाम ४०००+ ४००+ ४००= ४८००× ३६०= १७,२८,००० सतयुग ३०००+ ३००+ ३००= ३६००× ३६०= १२,९६,००० त्रेतायुग २०००+ २००+ २००= २४००× ३६०= ८,६४,००० द्वापरयुग १०००+ १००+ १००= १२००× ३६०= ४,३२,००० कलियुग १००००+ १०००+ १०००= १२०००× ३६०= ४३,२०,००० एकचतुर्युगी
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
अभी पहले जो यह चारों युगों की गणना की गयी है, वह १२००० वर्षों का एक देवों का युग कहलाता है।
दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया ।
ब्राह्मं एकं अहर्ज्ञेयं तावतीं रात्रिं एव च । ।1/72
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
देवताओं के सहस्र (हजार) युग के तुल्य ब्रह्माजी का एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि होती है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
.( दैविकानां युगानाम् तु) देवयुगों को (सहस्त्रं परिसंख्यया) हजार से गुणा करने पर जो कालपरिमाण निकलता है , जैसे - चार मानुषयुगों के दिव्यवर्ष १२००० होते हैं उनको हजार से गुणा करने पर १,२०,००,००० दिव्यवर्षों का (ब्राह्मम्) परमात्मा का (एकं अहः) एक दिन (च) और (तावतीं रात्रिम्) उतने ही दिव्यवर्षों की उसकी एक रात (ज्ञेयम्) समझनी चाहिए ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
१००० दैविक युगों का एक ब्राह्मदिन और उतनी ही ब्राह्म रात्रि जाननी चाहिए।
तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यं अहर्विदुः ।
रात्रिं च तावतीं एव तेऽहोरात्रविदो जनाः । ।1/73
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
ब्रह्मा के सहस्र युग के तुल्य परब्रह्म का एक दिन होता है। सो वह दिन बड़ा पवित्र है और उतनी ही रात्रि भी होती है इसे रात्रि दिन के ज्ञाताओं ने कहा।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
जो लोग तत् युगसहस्त्रान्तं ब्राह्म पुण्यम् अहः उस एक हजार दिव्य युगों के परमात्मा के पवित्र दिन को च और तावतीं एव रात्रिम् उतने ही युगों की परमात्मा की रात्रि को विदुः समझते हैं ते वे ही वै अहोरात्रविदः जनाः वास्तव में दिन - रात - सृष्टि - प्रलय के काल के वेत्ता लोग हैं ।
टिप्पणी :
महर्षिदयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में १।६८ से ७३ श्लोकों को उद्धृत करके उनका भाव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है - प्रश्न - वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं ? उत्तर - एक वृन्द्र, छानवे करोड़ , आठ लाख, बावन हजार, नव सौ, छहत्तर अर्थात् १,९६,०८,५२,९७६ वर्ष वेदों की और जगत् की उत्पत्ति में हो गये हैं और यह संवत् ७७ सतहत्तरवां वत्र्त रहा है । प्रश्न - यह कैसे निश्चय होय कि इतने ही वर्ष वेद और जगत् की उत्पत्ति में बीत गये हैं ? उत्तर - यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें सातवें (७) वैवस्वत मनु का वत्र्तमान है । इससे पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके हैं - स्वायंभुव १, स्वारोचिष २, औत्तमि ३, तामस ४, चाक्षुष ६, ये छः तो बीत गये हैं और ७ (सातवां) वैवस्वत वत्र्त रहा है और सावर्णि आदि ७ (सात) मन्वतर आगे भोगेगें । ये सब मिलके १४ (चैदह) मन्वन्तर होते हैं और एकहत्तर चतुर्युगियों का नाम मन्वन्तर धरा गया है, सो उस की गणना इस प्रकार से है कि (१७२८०००) सत्रह लाख अठाईस हजार वर्षों का सतयुग रक्खा है; (१२९६०००) बारह लाख, छानवे हजार वर्षों का नाम त्रेता;(८६४०००) आठ लाख चैंसठ हजार वर्षों का नाम द्वापर और (४३२०००) चार लाख, बत्तीस हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्खा है तथा आर्यों ने एक क्षण और निमेष से लेके एक वर्ष पर्यन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है और इन चारों युगों के (४३२००००) तितालीसलाख, बीस हजार वर्ष होते हैं , जिनका चतुर्युगी नाम है । एकहत्तर (७१) चतुर्युगियों के अर्थात् (३०६७२००००) तीस करोड़, सरसठ लाख, बीस हजार वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है और ऐसे - ऐसे छः मन्वन्तर मिलकर अर्थात् (१८४०३२००००) एक अर्ब, चैरासी करोड़, तीन लाख, बीस हजार वर्ष हुए और सातवें मन्वन्तर के भोग में यह (२८) अठाईसवीं चतुर्युगी है । इस चतुर्युगी में कलियुग के (४९७६) चार हजार, नौ सौ छहत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका है और बाकी (४२७०२४) चार लाख, सत्ताईस हजार चौबीस वर्षों का भोग होने वाला है । जानना चाहिए कि (१२०५३२९७६) बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नव सौ छहत्तर वर्ष तो वैवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं और (१८६१८७०२४) अठारह करोड़, एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं । इनमें से यह वर्तमान वर्ष (७७) सतहत्तरवाँ है जिसको आर्यलोग विक्रम का (१९३३) उन्नीस सौ तेतीसवां संवत् कहते हैं । जो पूर्व चतुर्युगी लिख आये हैं उन एक हजार चतुर्युगियों की ब्राह्मदिन संज्ञा रखी है और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए । सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार चतुर्युगी पर्यन्त ईश्वर इस को बना रखता है, इसी का नाम ब्राह्मदिन रक्खा है, और हजार चतुर्युगी पर्यन्त सृष्टि को मिटाके प्रलय अर्थात् कारण में लीन रखता है , उस का नाम ब्राह्मरात्रि रक्खा है अर्थात् सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है । यह जो वर्तमान ब्राह्मदिन है, इसके (१,९६,०८,५२,९७६) एक अर्ब, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नव सौ छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं और (२३३३२२७०२४) दो अर्ब, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख , सत्ताईस हजार चौबीस वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं । इनमें से अन्त का यह चौबीसवां वर्ष भोग रहा है । आगे आने वाले भोग के वर्षों में से एक - एक घटाते जाना और गत वर्षों में क्रम से एक - एक वर्ष मिलाते जाना चाहिये । जैसे आज पर्यन्त घटाते बढ़ाते आये हैं । (ऋ० भू० वेदात्पत्ति विषय)
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
एवं, उस १००० युग के ब्राह्म पुण्यदिन को और उतनी ही ब्राह्मरात्रि को जो उन जानते हैं वे अहोरात्र के (सृष्टिकाल और प्रलयकाल के) वेत्ता हैं।१
टिप्पणी :
१. मानुष वर्ष में उपर्युक्त सृष्टि व प्रलय के काल का परिवर्तन इस प्रकार होगाः-४३२००००×१०००=४३२००००००० अर्थात् ४ अरब ३२ करोड़ वर्ष की सृष्टि की आयु है; और उतनी ही आयु प्रलय की है। क्योंकि ‘सर्वेषाँ तु स नामानि’ आदि चौथे श्लोक में वेदोत्पत्ति सृष्टि की आदि में वर्णित की गयी है, अतः वेदोत्पत्ति का काल भी सृष्टिकाल जितना ही समझना चाहिए। अथर्ववेद ८ म काण्ड, २ य सूक्त के २१ वें मन्त्र में सृष्टि व प्रलय के काल का प्रतिपादन इस प्रकार किया है- शंत तेऽयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः। इन्द्राग्नी विश्वेदेवास्ते न मन्यन्तामहृणीयमानाः॥ (ते) उन अहोरात्रों अर्थात् सृष्टि और प्रलय को (शतं अयुतं हायनान्) १० हजार वर्ष गुणा १०० अर्थात् १० लाख तक शून्यों से पहले (द्वे त्रीणि चत्वारि युगे) क्रमशः २, ३, ४ मिलाने पर ४,३२,००००००० वर्ष की आयु वाले (कृण्मः) करता हूं। (इन्द्राग्नी) ब्राह्मण और क्षत्रिय (विश्वेदेवाः) तथा वैश्य (अहृणीयमानाः) ये द्विज शान्तचित्त होकर (ते) उन सृष्टिप्रलय रूपी अहोरात्रों का (मन्यन्तां) मनन करें। इसी प्रकार यजुर्वेद अ० १५ मन्त्र ६५ में कहा है-‘सहस्रस्य प्रमा असि’। हे परमेश्वर! तू सहस्र महायुग (१००० चतुर्युगी) परिमित सर्ग और प्रलय का प्रमाता या निर्माता है।
तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते ।
प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम् । ।1/74
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
यह ब्रह्मा अपने दिन में काय्र्य करते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं। जब जाग्रत होते हैं तो संकल्प-विकल्प रूप मन को सृष्टि रचने की आज्ञा देते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(प्रसुप्तः सः) वह प्रलय - अवस्था में सोया हुआ - (सा (१।५२-५७) परमात्मा (तस्य अहर्निशस्य अन्ते) उस (१।६८-७२) दिन - रात के बाद (प्रति बुध्यते) जागता है - सृष्टयु त्पत्ति में प्रवृत्त होता है (च) और प्रतिबुद्धः जागकर (सद् - असद् - आत्मकम्) जो कारणरूप में विद्यमान रहे और जो विकारी अंश से कार्यरूप में अविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले (मनः) ‘महत्’ नामक प्रकृति के आद्यकार्यतत्त्व की सृजति सृष्टि करता है ।
मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया ।
आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः । ।1/75
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
मन ने ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर आप से आप आकाश को बनाया, इसका गुण शब्द है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(सिसृक्षया) सृष्टि को रचने की इच्छा से फिर वह परमात्मा (मनः सृष्टिं विकुरूते) महत्तत्त्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है - अहंकार के रूप में विकृत करता है (तस्मात्) उस विकारी अंश से (चोद्यमानं आकाशं जायते) प्रेरित हुआ - हुआ ‘आकाश’ उत्पन्न होता है (तस्य) उस आकाश का (गुणं शब्दं विदुः) गुण ‘शब्द’ को मानते हैं ।
टिप्पणी :
आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षिदयानन्द लिखते हैं - ‘‘उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पनन सा होता है । वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती । क्यों कि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सकें ?’’ (स० प्र० अष्टमसमु०)
आकाशात्तु विकुर्वाणात्सर्वगन्धवहः शुचिः ।
बलवाञ् जायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः । ।1/76
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
आकाश के पश्चात् सब गन्धों की ज्ञाता (पहिचानने वाली), पवित्र और बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। इस का गुण स्पर्श है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(आकाशात् तु विकुर्वाणात्) उस आकाश के विकारोत्पादक अंश से (सर्वगन्धवहः) सब गन्धों को वहन करने वाला शुचिः शुद्ध और बलवान् शक्तिशाली (वायुः) ‘वायु’ (जायते) उत्पन्न होता है (सः वै) वह वायु निश्चय से (स्पर्शगुणः) स्पर्श गुण वाला (मतः) माना गया है
वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम् ।
ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणं उच्यते । ।1/77
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
वायु के पश्चात् तम का नाश करने वाली और प्रकाश फैलाने वाली ज्योति उत्पन्न की। इसका गुण रूप है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(वायोः अपि) उस वायु के भी (विकुर्वाणात् )विकारोत्पादक अंश से (विरोचिष्णुः उज्जवल तमोनुदम्) अन्धकार को नष्ट करने वाली (भास्वत् )प्रकाशक (ज्योतिः उत्पद्यते ‘अग्नि’) उत्पन्न होती है (तत् रूप गुणम् उच्यते )उसका गुण ‘रूप’ कहा है ।
ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्मृताः ।
अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः । ।1/78
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
अग्नि के पश्चात् जल बनाया, जिसका गुण रस है। और जल से पृथ्वी को रचा, जिसका गुण गन्ध है। संसार के प्रारम्भ से यही स्वभाव रहता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(च )और (ज्योतिषः विकुर्वाणात्) अग्नि के विकारोत्पादक अंश से (रसगुणाः आपः स्मृताः) ‘रस’ गुण वाला जल उत्पन्न होता है, और अद्भ्यः जल से गन्धगुणा भूमिः ‘गन्ध’ गुण वाली भूमि उत्पन्न होती है (इति एषा सृष्टि आदितः) यह इस प्रकार प्रारम्भ से लेकर (१।१४ से) यहां तक वर्णित सृष्टि उत्पन्न होने की प्रक्रिया है ।
यद्प्राग्द्वादशसाहस्रं उदितं दैविकं युगम् ।
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरं इहोच्यते । ।1/79
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
बारह सहस्र वर्ष का देवताओं का एक युग होता है। और उसका एकहत्तर गुणा एक मन्वन्तर होता है। यह बारह सहस्र देवताओं के वर्ष हैं, न कि मनुष्यों के।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
. (प्राक्) पहले श्लोकों में (१।७१) (यत्) जो (द्वादशसाहस्त्रम्) बारह हजार दिव्य वर्षों का (दैविकं युगम् उदितम्) एक ‘देवयुग’ कहा है( तत् एक - सप्ततिगुणम्) उससे इकहत्तर गुना समय अर्थात् १२००० × ७१ - ८, ५२, ००० दिव्यवर्षों का अथवा ८,५२,००० दिव्यवर्ष × ३६० = ३०,६७,२०,००० मानुषवर्षों का (इह मन्वन्तरं उच्यते) यहां एक ‘मन्वन्तर’ का कालपरिमाण माना गया है ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
जो पहले १२००० वर्ष का दैविक युग बतलाया गया है, उसका ७१ गुणा इस मन्वन्तर-काल-गणना में एक मन्वन्तर कहलाता है।१
टिप्पणी :
. पहले चतुर्येगी-प्रमाण के समय दर्शाया जा चुका है कि सत्युग की गणना में ८५०० दैववर्षों का सन्ध्याकाल होता है। उसी तरह इस मन्वन्तर-गणना में भी प्रत्येक मन्वन्तर के पीछे ८५०० दैववर्षों का सन्ध्याकाल होता है तथा आदिम मन्वन्तर स्वायम्भुव के प्रारम्भ में ८५०० दैववर्षों का प्रारम्भिक सन्ध्या काल और अधिक होता है। सब मन्वन्तर १४ हैं। अतः स्वायम्भुव का आदिम सन्ध्याकाल मिला कर कुल १५ सन्ध्याकाल ८५०० वर्षों के प्रत्येक हुए। अब पाठक निम्न रीति से स्पष्टतया युग व मन्वन्तर, इन दोनों प्रकार की गणनायों से दैववर्षों में सृष्टिकाल समझ सकेगे- १२०००×१०००=१२०००००० युग-गणना से १२०००×७१×१४+(८५००×१५)=१२०००००० मन्वन्तर गणना से। सृष्टि, प्रलय और वेदोत्पत्ति के काल को मनुष्य सुगमतया गिन सकें, इसलिए ब्रह्मादिन और ब्राह्मरात्रि की संज्ञायें बांधी गयी हैं। (ऋ० भू० वेदोत्पत्ति)
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च ।
क्रीडन्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः । ।1/80
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति, नाश और मन्वन्तर आदि असंख्य बार अपनी स्वाभाविक शक्ति से रचते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(परमेष्ठी) वह सबसे महान! परमात्मा (असंख्यानि मन्वन्तराणि) असंख्य ‘मन्वन्तरों’ को (सर्गः) सृष्टि - उत्पत्ति (च और संहारः) एव प्रलय को (क्रीडन् इव) खेलता हुआ - सा (पुनः पुनः) बार - बार (कुरूते) करता रहता है ।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
मन्वन्तर असंख्य हैं और सृष्टि व प्रलय भी अनन्त हैं। सर्वाधिष्ठाता परमात्मा इस सृष्टि-प्रलय-कार्य को खेल की तरह सहजतया बारबार करता रहता है।
चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे ।
नाधर्मेणागमः कश्चिन्मनुष्यान्प्रति वर्तते । ।1/81
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
सतयुग में धर्म चारों चरण से स्थित था। इस युग के मनुष्य सत्य बोला करते थे और कोई अधर्म का काय्र्य नहीं करते थे।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।८१-८६ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - १।८० श्लोक की १।८७वें श्लोक से सृष्टि -रचना तथा उसकी रक्षा से सम्बन्ध होने से पूर्णतः संगति है । इनके मध्य में युगानुरूप धर्मादि का हृास और युगानुरूप फल - कथन की संगति प्रकरणविरूद्ध तथा मनु की मान्यता से विरूद्ध है । १।८१-८६ तक श्लोकों में जगत् का वर्णन न होने से १।८७ में ‘सर्वस्यास्य गुप्त्यर्थम्’ शब्दों की क्या संगति हो सती है ? क्यों कि इन पदों से समस्त - जगत् का ग्रहण किया है । अतः जगदुत्पत्ति के श्लोकों से ही संगति हो सकती है, युगानुरूप धर्मादि के हृास से नहीं । और इस अध्याय का विषय वर्णन करते हुए (१।१४४) श्लोक में सर्ग - रचना तथा धर्म बताया है, पुनः युगानुरूप फलकथन की इस विषय से क्या संगति ? और यह युगानुसार फलकथन मनु की मौलिक - मान्यता से भी विरूद्ध है । मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, अतः मनु का समस्त आधार धर्म - अधर्मानुसार (शुभ - अशुभकर्मानुसार) ही है । इस धर्मानुसार फलकथन की संगति युगानुरूप फलकथन से कदापि नहीं हो सकती । यदि युगानुरूप ही फल प्राप्त होवे तो मनुस्मृति का समस्त प्रयोजन ही धराशायी हो जाता है । और यह शास्त्र सब युगों के लिये निरर्थक हो जाता है और इन श्लोकों में चारों युगों में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को धर्म माना है । परन्तु मनु ने इन्हें सार्वभौम सार्वकालिक मानव - मात्र का धर्म माना है । और ‘‘राजा हि युगमुच्यते’’ (९।३०१) में राजा को ही युगा का कारण मनु ने क्यों कहा ? इससे स्पष्ट है कि ये सब श्लोक पौराणिक - युग की देन होने से प्रक्षिप्त हैं ।
इतरेष्वागमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोपितः ।
चौरिकानृतमायाभिर्धर्मश्चापैति पादशः । ।1/82
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
त्रेता आदि तीनों युगों में लोग अधर्म अर्थात् चोरी, झूठ और छल से कार्य करने लगे अतएव धर्म का एक-एक चरण घटता गया अर्थात् त्रेता में एक चौथाई, द्वापर में दो चौथाई (आधा) कलियुग में तीन चौथाई (पौन) धर्म न्यून हो गया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।८१-८६ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - १।८० श्लोक की १।८७वें श्लोक से सृष्टि -रचना तथा उसकी रक्षा से सम्बन्ध होने से पूर्णतः संगति है । इनके मध्य में युगानुरूप धर्मादि का हृास और युगानुरूप फल - कथन की संगति प्रकरणविरूद्ध तथा मनु की मान्यता से विरूद्ध है । १।८१-८६ तक श्लोकों में जगत् का वर्णन न होने से १।८७ में ‘सर्वस्यास्य गुप्त्यर्थम्’ शब्दों की क्या संगति हो सती है ? क्यों कि इन पदों से समस्त - जगत् का ग्रहण किया है । अतः जगदुत्पत्ति के श्लोकों से ही संगति हो सकती है, युगानुरूप धर्मादि के हृास से नहीं । और इस अध्याय का विषय वर्णन करते हुए (१।१४४) श्लोक में सर्ग - रचना तथा धर्म बताया है, पुनः युगानुरूप फलकथन की इस विषय से क्या संगति ? और यह युगानुसार फलकथन मनु की मौलिक - मान्यता से भी विरूद्ध है । मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, अतः मनु का समस्त आधार धर्म - अधर्मानुसार (शुभ - अशुभकर्मानुसार) ही है । इस धर्मानुसार फलकथन की संगति युगानुरूप फलकथन से कदापि नहीं हो सकती । यदि युगानुरूप ही फल प्राप्त होवे तो मनुस्मृति का समस्त प्रयोजन ही धराशायी हो जाता है । और यह शास्त्र सब युगों के लिये निरर्थक हो जाता है और इन श्लोकों में चारों युगों में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को धर्म माना है । परन्तु मनु ने इन्हें सार्वभौम सार्वकालिक मानव - मात्र का धर्म माना है । और ‘‘राजा हि युगमुच्यते’’ (९।३०१) में राजा को ही युगा का कारण मनु ने क्यों कहा ? इससे स्पष्ट है कि ये सब श्लोक पौराणिक - युग की देन होने से प्रक्षिप्त हैं ।
अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः ।
कृते त्रेतादिषु ह्येषां आयुर्ह्रसति पादशः । ।1/83
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
सतयुग में कोई बीमार न होता था और जो इच्छा करते थे, वही पूर्ण हो जाती थी। चार सौ वर्ष की आयु होती थी। त्रेता आदि तीनों युगों में मनुष्य की आयु एक एक चरण घट गई अर्थात् त्रेता में 300 वर्ष द्वापर में 200 वर्ष, कलियुग में 100 वर्ष।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।८१-८६ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - १।८० श्लोक की १।८७वें श्लोक से सृष्टि -रचना तथा उसकी रक्षा से सम्बन्ध होने से पूर्णतः संगति है । इनके मध्य में युगानुरूप धर्मादि का हृास और युगानुरूप फल - कथन की संगति प्रकरणविरूद्ध तथा मनु की मान्यता से विरूद्ध है । १।८१-८६ तक श्लोकों में जगत् का वर्णन न होने से १।८७ में ‘सर्वस्यास्य गुप्त्यर्थम्’ शब्दों की क्या संगति हो सती है ? क्यों कि इन पदों से समस्त - जगत् का ग्रहण किया है । अतः जगदुत्पत्ति के श्लोकों से ही संगति हो सकती है, युगानुरूप धर्मादि के हृास से नहीं । और इस अध्याय का विषय वर्णन करते हुए (१।१४४) श्लोक में सर्ग - रचना तथा धर्म बताया है, पुनः युगानुरूप फलकथन की इस विषय से क्या संगति ? और यह युगानुसार फलकथन मनु की मौलिक - मान्यता से भी विरूद्ध है । मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, अतः मनु का समस्त आधार धर्म - अधर्मानुसार (शुभ - अशुभकर्मानुसार) ही है । इस धर्मानुसार फलकथन की संगति युगानुरूप फलकथन से कदापि नहीं हो सकती । यदि युगानुरूप ही फल प्राप्त होवे तो मनुस्मृति का समस्त प्रयोजन ही धराशायी हो जाता है । और यह शास्त्र सब युगों के लिये निरर्थक हो जाता है और इन श्लोकों में चारों युगों में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को धर्म माना है । परन्तु मनु ने इन्हें सार्वभौम सार्वकालिक मानव - मात्र का धर्म माना है । और ‘‘राजा हि युगमुच्यते’’ (९।३०१) में राजा को ही युगा का कारण मनु ने क्यों कहा ? इससे स्पष्ट है कि ये सब श्लोक पौराणिक - युग की देन होने से प्रक्षिप्त हैं ।
वेदोक्तं आयुर्मर्त्यानां आशिषश्चैव कर्मणाम् ।
फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम् । ।1/84
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
वेद में मनुष्य की जो आयु निर्धारित की है, और इच्छापूत्र्ति के लिए जो आशिप और शाप है, और मनुष्यों की प्रकृति (स्वभाव)-यह सब बातें युगानुसार फल देती हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।८१-८६ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - १।८० श्लोक की १।८७वें श्लोक से सृष्टि -रचना तथा उसकी रक्षा से सम्बन्ध होने से पूर्णतः संगति है । इनके मध्य में युगानुरूप धर्मादि का हृास और युगानुरूप फल - कथन की संगति प्रकरणविरूद्ध तथा मनु की मान्यता से विरूद्ध है । १।८१-८६ तक श्लोकों में जगत् का वर्णन न होने से १।८७ में ‘सर्वस्यास्य गुप्त्यर्थम्’ शब्दों की क्या संगति हो सती है ? क्यों कि इन पदों से समस्त - जगत् का ग्रहण किया है । अतः जगदुत्पत्ति के श्लोकों से ही संगति हो सकती है, युगानुरूप धर्मादि के हृास से नहीं । और इस अध्याय का विषय वर्णन करते हुए (१।१४४) श्लोक में सर्ग - रचना तथा धर्म बताया है, पुनः युगानुरूप फलकथन की इस विषय से क्या संगति ? और यह युगानुसार फलकथन मनु की मौलिक - मान्यता से भी विरूद्ध है । मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, अतः मनु का समस्त आधार धर्म - अधर्मानुसार (शुभ - अशुभकर्मानुसार) ही है । इस धर्मानुसार फलकथन की संगति युगानुरूप फलकथन से कदापि नहीं हो सकती । यदि युगानुरूप ही फल प्राप्त होवे तो मनुस्मृति का समस्त प्रयोजन ही धराशायी हो जाता है । और यह शास्त्र सब युगों के लिये निरर्थक हो जाता है और इन श्लोकों में चारों युगों में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को धर्म माना है । परन्तु मनु ने इन्हें सार्वभौम सार्वकालिक मानव - मात्र का धर्म माना है । और ‘‘राजा हि युगमुच्यते’’ (९।३०१) में राजा को ही युगा का कारण मनु ने क्यों कहा ? इससे स्पष्ट है कि ये सब श्लोक पौराणिक - युग की देन होने से प्रक्षिप्त हैं ।
अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ।
अन्ये कलियुगे नॄणां युगह्रासानुरूपतः । ।1/85
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
युग के अनुसार मनुष्यों का धर्म सब युगों में पृथक् पृथक् होता है अर्थात् सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग में अलग 2 धर्म होता है।
टिप्पणी :
यह श्लोक स्वार्थियों के मिलाए हुए ज्ञात होते हैं, क्योंकि धर्म चारों युगों में एक समान रहता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।८१-८६ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - १।८० श्लोक की १।८७वें श्लोक से सृष्टि -रचना तथा उसकी रक्षा से सम्बन्ध होने से पूर्णतः संगति है । इनके मध्य में युगानुरूप धर्मादि का हृास और युगानुरूप फल - कथन की संगति प्रकरणविरूद्ध तथा मनु की मान्यता से विरूद्ध है । १।८१-८६ तक श्लोकों में जगत् का वर्णन न होने से १।८७ में ‘सर्वस्यास्य गुप्त्यर्थम्’ शब्दों की क्या संगति हो सती है ? क्यों कि इन पदों से समस्त - जगत् का ग्रहण किया है । अतः जगदुत्पत्ति के श्लोकों से ही संगति हो सकती है, युगानुरूप धर्मादि के हृास से नहीं । और इस अध्याय का विषय वर्णन करते हुए (१।१४४) श्लोक में सर्ग - रचना तथा धर्म बताया है, पुनः युगानुरूप फलकथन की इस विषय से क्या संगति ? और यह युगानुसार फलकथन मनु की मौलिक - मान्यता से भी विरूद्ध है । मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, अतः मनु का समस्त आधार धर्म - अधर्मानुसार (शुभ - अशुभकर्मानुसार) ही है । इस धर्मानुसार फलकथन की संगति युगानुरूप फलकथन से कदापि नहीं हो सकती । यदि युगानुरूप ही फल प्राप्त होवे तो मनुस्मृति का समस्त प्रयोजन ही धराशायी हो जाता है । और यह शास्त्र सब युगों के लिये निरर्थक हो जाता है और इन श्लोकों में चारों युगों में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को धर्म माना है । परन्तु मनु ने इन्हें सार्वभौम सार्वकालिक मानव - मात्र का धर्म माना है । और ‘‘राजा हि युगमुच्यते’’ (९।३०१) में राजा को ही युगा का कारण मनु ने क्यों कहा ? इससे स्पष्ट है कि ये सब श्लोक पौराणिक - युग की देन होने से प्रक्षिप्त हैं ।
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानं उच्यते ।
द्वापरे यज्ञं एवाहुर्दानं एकं कलौ युगे । ।1/86
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
सतयुग में केवल तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ, और कलियुग में दान ही मुख्य रक्खा गया।
टिप्पणी :
यह श्लोक स्वार्थियों के मिलाए हुए ज्ञात होते हैं, क्योंकि धर्म चारों युगों में एक समान रहता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।८१-८६ तक छः श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - १।८० श्लोक की १।८७वें श्लोक से सृष्टि -रचना तथा उसकी रक्षा से सम्बन्ध होने से पूर्णतः संगति है । इनके मध्य में युगानुरूप धर्मादि का हृास और युगानुरूप फल - कथन की संगति प्रकरणविरूद्ध तथा मनु की मान्यता से विरूद्ध है । १।८१-८६ तक श्लोकों में जगत् का वर्णन न होने से १।८७ में ‘सर्वस्यास्य गुप्त्यर्थम्’ शब्दों की क्या संगति हो सती है ? क्यों कि इन पदों से समस्त - जगत् का ग्रहण किया है । अतः जगदुत्पत्ति के श्लोकों से ही संगति हो सकती है, युगानुरूप धर्मादि के हृास से नहीं । और इस अध्याय का विषय वर्णन करते हुए (१।१४४) श्लोक में सर्ग - रचना तथा धर्म बताया है, पुनः युगानुरूप फलकथन की इस विषय से क्या संगति ? और यह युगानुसार फलकथन मनु की मौलिक - मान्यता से भी विरूद्ध है । मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, अतः मनु का समस्त आधार धर्म - अधर्मानुसार (शुभ - अशुभकर्मानुसार) ही है । इस धर्मानुसार फलकथन की संगति युगानुरूप फलकथन से कदापि नहीं हो सकती । यदि युगानुरूप ही फल प्राप्त होवे तो मनुस्मृति का समस्त प्रयोजन ही धराशायी हो जाता है । और यह शास्त्र सब युगों के लिये निरर्थक हो जाता है और इन श्लोकों में चारों युगों में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को धर्म माना है । परन्तु मनु ने इन्हें सार्वभौम सार्वकालिक मानव - मात्र का धर्म माना है । और ‘‘राजा हि युगमुच्यते’’ (९।३०१) में राजा को ही युगा का कारण मनु ने क्यों कहा ? इससे स्पष्ट है कि ये सब श्लोक पौराणिक - युग की देन होने से प्रक्षिप्त हैं ।
सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः ।
मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत् । ।1/87
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
इस सारे संसार का कार्य चलाने के हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण शरीर के चार भाग मुख, वाहु, उरु और पाँव के अनुसार बनाये। और चारों वर्णों के काम पृथक्-पृथक् निर्धारित किये।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(अस्य सर्वस्य सर्गस्य) इस ५ - ८० पर्यन्त श्लोकों में वर्णित समस्त संसार की (गुप्त्यर्थम्) गुप्ति अर्थात् सुरक्षा, व्यवस्था एवं समृद्धि के लिए (सः महाद्युतिः) महातेजस्वी परमात्मा ने मुख - बाहुं - ऊरू - पद् - जानाम् मुख, बाहु जघा और पैर की तुलना से निर्मितों के अर्थात् क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के पृथक् (कर्माणि अकल्पयत्) पृथक् - पृथक् कर्म बनाये ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(सर्वस्य तु सर्गम्य) सब सृष्टि की (गुप्ति अर्धम) रक्षा के लिए (य महाधुति:) उस तेजस्वी ब्रहा्र ने (मुख बाहु उरू पत जानाम) मुख बाहु जंधा और पैर के स्थानपत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रो के (पृथक कर्माणि अकत्पयत) अलग अलग कर्म बनाये
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
उस महातेजस्वी परमेष्ठी ने इस सब सृष्टि की रक्षा के लिए मुख, बाहु, जाँघ और पारद सद्श गुणधर्मों से उत्पन्न वर्णों के पृथक्-पृथक् कर्म आदिष्ट किये।
अध्यापनं अध्ययनं यजनं याजनं तथा ।
दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानां अकल्पयत् । ।1/88
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यह छह कर्म ब्राह्मण के लिये बनाये।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
(ब्राह्मणानाम्) ब्राह्मणों के अध्ययनम् अध्यापनम् पढ़ना - पढ़ाना तथा तथा यजनं याजनम् यज्ञ करना - कराना, दानं, च प्रतिग्रहम् एव दान देना और लेना, ये छः कर्म अकल्पयत् हैं ।
टिप्पणी :
(स० प्र० चतुर्थ समु०) ‘‘एक निष्कपट होके प्रीति से पुरूष पुरूषों को और स्त्री स्त्रियों को पढ़ावे - दो - पूर्ण विद्या पढें, तीन - अग्निहोत्रादि यज्ञ करें, चार - यज्ञ करावें, पांच - विद्या अथव सुवर्ण आदि का सुपात्रों को दान देवें, छठा - न्याय से धनोपार्जन करने वाले गृहस्थों से दान लेवें भी ।’’ (सं० वि० गृहाश्रम प्रकरण)
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(अघ्यापनम) पढाना (अघ्ययनम) पढना (यजनम) यज्ञ करना (याजन तथा) और यज्ञ करना (दान) दान देना (प्रतिग्रह च एव) और दान लेना (ब्राह्मणाम) ब्राह्मणो के धर्म (अकल्पयत) निश्चित किये।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
ब्राह्मणों के पढ़ना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, और लेना-ये छह कर्म निर्दिष्ट किये।
प्रजानां रक्षणं दानं इज्याध्ययनं एव च ।
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः । ।1/89
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यह छह कर्म ब्राह्मण के लिये बनाये।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
. ‘‘दीर्घ ब्रह्मचर्य से अध्ययनम् सांगोपांग वेदादि शास्त्रों को यथावत् पढ़ना, इज्या अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना दानम् सुपात्रों को विद्या, सुवर्ण आदि और प्रजा को अभयदान देना, प्रजानां रक्षणम् प्रजाओं का सब प्राकर से सर्वदा यथावत् पालन करना........ (विषयेष्वप्रसक्तिः) विषयों में अनासक्त होके सदा जितेन्द्रिय रहना - लोभ, व्यभिचार, मद्यपानादि नशा आदि दुव्र्यसनों से पृथक् रहकर विनय सुशीलतादि शुभ कर्मों में सदा प्रवृत्त रहना’’ ।
टिप्पणी :
(सं० प्र० षष्ठ समु०) क्षत्रियस्य समासतः ये संक्षेप से क्षत्रिय के कर्म हैं । ‘‘न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन दान विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना इज्या अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना अध्ययन वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में न फंसकर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर आत्मा से बलवान् रहना ।’’
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(प्रजानां रक्षणम्) प्रजा की रक्षा (दानम्) दान, (इज्या) यज्ञ, (अध्ययनम् एव च) और पढ़ना (विषयेषु, अप्रसक्तिः च) और विषयों में न लगना (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय के धर्म हैं (समासतः) संक्षेप से।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, विद्या-धर्म के प्रवर्तन और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना, अग्निहोत्रादि यज्ञ करना, वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, और विषयों में न फंसकर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बलवान् रहना, ये संक्षेप से क्षत्रिय के कर्म आदिष्ट किये।
पशूनां रक्षणं दानं इज्याध्ययनं एव च ।
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिं एव च । ।1/90
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
चौपायों की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती (कृषि) करना, ये सात कर्म वैश्यों के लिये नियत किये हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
वैश्य के कर्म - ‘‘पशुरक्षा गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना, दान विद्याधर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का व्यय करना इज्या अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना अध्ययन वेदादि शास्त्रों का वणिक्पथ सब प्रकार के व्यापार करना कुसीद एक सैंकड़े में चार, छः, आठ, बारह , सोलह वा बीस आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रूपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रूपये से अधिक न लेना और न देना कृषि खेती करना वैश्यस्य ये वैश्य के कर्म हैं ।’’
टिप्पणी :
(स० प्र० चतुर्थ समु०) ‘‘अध्ययनम् वेदादि शास्त्रों का पढ़ना इज्या अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना दानम् अन्नादि का दान देना, ये तीन धर्म के लक्षण और पशूनां रक्षणम् गाय आदि पशुओं का पालन करना उनसे दुग्धादि का बेचना वणिक् पथम् नाना देशों की भाषा, हिसाब, भूगर्भविद्या, भूमि, बीज आदि के गुण जानना और सब पदार्थों के भावाभाव समझना कुसीदम् ब्याज का लेना कृषिमेव च खेती की विद्या का जानना, अन्न आदि की रक्षा, खात और भूमि की परीक्षा, जोतना, बोना , आदि व्यवहार का जानना, ये चार कर्म वैश्य की जीविका ।’’ (सं० वि० गृहाश्रम प्रक०) ‘‘सवा रूपये सैंकड़े से अधिक, चार आने से न्यून ब्याज न लेवें न देवें । जब दूना धन आ जाये, उससे आगे कौड़ी न लेवे, न देवे । जितना न्यून ब्याज लेवेगा उतना ही उसका धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसन्तान उसके कुल में न होंगे ।’’ (सं० वि० गृहाश्रम प्रक० में ऋ० दया० की टिप्पणी)
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(पशूनां रक्षणम्) पशु-पालन, (दानम्) दान, (इज्या) यज्ञ (अध्ययनम् एव च) और पढ़ना (वणिक् पथम्) व्यापार, (कुसीदं च) और लेन देन, (वैश्यस्य) वैश्य के धर्म हैं। (कृषिम् एव च) और खेती।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
गाय आदि पशुओं का पालन बर्धन करना, विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का व्यय करना, अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना, वेदादि शास्रों का पढ़ना, सब प्रकार के व्यापार करना, एक सैंकड़े में चार छह आठ सोलह व बीस आनों से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपए से अधिक न लेना और न देना, तथा खेती करना, ये वैश्य के कर्म अदिष्ट किये।१
टिप्पणी :
१. व्याज सम्बन्धी उपर्युक्त स्पष्टीकरण स्वामी जी ने दसवें अध्याय में आए ‘वशिष्ठविहितां’ तथा ‘कुसीदबृद्धिर्द्वैगुण्यं’ श्लोकों के आधार पर किया है। संस्कारविधि में स्वामी जी ने ‘वणिक्पथं’ की विस्तृत व्याख्या ‘‘नाना देशों की भाषा हिसाब भूगर्भविद्या भूमि बीज आदि के गुण जानना’’ और कृषि की ‘‘खेती की विद्या जानना, अन्नादि की रक्षा, खाद और भूमि की परीक्षा, जोतना बोना आदि व्यवहार का जानना’’ की है।
एकं एव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।
एतेषां एव वर्णानां शुश्रूषां अनसूयया । ।1/91
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
शूद्र के लिये एक ही कर्म प्रभु ने नियत किया अर्थात् तन और मन से तीनों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) की सेवा करना।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
‘‘प्रभुः परमेश्वर ने शूद्रस्य जो विद्याहीन - जिसको पढ़ने से भी विद्या न आ सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उस शूद्र के लिए एतेषामेव वर्णानाम इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की अनसूयया निन्दा से रहित प्रीति से शुश्रूषाम् सेवा करना, एकमेव कर्म यही एक कर्म समादिशत् करने की आज्ञा दी है ।’’
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(एकम् एव तु शूद्रस्य) शूद्र का केवल एक (प्रभुः) ब्रह्मा ने (कर्म) काम (सम् आदिशत्) बताया। (एतेषम् एव वर्णानाम्) इन वर्णों की ही (शुश्रूषां) सेवा को (अनुसूयया) बिना निन्दा के। शूद्र को बिना संकोच अन्य वर्णों की सेवा करनी चाहिये।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म समादिष्ट किया है; और वह है निन्दा ईर्ष्या अभिमान आदि दोषों को छोड़ कर इन्हीं तीनों वर्णों की यथावत् सेवा करना।
ऊर्ध्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः ।
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखं उक्तं स्वयंभुवा । ।1/92
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
पुरुष के सब अंग नाभि से शिषा पय्र्यनत पवित्र हैं। विशेषकर मुख और भी अधिक पवित्र है। यह ब्रह्माजी ने कहा है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(ऊध्र्वं नाभेः) नाभि से ऊपर, (मेध्यातरः) पवित्र, (पुरुषः परिकीत्र्तितः) पुरुष बताया गया है (तस्मात्) उससे भी (मेध्यतमम्) पवित्र (तु) तो (अस्य मुखम्) इसका मुख (उक्तम्) बताया गया (स्वयंभुवा) ब्रह्मा से। ब्रह्मा ने बताया है कि नाभि से ऊपर जितना जितना चलते जाओ उतना उतना पवित्र है और मुख सबसे पवित्र है।
उत्तमाङ्गोद्भवाज्ज्येष्ठ्याद्ब्रह्मणश्चैव धारणात् ।
सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः । ।1/93
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
संसार में ब्राह्मण धर्म के कारण सर्वश्रेष्ठ हैं, इस हेतु कि सबसे पवित्र अंग अर्थात् मुँह का कार्य करते हैं और वेदानुसार कर्म करते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(उत्तम-अंग-उद्धवात्) उत्तम अंग होने से (ज्यैष्ठयात्) ज्येष्ठ होने से (ब्रह्मणः च एव धारणात्) और वेद के धारण करने से (सर्वस्य एव अस्य सर्गस्य) इस सब सृष्टि का (धर्मतः) धर्म के हिसाब से (ब्राह्मणः प्रभुः) ब्राह्मण प्रभु है।
पतं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसृजत् ।
हव्यकव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये । ।1/94
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
ब्रह्माजी ने अपने तपोबल से पहले ब्राह्मण को अपने मुँह से उपदेश देकर उत्पन्न किया जिससे कि सारे संसार की रक्षा करें और मन्त्रबल से देवताओं को द्रव्य और पितरों को कव्य पहुँचावें।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।
कव्यानि चैव पितरः किं भूतं अधिकं ततः । ।1/95
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
उस ब्राह्मण से बढ़कर और कौन है कि जिसके मुख से देवतागण हव्य और पितरगण कव्य खाते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः । ।1/96
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
चर-अचर प्राणियों में कीड़ा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ चौपाया, उससे श्रेष्ठ मनुष्य और उससे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः) सब चीजों में जीव श्रेष्ठ हैं। (प्राणिनां बुद्धिजीविनः) जीवधारियों में बुद्धि वाले श्रेष्ठ हैं। (बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः) बुद्धि वालों में मनुष्य श्रेष्ठ है। (नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः) और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है।
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।
कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः । ।1/97
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
ब्राह्मणों में वेदशास्त्र के पढ़ने वाले, उनसे वेदशास्त्र के अनुसार काय्र्य करने की इच्छा रखने वाले, उनसे वेदशास्त्रानुसार कर्म करने वाले, और उनसे अधिक ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(ब्राह्मणेषु च विद्वांसः) और ब्राह्मणों में विद्वान् श्रेष्ठ हैं। (विद्वत्सु कृतबुद्धयः) विद्वानों में विचित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ हैं। (कृतबुद्धिषु कर्तारः) विचित्र बुद्धि वालों में वे जो नया आविष्कार करते हैं। (कृर्तृषु ब्रह्मवेदिनः) और आविष्कार-कत्र्ताओं में वह श्रेष्ठ है जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं।
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।
स हि धर्मार्थं उत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते । ।1/98
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
ब्राह्मण धर्म की मूर्ति है, और धर्म करने के लिये उत्पन्न किया गया है, अतएव मुक्ति पाने के योग्य होता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(उत्पत्तिः एव विप्रस्य) ब्राह्मण की उत्पत्ति अर्थात् नियुक्ति ही (मूर्तिः धर्मस्य शाश्वती) सदा धर्म की मूर्ति है। (स हि धर्मार्थम् उत्पन्नः) वह तो धर्म के लिये ही बनाया गया है। (ब्रह्मभूयाय) मोक्ष के लिये (कल्पते) माना जाता है।
ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यां अधिजायते ।
ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये । ।1/99
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
परमेश्वर ने धर्मकोप (खजाना) की रक्षा के हेतु वेदवान् (वेदज्ञाता) ब्राह्मणों को उत्पन्न किया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(ब्राह्मणः जायमानः हि) ब्राह्मण उत्पन्न होकर ही (पृथिव्याम् अधिजायते) पृथिवी में सर्वोपरि होता है। (ईश्वर सर्वभूतानाम्) सब प्राणियों में मुख्य और (धर्मकोशस्य गुप्तये) धर्मकोश की रक्षा के लिये।
सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किं चिज्जगतीगतम् ।
श्रैष्ठ्येनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति । ।1/100
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जो कुछ इस संसार में है यह सब ब्राह्मण के हेतु है, क्योंकि ब्राह्मण अपने ज्ञानबल से उनका ठीक ठीक लाभ भोग सकता है और दूसरे वर्ण ज्ञान की न्यूनता के कारण लाभ नहीं भोग सकते। इस हेतु सब कुछ ब्राह्मण ही का है, क्योंकि वह ब्रह्माजी के उपदेश से सबको धर्म की शिक्षा देने (सिखलाने) के हेतु उत्पन्न हुआ है। अतएव सबसे श्रेष्ठ हैं।
टिप्पणी :
इस श्लोक से ज्ञान की श्रेष्ठता दर्शती है। और शेष के समान यह श्लोक मिलाया हुआ है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(सर्वं स्वं ब्राह्मणस्य इदम्) यह सब ब्राह्मण का है (यत्किंचित् जगतीगतम्) जो कुछ जगत में है। (श्रैष्ठ्येन अभिजनेन) श्रेष्ठ योनि के कारण (इदं सर्वं वै ब्राह्मणो अर्हति) ब्राह्मण इस सबके योग्य है। अर्थात् देहधारियों में श्रेष्ठ होने के कारण ब्राह्मण को समस्त जगत् की रक्षा का भार सौंपा गया है। गत श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मण धर्मकोश की रक्षा के लिये है।
स्वं एव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।
आनृशंस्याद्ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः । ।1/101
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
ब्राह्मण अपनी ही वस्तुओं को खाता, पहिनता और देता है। उसकी कृपा से क्षत्रिय लोग अर्थात् दूसरे मनुष्य आनंद करते हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(स्वम् एव ब्राह्मणः भुक्ते) ब्राह्मण अपना ही खाता है। (स्वं वस्ते) अपना ही पहनता है (स्व ददाति च) और अपना ही दान करता है। (आनृशंस्याद् ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण की कृपा से ही (भुंजते) खाते हैं (हि इतरे जनाः) दूसरे मनुष्य। अर्थात् यदि ब्राह्मण धर्मकोश की रक्षा करने की कृपा न करे तो जगत् बिगड़ जाये और अन्य लोगों को सुख न मिले।
तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणां अनुपूर्वशः ।
स्वायंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रं अकल्पयत् । ।1/102
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
उस ब्राह्मण के कर्म और क्षत्रिय आदि के कर्म के ज्ञानार्थ ब्रह्मा के पुत्र मनुजी ने इस शास्त्र का बनाया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
विदुषा ब्राह्मणेनेदं अध्येतव्यं प्रयत्नतः ।
शिश्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्नान्येन केन चित् । ।1/103
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
वे ब्राह्मण पण्डित हैं, वे इस शास्त्र को यत्न से पढ़े और शिष्यों (चेलों विद्यार्थियों) को भी पढ़ावें और क्षत्रिय आदि भी पढ़ें, किन्तु पढ़ावें नहीं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
इदं शास्त्रं अधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः ।मनोवाग्गेहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते । ।1/104
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जो ब्राह्मण इस शास्त्र को पढ़ता है और व्रत करता है, वह मन, वाणी और शरीर से उत्पन्न हुए कर्म दोष से लिप्त नहीं होता।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
पुनाति पङ्क्तिं वंश्यांश्च सप्तसप्त परावरान् ।पृथिवीं अपि चैवेमां कृत्स्नां एकोऽपि सोऽर्हति । ।1/105
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
पापियों की मुक्ति को ब्राह्मण पवित्र करता है। वह अपनी सात पुश्त ऊपर ओर सात पुश्त नीचे की पवित्र करता है। वह सारी पृथ्वी को अकेला धारण कर सकता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठं इदं बुद्धिविवर्धनम् ।इदं यशस्यं आयुष्यं इदं निःश्रेयसं परम् । ।1/106
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
यह शास्त्र कल्याण, बुद्धि, यश, आयु और दाता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम् ।चतुर्णां अपि वर्णानां आचारश्चैव शाश्वतः । ।1/107
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
इस शास्त्र में सारे धर्म कर्मों के गुण-दोष और चारों वर्णों के आचार कहे हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।९२-१०७ तक १६ श्लोक निम्न - कारणों से प्रक्षिप्त हैं - क्यों कि इनमें ‘पक्षपात - पूर्ण’ ब्राह्मणों की प्रशंसा और मध्य में इस शास्त्र की अप्राकरणिक प्रशंसा की गई है । इस अध्याय के वण्र्य - विषय से इनकी कोई संगति नहीं है । वर्णों के कर्म - विवेचन से यदि कोई इनका सम्बन्ध बताना चाहे, तो भी उचित नहीं । क्यों कि वर्णों में दूसरे वर्ण भी अपेक्षाकृत प्रशस्य हैं, उनका यहाँ लेशमात्र भी वर्णन क्यों नहीं ? ब्राह्मण को ही धर्म की मूत्र्ति , सब धनों का स्वामी , तथा उसी की कृपा से दूसरे वर्णों का जीवन बताना अतिशयोक्तिपूर्ण, असंगत वर्णन किया है । और पूर्वापर - प्रकरण से भी इन श्लोकों का स्पष्ट विरोध है । इससे पूर्व १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का वर्णन किया है , और १।१०८ से कर्मानुसार आचरण को धर्म कहने से धर्म का स्वरूप बताया गया है । १।१०२ से १०७ तक श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी तथा शास्त्र की महिमा बताई है, इसकी संगति ग्रन्थ के प्रारम्भ अथवा अन्त में तो कुछ अंश में संगत कही जा सकती है, किन्तु यहां मध्य में सर्वथा असंगत है । इन श्लोकों में ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी इन्हें अर्वाचीन ही सिद्ध करता है, क्यों कि इस मनुस्मृति के लिये ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग मनु जैसा आप्तपुरूष स्वयं नहीं कर सकता । और जो मूल प्रवक्ता १।१४४ में स्वयं यह कह रहा है कि मैंने इस अध्याय में सृष्टि - उत्पत्ति तथा धर्मोत्पत्ति ही कही है, क्या उसके कथन के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के विरूद्ध दूसरे विषयों का वर्णन उचित हो सकता है ? ये श्लोक उस समय के सिद्ध होते हैं कि जिस समय धर्म - शास्त्र के नाम पर अनेक - स्मृतियों की रचना हो गई, उस समय किसी विद्वान् ने इसकी प्रशंसा में इन श्लोकों को मिलाया है । और मनु की शैली के अनुकूल भी ये श्लोक नहीं हैं, मनु तो प्रथम विषय का निर्देश करके और समाप्ति पर भी विषय - निर्देश अवश्य करते हैं । इन श्लोकों में कहीं भी विषय का निर्देश नहीं है । और मनु की प्रवचन - शैली का भी इन श्लोकों में अभाव है । और १।९४-९५ श्लोकों में ब्राह्मण के मुख से पितरों का हव्य - कव्य भक्षण करना तथा १।१०५ में अगली - पिछली सात - सात पीढि़यों का पवित्र करना मनु की मान्यता से विरूद्ध है । मृतक - श्राद्ध की पौराणिक भावना के प्रचलित होने पर इन श्लोकों को किसी ने मिलाया है । मनु के मत में वेद - विरूद्ध मृतक - श्राद्ध का कोई स्थान नहीं है, वे तो जीवित - पितरों की ही सेवा का सर्वत्र विधान करते हैं । और सात - सात पीढि़यों का पवित्र होना कर्मानुसार - फल - व्यवस्था को खण्डित करता है । चाहे मनुष्य कितने भी पाप - कर्म करते रहें, और इस शास्त्र का पाठ कर लें, यदि वे पापी पवित्र हो जायेंगे, तो पाप का फल कौन भोगेगा ? इससे पाप करने को प्रोत्साहन ही मिलता है । अतः किसी अधर्मात्मा पुरूष ने ही ये श्लोक बनाये हैं , मनु जैसे पवित्र व्यक्ति ऐसी वेद तथा ईश्वरीय न्याय के विरूद्ध - बात को कभी नहीं लिख सकता । और १।१०२ वें श्लोक में मनु अपने को ‘धीमान्’ भी नहीं कह सकते । और मनु ने वर्ण - व्यवस्था को कर्म - मूलक माना है, जन्ममूलक नहीं, किन्तु इन (१।९८-९९) श्लोकों में ब्राह्मण को जन्म से ही बड़ा कहकर जन्म मूलक माना है । यदि जन्म से ही कोई बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है, उसे कर्म करने (विद्यादि पढ़ना आदि) की क्या आवश्यकता रहेगी ? परन्तु मनु की मान्यता कर्म - प्रधान है । जो द्विज (२।१६८) वेद से अन्यत्र श्रम करता है, जो (२।१०३) प्रातः सांय सन्ध्या नहीं करता, उसको मनु ने शूद्र मानकर सभी द्विज - कर्मों से बहिष्कार का आदेश दिया है । और ४।२४५ वें श्लोक में तो स्पष्ट ही जन्म मूलक श्रेष्ठता का विरोध करके लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ - कर्मों से श्रेष्ठता तथा दुष्कर्मों के करने से हीनता को प्राप्त होता है । और निश्चित समय पर उपनयनादि न करने से ‘व्रात्य’ कहलाता है । इससे भी जन्म की श्रेष्ठता का खण्डन होता है । और मनु ने १।३१ में शरीर के अंगों से जो वर्णों की समानता बताई है, वह भी वर्णों में कर्म को मुख्य मानकर ही आलंकारिक वर्णन किया है । अतः जन्म से श्रेष्ठता बताने वाले, मृतकश्राद्ध के पोषक तथा पूर्वापर प्रकरण से विरूद्ध ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(अस्मिन्) इस शास्त्र में (धर्मः अखिलेन उक्तः) पूरा धर्म बताया गया है। (गुण दोषौ च कर्मणाम्) और कर्मों के गुण दोष भी। (चतुर्णाम् अपि वर्णानाम् आचारः च एव शाश्वतः) और चारों वर्णों का नित्य का आचार भी।
आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च ।तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्विजः । ।1/108
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जो आचार वेदशास्त्र में कहे हैं, वह परमधर्म हैं। इस हेतु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपना भला चाहें, वह इस शास्त्रानुसार कर्म करें।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
उपरोक्त श्लोक देकर स्वामी जी ने निम्न अर्थ दिया है - ‘‘कहने सुनने - सुनाने, पढ़ने - पढ़ाने का फल यह है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना । इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रहे ।’’ (स० प्र० तृतीय समु०) ‘‘जो सत्य - भाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है । ’’ (स० प्र० दशम समु०) श्रुत्युक्तः च स्मार्त एव वेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में भी कहा हुआ जो आचारः आचरण है परमः धर्मः वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तस्मात् इसीलिए आत्मवान् द्विजः आत्मोन्नति चाहने वाले द्विज को चाहिए कि वह अस्मिन् इस श्रेष्ठाचरण में सदा नित्यं युक्तः स्यात् सदा निरन्तर प्रयत्नशील रहे ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(आचारः परमः धर्मः श्रुति-उक्तः स्मार्त एव च) वेद में बताया हुआ और स्मृति में बताया हुआ सदाचार परम धर्म है। (तस्मात्) इसलिये (अस्मिन् सदा युक्तः नित्यं स्यात्) इसमें सदा तत्पर रहे (आत्मवान् द्विजः) आत्मज्ञानी द्विज।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
परम धर्म यही है-सुनने सुनाने और पढ़ने पढ़ाने का फल यही है-कि वेद और वेदानुकूल स्मृतिओं में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना। इसलिए आत्माभिमानो ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य द्विज इस धर्माचरण में सदा नित्य युक्त रहे।
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलं अश्नुते ।आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाज्भवेत् । ।1/109
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
आचार-रहित ब्राह्मण वेद के फल का भोग नहीं कर सकता। और आचार-सहित ब्राह्मण वेदों के फल का भोग कर सकता है।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
आचारात् विच्युतः विप्रः जो धर्माचरण से रहित द्विज है वह वेदफलं न अश्नुते वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो आचारेण तु संयुक्तः विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है, वही सम्पूर्णफलभाक् भवेत् सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है । (स० प्र० तृतीय समु०)
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(आचारात् विच्युतः विप्रः) आचार से गिरा हुआ विद्वान् (न वेदफलम् अश्नुते) वेद के फल को नहीं पाता। (आचारेण तु संयुक्तः) और सदाचार से युक्त (सम्पूर्ण फलभाक् भवेत्) सब फल का भागी होता है।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
क्योंकि जो धर्माचरण से रहित द्विज है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल का प्राप्त नहीं हो सकता। किन्तु जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है।१
एवं आचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् ।सर्वस्य तपसो मूलं आचारं जगृहुः परम् । ।1/110
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
जब मनुजी ने देखा कि आचार से ही धर्म प्राप्त होता है, तब सब तपों का मूल जो आचार है, उसी को अपनाया।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
. एवम् इस प्रकार आचारतः धर्माचरण से ही धर्मस्य धर्म की गतिम् प्राप्ति एवं अभिवृद्धि दृष्ट्वा देखकर मुनयः मुनियों ने सर्वस्य तपसः परं मूलम् सब तपस्याओं का श्रेष्ठ मूल आधार आचारम् धर्माचरण को ही जगृहुः स्वीकार किया है ।
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
(एवम्) इस प्रकार (आचारतः) आचार की अपेक्षा से (दृष्टवा) देखकर (धर्मस्य) धर्म के (मुनयः) मुनि लोगों ने (गतिम्) गति को (सर्वस्य तपसः) सब तप के (मूलम् आचारम्) मूल आचार को (जगृहुः) ग्रहण किया (परम्) बड़े को। इस प्रकार मुनियों ने धर्म की गति को सदाचार की अपेक्षा से देखकर सब तप के मूल सदाचार का ग्रहण किया।
Commentary by : पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
इस प्रकार मुनियों ने धर्माचरण से धर्म के प्रवर्तन का देख कर सब प्रकार की तपस्या के मूल श्रेष्ठ आचार को ग्रहण किया।
जगतश्च समुत्पत्तिं संस्कारविधिं एव च ।व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम् । ।1/111
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
तनी बातें इस शास्त्र में कही गई हैं, सृष्टि उत्पत्ति, संस्कार* करने की विधि, व्रत की आवश्यकता, स्नान की विधि।
टिप्पणी :
*संस्कार 16 हैं:- 1-गर्भाधा न, 2-पुंसवन, 3-सीमन्तोन्नयन, 4-जातकर्म, 5-नामकरण, 6-निष्क्रमण, 7-अन्नप्राशन, 8-चूड़ाकर्म, 9-कर्णवेध, 10-उपनयन, 11-वेदारम्भ, 12-समावर्तन, 13-विवाह, 14-गृहस्थाश्रम, 15-वाणप्रस्थाश्रम, 16-सन्यास।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।१११ से ११८ तक आठ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।११० श्लोक में धर्म का प्रकरण है और १।१२० श्लोक में भी धर्म का वर्णन है । इस धर्मविषय के मध्य में इन प्रक्षिप्त श्लोकों में वर्णित विषय - सूची सर्वथा ही असंगत है । और यह विषयसूची यदि मौलिक होती, तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होनी चाहिये थी अथवा ग्रन्थ के अन्त में । किसी विषय के बीच में विषय - सूची की कोई संगति नहीं है । ये श्लोक मनु की शैली से भी विरूद्ध हैं । मनु प्रत्येक विषय का प्रारम्भ तथा अन्त में निर्देश अवश्य करते हैं, और प्रवचन - शैली में तो यह अत्यावश्यक होता है, परन्तु इन आठ श्लोकों में वण्र्य विषय का संकेत नहीं है । और १।११८ श्लोक में ‘शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मनुः’ कहकर तो प्रक्षेप्ता ने इनके प्रक्षिप्त होने का प्रबल प्रमाण ही दे दिया है । मनु का नाम लेकर किसी और ने ही इन्हें बनाया है और ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी मनु का नहीं है । क्यों कि प्रवचन को जब ग्रन्थरूप में संकलित किया गया, तदनन्तर ही ‘शास्त्र’ शब्द का मनुस्मृति के लिए व्यवहार सम्भव हो सकता है , स्वयं मनु द्वारा नहीं । और इन श्लोकों में जो विषय - सूची दिखाई गई है , उसके अनुसार मनुस्मृति में विषयों का वर्णन भी नही है । जैसे - १।११८ श्लोक में कहे कुलधर्म, व पाखण्डियों के धर्मों का कहीं मनुस्मृति में वर्णन ही नहीं है । और जिस विषय को मनु ने ‘कार्यविनिर्णय’ शब्द से कहा है, उसको इस विषय सूची में पृथक् - पृथक् ‘साक्षिप्रश्नविधान’, ‘स्त्रीपुरूषधर्म’, विभावधर्म आदि नामों से उल्लेख किया है और मनुस्मृति में वर्णित अनेक मुख्य विषयों - (प्रथम अध्याय में धर्मोत्पत्ति, १२वें अध्याय में त्रिविध गतियाँ, धर्मनिश्चयविधि आदि) का इस विषयसूची में अभाव ही है । अतः यह विषयसूची असंगत, शैली - विरूद्ध, तथा सर्वथा अपूर्ण है ।
दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लक्षणम् ।महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतम् । ।1/112
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
स्त्री प्रसंग, विवाहों का लक्षण, महायज्ञ विधान, श्राद्ध की विधि।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।१११ से ११८ तक आठ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।११० श्लोक में धर्म का प्रकरण है और १।१२० श्लोक में भी धर्म का वर्णन है । इस धर्मविषय के मध्य में इन प्रक्षिप्त श्लोकों में वर्णित विषय - सूची सर्वथा ही असंगत है । और यह विषयसूची यदि मौलिक होती, तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होनी चाहिये थी अथवा ग्रन्थ के अन्त में । किसी विषय के बीच में विषय - सूची की कोई संगति नहीं है । ये श्लोक मनु की शैली से भी विरूद्ध हैं । मनु प्रत्येक विषय का प्रारम्भ तथा अन्त में निर्देश अवश्य करते हैं, और प्रवचन - शैली में तो यह अत्यावश्यक होता है, परन्तु इन आठ श्लोकों में वण्र्य विषय का संकेत नहीं है । और १।११८ श्लोक में ‘शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मनुः’ कहकर तो प्रक्षेप्ता ने इनके प्रक्षिप्त होने का प्रबल प्रमाण ही दे दिया है । मनु का नाम लेकर किसी और ने ही इन्हें बनाया है और ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी मनु का नहीं है । क्यों कि प्रवचन को जब ग्रन्थरूप में संकलित किया गया, तदनन्तर ही ‘शास्त्र’ शब्द का मनुस्मृति के लिए व्यवहार सम्भव हो सकता है , स्वयं मनु द्वारा नहीं । और इन श्लोकों में जो विषय - सूची दिखाई गई है , उसके अनुसार मनुस्मृति में विषयों का वर्णन भी नही है । जैसे - १।११८ श्लोक में कहे कुलधर्म, व पाखण्डियों के धर्मों का कहीं मनुस्मृति में वर्णन ही नहीं है । और जिस विषय को मनु ने ‘कार्यविनिर्णय’ शब्द से कहा है, उसको इस विषय सूची में पृथक् - पृथक् ‘साक्षिप्रश्नविधान’, ‘स्त्रीपुरूषधर्म’, विभावधर्म आदि नामों से उल्लेख किया है और मनुस्मृति में वर्णित अनेक मुख्य विषयों - (प्रथम अध्याय में धर्मोत्पत्ति, १२वें अध्याय में त्रिविध गतियाँ, धर्मनिश्चयविधि आदि) का इस विषयसूची में अभाव ही है । अतः यह विषयसूची असंगत, शैली - विरूद्ध, तथा सर्वथा अपूर्ण है ।
वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च ।भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिं एव च । ।1/113
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
वृत्ति (जीविका) का लक्षण, स्नातक (ब्रह्मचारी) का व्रत, भक्ष्य और अभक्ष्य (खाने वाले और न खाने वाले) पदार्थ, शौच (पवित्रता), द्रव्यों को शुद्ध करने की विधि।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।१११ से ११८ तक आठ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।११० श्लोक में धर्म का प्रकरण है और १।१२० श्लोक में भी धर्म का वर्णन है । इस धर्मविषय के मध्य में इन प्रक्षिप्त श्लोकों में वर्णित विषय - सूची सर्वथा ही असंगत है । और यह विषयसूची यदि मौलिक होती, तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होनी चाहिये थी अथवा ग्रन्थ के अन्त में । किसी विषय के बीच में विषय - सूची की कोई संगति नहीं है । ये श्लोक मनु की शैली से भी विरूद्ध हैं । मनु प्रत्येक विषय का प्रारम्भ तथा अन्त में निर्देश अवश्य करते हैं, और प्रवचन - शैली में तो यह अत्यावश्यक होता है, परन्तु इन आठ श्लोकों में वण्र्य विषय का संकेत नहीं है । और १।११८ श्लोक में ‘शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मनुः’ कहकर तो प्रक्षेप्ता ने इनके प्रक्षिप्त होने का प्रबल प्रमाण ही दे दिया है । मनु का नाम लेकर किसी और ने ही इन्हें बनाया है और ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी मनु का नहीं है । क्यों कि प्रवचन को जब ग्रन्थरूप में संकलित किया गया, तदनन्तर ही ‘शास्त्र’ शब्द का मनुस्मृति के लिए व्यवहार सम्भव हो सकता है , स्वयं मनु द्वारा नहीं । और इन श्लोकों में जो विषय - सूची दिखाई गई है , उसके अनुसार मनुस्मृति में विषयों का वर्णन भी नही है । जैसे - १।११८ श्लोक में कहे कुलधर्म, व पाखण्डियों के धर्मों का कहीं मनुस्मृति में वर्णन ही नहीं है । और जिस विषय को मनु ने ‘कार्यविनिर्णय’ शब्द से कहा है, उसको इस विषय सूची में पृथक् - पृथक् ‘साक्षिप्रश्नविधान’, ‘स्त्रीपुरूषधर्म’, विभावधर्म आदि नामों से उल्लेख किया है और मनुस्मृति में वर्णित अनेक मुख्य विषयों - (प्रथम अध्याय में धर्मोत्पत्ति, १२वें अध्याय में त्रिविध गतियाँ, धर्मनिश्चयविधि आदि) का इस विषयसूची में अभाव ही है । अतः यह विषयसूची असंगत, शैली - विरूद्ध, तथा सर्वथा अपूर्ण है ।
स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासं एव च ।राज्ञश्च धर्मं अखिलं कार्याणां च विनिर्णयम् । ।1/114
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
स्त्रियों का धर्म-योग, तप, मोक्ष और सन्यास धर्म, राजाओं का धर्म, और सब कामों का विचार।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।१११ से ११८ तक आठ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।११० श्लोक में धर्म का प्रकरण है और १।१२० श्लोक में भी धर्म का वर्णन है । इस धर्मविषय के मध्य में इन प्रक्षिप्त श्लोकों में वर्णित विषय - सूची सर्वथा ही असंगत है । और यह विषयसूची यदि मौलिक होती, तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होनी चाहिये थी अथवा ग्रन्थ के अन्त में । किसी विषय के बीच में विषय - सूची की कोई संगति नहीं है । ये श्लोक मनु की शैली से भी विरूद्ध हैं । मनु प्रत्येक विषय का प्रारम्भ तथा अन्त में निर्देश अवश्य करते हैं, और प्रवचन - शैली में तो यह अत्यावश्यक होता है, परन्तु इन आठ श्लोकों में वण्र्य विषय का संकेत नहीं है । और १।११८ श्लोक में ‘शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मनुः’ कहकर तो प्रक्षेप्ता ने इनके प्रक्षिप्त होने का प्रबल प्रमाण ही दे दिया है । मनु का नाम लेकर किसी और ने ही इन्हें बनाया है और ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी मनु का नहीं है । क्यों कि प्रवचन को जब ग्रन्थरूप में संकलित किया गया, तदनन्तर ही ‘शास्त्र’ शब्द का मनुस्मृति के लिए व्यवहार सम्भव हो सकता है , स्वयं मनु द्वारा नहीं । और इन श्लोकों में जो विषय - सूची दिखाई गई है , उसके अनुसार मनुस्मृति में विषयों का वर्णन भी नही है । जैसे - १।११८ श्लोक में कहे कुलधर्म, व पाखण्डियों के धर्मों का कहीं मनुस्मृति में वर्णन ही नहीं है । और जिस विषय को मनु ने ‘कार्यविनिर्णय’ शब्द से कहा है, उसको इस विषय सूची में पृथक् - पृथक् ‘साक्षिप्रश्नविधान’, ‘स्त्रीपुरूषधर्म’, विभावधर्म आदि नामों से उल्लेख किया है और मनुस्मृति में वर्णित अनेक मुख्य विषयों - (प्रथम अध्याय में धर्मोत्पत्ति, १२वें अध्याय में त्रिविध गतियाँ, धर्मनिश्चयविधि आदि) का इस विषयसूची में अभाव ही है । अतः यह विषयसूची असंगत, शैली - विरूद्ध, तथा सर्वथा अपूर्ण है ।
साक्षिप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरपि ।विभागधर्मं द्यूतं च कण्टकानां च शोधनम् । ।1/115
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
साक्षी के ¬प्रश्न का विधान अर्थात् गवाह की गवाही की विधि, पुरुष और स्त्री का धर्म, धर्म के विभाग, द्युत (जुआ) के विषय में, अपराधियों के दण्ड।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।१११ से ११८ तक आठ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।११० श्लोक में धर्म का प्रकरण है और १।१२० श्लोक में भी धर्म का वर्णन है । इस धर्मविषय के मध्य में इन प्रक्षिप्त श्लोकों में वर्णित विषय - सूची सर्वथा ही असंगत है । और यह विषयसूची यदि मौलिक होती, तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होनी चाहिये थी अथवा ग्रन्थ के अन्त में । किसी विषय के बीच में विषय - सूची की कोई संगति नहीं है । ये श्लोक मनु की शैली से भी विरूद्ध हैं । मनु प्रत्येक विषय का प्रारम्भ तथा अन्त में निर्देश अवश्य करते हैं, और प्रवचन - शैली में तो यह अत्यावश्यक होता है, परन्तु इन आठ श्लोकों में वण्र्य विषय का संकेत नहीं है । और १।११८ श्लोक में ‘शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मनुः’ कहकर तो प्रक्षेप्ता ने इनके प्रक्षिप्त होने का प्रबल प्रमाण ही दे दिया है । मनु का नाम लेकर किसी और ने ही इन्हें बनाया है और ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी मनु का नहीं है । क्यों कि प्रवचन को जब ग्रन्थरूप में संकलित किया गया, तदनन्तर ही ‘शास्त्र’ शब्द का मनुस्मृति के लिए व्यवहार सम्भव हो सकता है , स्वयं मनु द्वारा नहीं । और इन श्लोकों में जो विषय - सूची दिखाई गई है , उसके अनुसार मनुस्मृति में विषयों का वर्णन भी नही है । जैसे - १।११८ श्लोक में कहे कुलधर्म, व पाखण्डियों के धर्मों का कहीं मनुस्मृति में वर्णन ही नहीं है । और जिस विषय को मनु ने ‘कार्यविनिर्णय’ शब्द से कहा है, उसको इस विषय सूची में पृथक् - पृथक् ‘साक्षिप्रश्नविधान’, ‘स्त्रीपुरूषधर्म’, विभावधर्म आदि नामों से उल्लेख किया है और मनुस्मृति में वर्णित अनेक मुख्य विषयों - (प्रथम अध्याय में धर्मोत्पत्ति, १२वें अध्याय में त्रिविध गतियाँ, धर्मनिश्चयविधि आदि) का इस विषयसूची में अभाव ही है । अतः यह विषयसूची असंगत, शैली - विरूद्ध, तथा सर्वथा अपूर्ण है ।
वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम् ।आपद्धर्मं च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा । ।1/116
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
वैश्य और शूद्रों का धर्म, वर्णसंकरों की उत्पत्ति संकट के समय में वर्णों का धर्म, प्रायश्चित (पाप से मुक्त होने की विधि)।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।१११ से ११८ तक आठ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।११० श्लोक में धर्म का प्रकरण है और १।१२० श्लोक में भी धर्म का वर्णन है । इस धर्मविषय के मध्य में इन प्रक्षिप्त श्लोकों में वर्णित विषय - सूची सर्वथा ही असंगत है । और यह विषयसूची यदि मौलिक होती, तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होनी चाहिये थी अथवा ग्रन्थ के अन्त में । किसी विषय के बीच में विषय - सूची की कोई संगति नहीं है । ये श्लोक मनु की शैली से भी विरूद्ध हैं । मनु प्रत्येक विषय का प्रारम्भ तथा अन्त में निर्देश अवश्य करते हैं, और प्रवचन - शैली में तो यह अत्यावश्यक होता है, परन्तु इन आठ श्लोकों में वण्र्य विषय का संकेत नहीं है । और १।११८ श्लोक में ‘शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मनुः’ कहकर तो प्रक्षेप्ता ने इनके प्रक्षिप्त होने का प्रबल प्रमाण ही दे दिया है । मनु का नाम लेकर किसी और ने ही इन्हें बनाया है और ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी मनु का नहीं है । क्यों कि प्रवचन को जब ग्रन्थरूप में संकलित किया गया, तदनन्तर ही ‘शास्त्र’ शब्द का मनुस्मृति के लिए व्यवहार सम्भव हो सकता है , स्वयं मनु द्वारा नहीं । और इन श्लोकों में जो विषय - सूची दिखाई गई है , उसके अनुसार मनुस्मृति में विषयों का वर्णन भी नही है । जैसे - १।११८ श्लोक में कहे कुलधर्म, व पाखण्डियों के धर्मों का कहीं मनुस्मृति में वर्णन ही नहीं है । और जिस विषय को मनु ने ‘कार्यविनिर्णय’ शब्द से कहा है, उसको इस विषय सूची में पृथक् - पृथक् ‘साक्षिप्रश्नविधान’, ‘स्त्रीपुरूषधर्म’, विभावधर्म आदि नामों से उल्लेख किया है और मनुस्मृति में वर्णित अनेक मुख्य विषयों - (प्रथम अध्याय में धर्मोत्पत्ति, १२वें अध्याय में त्रिविध गतियाँ, धर्मनिश्चयविधि आदि) का इस विषयसूची में अभाव ही है । अतः यह विषयसूची असंगत, शैली - विरूद्ध, तथा सर्वथा अपूर्ण है ।
संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्मसंभवम् ।निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् । ।1/117
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
शुभ और अशुभ कर्मों से उत्तम, मध्यम व अधम शरीर में जन्म पाना, उत्तम ज्ञान अर्थात् आत्मज्ञान से शुभाशुभ कर्मों का फल।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।१११ से ११८ तक आठ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।११० श्लोक में धर्म का प्रकरण है और १।१२० श्लोक में भी धर्म का वर्णन है । इस धर्मविषय के मध्य में इन प्रक्षिप्त श्लोकों में वर्णित विषय - सूची सर्वथा ही असंगत है । और यह विषयसूची यदि मौलिक होती, तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होनी चाहिये थी अथवा ग्रन्थ के अन्त में । किसी विषय के बीच में विषय - सूची की कोई संगति नहीं है । ये श्लोक मनु की शैली से भी विरूद्ध हैं । मनु प्रत्येक विषय का प्रारम्भ तथा अन्त में निर्देश अवश्य करते हैं, और प्रवचन - शैली में तो यह अत्यावश्यक होता है, परन्तु इन आठ श्लोकों में वण्र्य विषय का संकेत नहीं है । और १।११८ श्लोक में ‘शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मनुः’ कहकर तो प्रक्षेप्ता ने इनके प्रक्षिप्त होने का प्रबल प्रमाण ही दे दिया है । मनु का नाम लेकर किसी और ने ही इन्हें बनाया है और ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी मनु का नहीं है । क्यों कि प्रवचन को जब ग्रन्थरूप में संकलित किया गया, तदनन्तर ही ‘शास्त्र’ शब्द का मनुस्मृति के लिए व्यवहार सम्भव हो सकता है , स्वयं मनु द्वारा नहीं । और इन श्लोकों में जो विषय - सूची दिखाई गई है , उसके अनुसार मनुस्मृति में विषयों का वर्णन भी नही है । जैसे - १।११८ श्लोक में कहे कुलधर्म, व पाखण्डियों के धर्मों का कहीं मनुस्मृति में वर्णन ही नहीं है । और जिस विषय को मनु ने ‘कार्यविनिर्णय’ शब्द से कहा है, उसको इस विषय सूची में पृथक् - पृथक् ‘साक्षिप्रश्नविधान’, ‘स्त्रीपुरूषधर्म’, विभावधर्म आदि नामों से उल्लेख किया है और मनुस्मृति में वर्णित अनेक मुख्य विषयों - (प्रथम अध्याय में धर्मोत्पत्ति, १२वें अध्याय में त्रिविध गतियाँ, धर्मनिश्चयविधि आदि) का इस विषयसूची में अभाव ही है । अतः यह विषयसूची असंगत, शैली - विरूद्ध, तथा सर्वथा अपूर्ण है ।
देशधर्माञ् जातिधर्मान्कुलधर्मांश्च शाश्वतान् ।पाषण्डगणधर्मांश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः । ।1/118
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म और पाखण्डी धर्म अर्थात् देश, जाति, कुल और पाखण्डी इन सबों के धर्म, इतनी बातें मनुजी ने इस शास्त्र में कही हैं।
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।१११ से ११८ तक आठ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरूद्ध हैं । १।११० श्लोक में धर्म का प्रकरण है और १।१२० श्लोक में भी धर्म का वर्णन है । इस धर्मविषय के मध्य में इन प्रक्षिप्त श्लोकों में वर्णित विषय - सूची सर्वथा ही असंगत है । और यह विषयसूची यदि मौलिक होती, तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होनी चाहिये थी अथवा ग्रन्थ के अन्त में । किसी विषय के बीच में विषय - सूची की कोई संगति नहीं है । ये श्लोक मनु की शैली से भी विरूद्ध हैं । मनु प्रत्येक विषय का प्रारम्भ तथा अन्त में निर्देश अवश्य करते हैं, और प्रवचन - शैली में तो यह अत्यावश्यक होता है, परन्तु इन आठ श्लोकों में वण्र्य विषय का संकेत नहीं है । और १।११८ श्लोक में ‘शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मनुः’ कहकर तो प्रक्षेप्ता ने इनके प्रक्षिप्त होने का प्रबल प्रमाण ही दे दिया है । मनु का नाम लेकर किसी और ने ही इन्हें बनाया है और ‘शास्त्र’ शब्द का प्रयोग भी मनु का नहीं है । क्यों कि प्रवचन को जब ग्रन्थरूप में संकलित किया गया, तदनन्तर ही ‘शास्त्र’ शब्द का मनुस्मृति के लिए व्यवहार सम्भव हो सकता है , स्वयं मनु द्वारा नहीं । और इन श्लोकों में जो विषय - सूची दिखाई गई है , उसके अनुसार मनुस्मृति में विषयों का वर्णन भी नही है । जैसे - १।११८ श्लोक में कहे कुलधर्म, व पाखण्डियों के धर्मों का कहीं मनुस्मृति में वर्णन ही नहीं है । और जिस विषय को मनु ने ‘कार्यविनिर्णय’ शब्द से कहा है, उसको इस विषय सूची में पृथक् - पृथक् ‘साक्षिप्रश्नविधान’, ‘स्त्रीपुरूषधर्म’, विभावधर्म आदि नामों से उल्लेख किया है और मनुस्मृति में वर्णित अनेक मुख्य विषयों - (प्रथम अध्याय में धर्मोत्पत्ति, १२वें अध्याय में त्रिविध गतियाँ, धर्मनिश्चयविधि आदि) का इस विषयसूची में अभाव ही है । अतः यह विषयसूची असंगत, शैली - विरूद्ध, तथा सर्वथा अपूर्ण है ।
यथेदं उक्तवाञ् शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया ।तथेदं यूयं अप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत । ।1/119
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by : स्वामी दर्शनानंद जी
भृगुजी कहते हैं कि जिस प्रकार हमने इस शास्त्र को मनुजी से पूछा और उन्होंने कहा, उसी तरह आप लोग भी हमसे सुनिये-
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।११९ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है - इस श्लोक में कहा है कि ‘जैसे मनु ने इस शास्त्र को मेरे से कहा, वैसे ही मेरे से तुम सब जानो’ । इससे स्पष्ट है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी दूसरे ने बनाकर मिलाया है । और यह श्लोक भी पूर्वापर - संगति से मेल नहीं खाता । १।११० श्लोक में तथा १।१२० श्लोक में धर्म का वर्णन है, यह श्लोक उस प्रकरण से विरूद्ध है और इस श्लोक में ‘शास्त्र’ अब्द का प्रयोग भी इसे अर्वाचीन सिद्ध कर रहा है । और महर्षियों ने (१।१-४) श्लोकों में मनु जी से धर्म विषयक जिज्ञासा की थी, अतः उत्तर भी मनु जी का ही होना चाहिए । किन्तु इस श्लोक में किसी अन्य भृगु आदि को ही प्रवचन करने वाला माना है, अतः पूर्व श्लोकों में कहे वचनों से यह विरूद्ध है ।


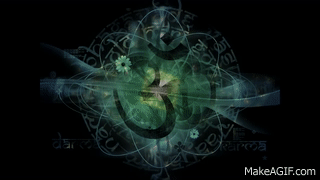




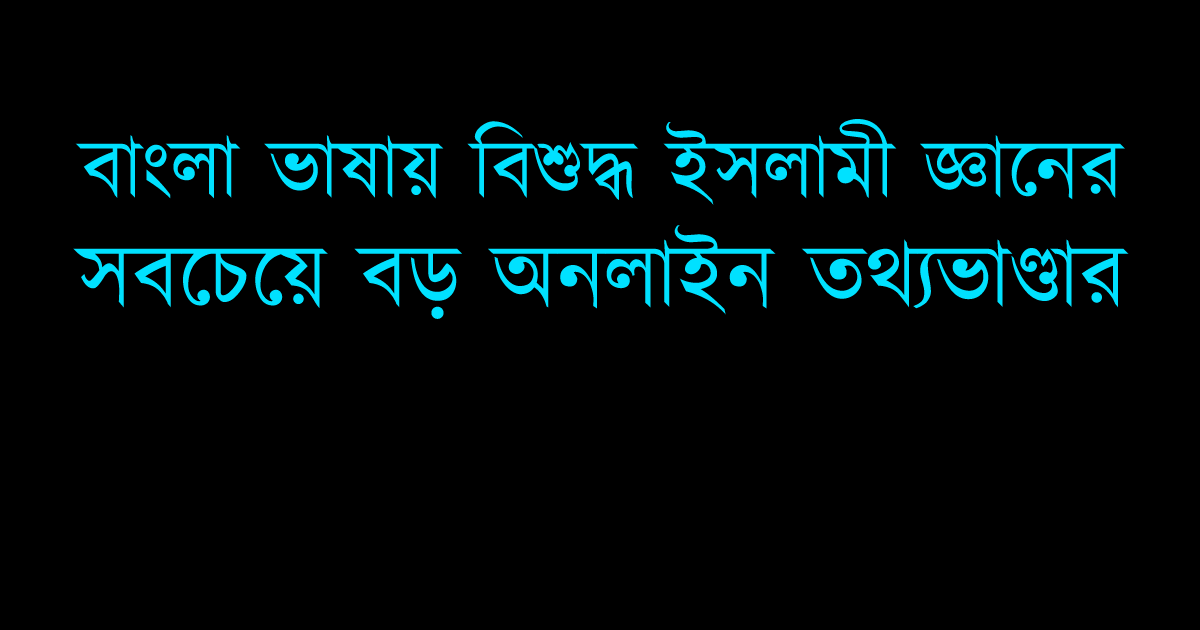

















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ