भूमिका
अपध्नन्तो अराव्ण: पवमाना: स्वर्दृश:।
योनावृतस्य सीदत॥ (ऋ.९.१३.९)
इस मन्त्र का आपने निम्नानुसार भाष्य उद्धृत किया है—
"May you (O love divine), the beholder of the path of enlightenment, purifying our mind and destroying the infidels who refuse to offer worship, come and stay in the prime position of the eternal sacrifice." -Tr. Satya Prakash Saraswati
अर्थात् आप (हे ईश्वरीय प्रेम), आत्मज्ञान के मार्ग के द्रष्टा, हमारे मन को शुद्ध करने वाले और पूजा करने से इनकार करने वाले नास्तिकों को नष्ट करने वाले, आओ और शाश्वत यज्ञ के प्रधान पद पर रहो।"
(अराव्ण:) दुष्टों को (अपध्नन्त:) दारुण दण्ड देने वाला (पवमाना:) सत्कर्मियों को पवित्र करने वाला (स्वर्दृश:) सर्वद्रष्टा परमात्मा (ऋतस्य) सत्कर्मरूपी यज्ञ की (योनौ) वेदी में (सीदत) आकर विराजमान हो ॥ ९॥
यहाँ अंंग्रेजी अनुवाद को स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती का बताया गया है। निश्चित ही यह अनुवाद उचित नहीं है, परन्तु हिन्दी अनुवाद किसका है, यह आपने नहीं दर्शाया है। इसे हम बता रहे हैं कि यह आर्यविद्वान् आचार्य बैद्यनाथ शास्त्री के द्वारा किया हुआ अनुवाद है। इस हिन्दी अनुवाद पर आपको क्या आपत्ति है? अथवा संसार का कोई सभ्य अथवा न्यायप्रिय व्यक्ति इस पर क्या आपत्ति कर सकता है? क्या दुष्ट को दण्ड देना अपराध है? यदि ऐसा है, तो संसार के सभी न्यायालय और पुलिस व्यवस्था व सेना को बन्द वा समाप्त कर देनी चाहिए। मैं इस मन्त्र पर आपके आक्षेप को समझ नहीं पा रहा। क्या आप दुष्ट को पुरस्कृत और सत्कर्म करने वाले को दण्डित वा अपवित्र करना चाहते हैं? जैसाकि संसार में खूनी मजहबों का इतिहास व चरित्र रहा है। यद्यपि यह हिन्दी भाष्य गलत नहीं है, परन्तु यह कथमपि पर्याप्त भी नहीं है। अब हम इस मन्त्र पर अपने ढंग से विचार करते हैं—
इस मन्त्र का ऋषि असित काश्यप देवल है। इसका अर्थ यह है कि यह मन्त्ररूपी छन्द रश्मि कूर्म प्राण राश्मियों से उत्पन्न ऐसी सूक्ष्म प्राण राश्मियों, जो स्वयं किसी के बंधन में नहीं आतीं, परन्तु सूक्ष्म कणों और रश्मियों को अपने साथ बाँधने में समर्थ होती हैं, से होती है। इसका देवता पवमान सोम और छन्द यवमध्या गायत्री है। इस कारण इसके दैवत और छान्दस प्रभाव से इस सृष्टि में विद्यमान सोम पदार्थ श्वेतवर्णीय तेज से युक्त होने लगता है। इसके साथ ही इस सृष्टि में विद्युत् चुम्बकीय बल भी समृद्ध होने लगता है। अब हम इसका तीन प्रकार का भाष्य करते हैं—
आधिदैविक भाष्य १— (पवमाना:, स्वर्दृश:) सूर्य के समान तेजस्वी और शुद्ध सोम पदार्थ (अराव्ण:, अपघ्नन्त:) [अराव्ण:=रा दाने (अदा.) धातोर्वनिप्। नञ्समास:] संयोग-वियोग की प्रक्रिया में बाधा डालने वाले अथवा उस प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ पदार्थों को नष्ट करता अथवा उन्हें हटाता हुआ (ऋतस्य, योनौ, सीदत) [ऋतम्=ऋतमित्येष (सूर्य:) वै सत्यम् (ऐ.४.२०), ऋतमेवपरमेष्ठी (तै.ब्रा.१.५.५.१), अग्निर्वा ऋतम् (तै.ब्रा.२.१.११.१)] सूर्यलोक के सर्वोत्तम आग्नेय क्षेत्र अर्थात् केन्द्रीय भाग अथवा सम्पूर्ण सूर्यलोक के उत्पत्ति और निवासस्थान में विद्यमाने रहता है।
भावार्थ— सूर्यलोक की उत्पत्ति होने से पहले विशाल खगोलीय मेघों के अन्दर सोम रश्मियाँ शुद्ध रूप में व्याप्त होती हैं। जब वे सोम रश्मियाँ तप्त होने लगती हैं, तब वे ऐसे पदार्थ जो, स्वयं सूर्यलोक के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संयोग-वियोग आदि प्रक्रियाओं में भाग लेने योग्य नहीं होते हैं अथवा जो संयोग-वियोग प्रक्रियाओं में बाधा डाल रहे होते हैं, उन्हें नष्ट वा दूर करती हैं। ऐसा करते हुए वे सोम रश्मियाँ सम्पूर्ण खगोलीय मेघ में व्याप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार सोम प्रधान विद्युत् ऋणावेशित कण भी सम्पूर्ण खगोलीय मेघ और कालान्तर में सूर्यलोक में व्याप्त हो जाते हैं।
आधिदैविक भाष्य २— (पवमाना:, स्वर्दृश:) विद्युत् के समान गत्यादि व्यवहार करने वाले अर्थात् विद्युत् की भाँति शुद्ध मार्गों पर गमन करते हुए सूक्ष्म कण वा विकिरण (अपघ्रन्त:, अराव्ण:) मार्ग में आने वाले ऐसे कण, जो संयोग-वियोग क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं अथवा बाधा डालते हैं, को दूर हटाते हुए चलते हैं। (ऋतस्य, योनौ, सीदत) [ऋतम्= अग्निर्वा ऋतम् (तै.ब्रा. २.१.११.१)] वे कण अग्नि के कारणरूप प्राण तत्त्व में निरन्तर निवास करते हैं अर्थात् वे प्राणों में ही निवास और प्राणों में ही प्राणों के द्वारा गमन करते हैं।
भावार्थ— इस ब्रह्माण्ड में जो कण लगभग प्रकाश के वेग से गमन करते हैं, वे कण अथवा विकिरण मार्ग में बाधक पदार्थों को परे हटाते हुए अपने मार्ग को निर्बाध बनाते हुए चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे विभिन्न आयन्स वा इलेक्ट्रॉन्स को दूर नहीं हटाते, बल्कि उनके द्वारा उत्सर्जन और अवशोषण की क्रियाएँ करते हुए निरापद रूप से निरन्तर गमन करते रहते हैं। इन क्रियाओं के कारण उनकी वास्तविक शुद्ध गति में कुछ न्यूनता भी आती है। यदि अवशोषण व उत्सर्जक पदार्थ अधिक मात्रा में विद्यमान हो, तो उसी अनुपात में गमन करने वाले कणों की परिणामी गति कम होती चली जाएगी। वर्तमान विज्ञान द्वारा परिभाषित डार्क मैटर इन सूक्ष्म कणों वा विकिरणों के साथ कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करता, इसलिए उस पदार्थ को वे कण वा विकिरण दूर हटाते हुए निर्बाध गमन करते रहते हैं। ये कण वा विकिरण सूर्यादि तारों, अन्य आकाशीय लोकों, प्राणियों केे शरीरों वा वनस्पतियों अथवा खुले अन्तरिक्ष में सर्वत्र यही व्यवहार दर्शाते हैं।
ध्यातव्य— हमने यहाँ दो प्रकार के आधिदैविक भाष्य प्रस्तुत किये हैं, इसी प्रकार ‘पवमान स्वर्दृक्’ पदों से तारे, ग्रहादि लोकों का अर्थ ग्रहण करके अन्य भाष्य भी किये जा सकते हैं।क्रमशः...
सभी वेदभक्तों से निवेदन है कि वेदों पर किये गए आक्षेपों के उत्तर की इस शृंखला को आधिकाधिक प्रचारित करने का कष्ट करें‚ जिससे वेदविरोधियों तक उत्तर पहुँच सके और वेदभक्तों में स्वाभिमान जाग सके।
वेदभाष्य का अधिकारी कौन ?
अपध्नन्तो अराव्ण: पवमाना: स्वर्दृश:।
योनावृतस्य सीदत॥ (ऋ.९.१३.९)
आधिभौतिक भाष्य १— (पवमाना:, स्वर्दृश:) सूर्य के समान तेजस्वी वेदवित् पवित्रात्मा व पुरुषार्थी राजा (अपघ्नन्त:, अराव्ण:) ऐसे नागरिक, जो धनवान् होने पर भी राष्ट्रहित में न्यायकारी राजा द्वारा लिये जाने वाले कर का भुगतान न करते हों अथवा कर चोरी करते हैं अथवा आवश्यक होने पर किसी निर्धन का अथवा परोपकार के कार्य में आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं अथवा समाज और राष्ट्र के हितों के विरोधी वा उदासीन होते हैं, उन्हें राजा उचित दण्ड देता हुआ (ऋतस्य, योनौ, सीदत) [ऋतम् = ब्रह्म वाऽऋतम् (श.४.१.४.१०), सत्यं विज्ञानम् (म.द.ऋ.भा.१.७१.२)] समस्त ज्ञान-विज्ञान के मूल वेद के कारण रूप परब्रह्म परमात्मा में निवास करता है।
भावार्थ— किसी भी राष्ट्र का राजा शरीर, मन और आत्मा से पूर्ण स्वस्थ और बलवान् होना चाहिए। ऐसा राजा ही सतत पुरुषार्थ करने वाला हो सकता है। शरीर, मन वा आत्मा में से किसी के निर्बल वा रोगी होने पर कोई भी राजा राष्ट्र के संचालन में समर्थ नहीं हो सकता। इसके साथ ही जब तक राजा ज्ञान-विज्ञान से पूर्णत: सम्पन्न नहीं हो, तब तक भी राजा राष्ट्र का उचित संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे राजा को उसके चाटुकार, चालाक-स्वार्थी मन्त्री, प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, पूँजीपति एवं दूूसरे देशों के राजा भ्रमित करके अपना प्रयोजन सिद्ध करते रह सकते हैं। ऐसा राजा दण्डनीय और सम्माननीय पात्रों का विवेक नहीं रख सकता, जबकि विद्वान् और योगी राजा इसकी पहचान करके दण्डनीयों को दण्ड और सम्माननीयों को सम्मान देकर सम्पूर्ण राष्ट्र का हित सम्पादन करता है। जिस राष्ट्र में दण्डनीयों को दण्ड और सम्माननीयों को सम्मान तथा सत्य व उन्नति के मार्ग पर बढऩे वालों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, वह राष्ट्र अराजकता, हिंसा, भय, अशान्ति, अन्याय और तीनों प्रकार के दु:खों से ग्रस्त होता हुआ विनाश को प्राप्त होता है। अपराधी को दण्ड के विषय में भगवान् मनु का कथन है—
दण्ड: शास्ति प्रजा: सर्वा:, दण्ड एवाभिरक्षति।
दण्ड: सुप्तेषु जागर्ति, दण्डं धर्मं विदुर्बुधा:॥ (मनु.)
अर्थात् उचित दण्ड ही प्रजा पर शासन करता है और दण्ड ही प्रजा की रक्षा करता है। दण्ड कभी शिथिल नहीं होता, इसलिए विद्वान् लोग दण्ड को ही धर्म कहते हैं।
कंजूस को दण्ड देने के विषय में महात्मा विदुर ने कहा है—
द्वावम्भसी निवेष्टव्यौ, गले बद्ध्वा दृढां शिलाम्।
धनवन्तमदातारं, दरिद्रं चातपस्विनम्॥ (विदुरनीति.१.६५)
अर्थात् धनवान् होते हुए भी परोपकार के कार्यों में दान न देने वाले और निर्धन होते हुए भी परिश्रम न करने तथा दु:ख सहना न चाहने वाले को गले में भारी पत्थर बाँधकर गहरे जलाशय में डुबो देना चाहिए। यहाँ सम्पूर्ण प्रजा के लिए भी सन्देश है कि धनी व्यक्ति धन को ईश्वर का प्रसाद समझकर त्यागपूर्वक ही उपयोग करे। वह निर्धन व दुर्बल की अवश्य सहायता करे। उधर निर्धन व्यक्ति धनी से ईष्र्या कदापि न करे, बल्कि स्वयं धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करता रहे और दु:खों को भी सहन करने का अभ्यास करे। वह किसी के धन की चोरी करके धनी होने का प्रयास न करे अथवा बिना कर्म और योग्यता के धन, पद वा ऐश्वर्य पाने की इच्छा कभी नहीं करे।
आधिभौतिक भाष्य २— (पवमाना:, स्वर्दृश:) वेदविद्या के प्रकाश से प्रकाशमान ब्रह्मतेज से सम्पन्न पवित्रात्मा योगी आचार्य वा आचार्या अपने विद्यार्थियों को विद्याभ्यास कराते हुए (अपघ्नन्त:, अराव्ण:) विद्या को ग्रहण करने की इच्छा न करने वाले अथवा ग्रहण न करने वाले शिष्य और शिष्याओं की आवश्यक एवं उचित ताडऩा भी करें। (ऋतस्य, योनौ, सीदत) ऐसे आचार्य और आचार्या सम्पूर्ण सत्य विद्या के मूल कारण वेद अथवा परमात्मा में निरन्तर विराजमान रहते हैं।
भावार्थ— वेद ज्ञान से सम्पन्न निरन्तर योगनिष्ठ विद्वान् वा विदुषी को ही आचार्य वा आचार्या बनने का अधिकार होना चाहिए। उनको चाहिए कि वे अपने शिष्य वा शिष्याओं का प्रीतिपूर्वक और निष्कपट भाव से अध्यापन करें। जो विद्यार्थी विद्याग्रहण में प्रमाद करें और प्रीतिपूर्वक समझाने से भी न समझें, उन्हें समुचित दण्ड अवश्य दें। इस विषय में ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ-प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण देते हुए लिखा है—
सामृतैै: पाणिभिघ्र्नन्ति गुरवो न विषोक्षितै:।
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणा:॥
अर्थात् जो माता, पिता और आचाय्र्य, सन्तान और शिष्यों का ताडऩ करते हैं, वे जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाडऩ करते हैं, वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि लाडऩ से सन्तान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताडऩा से गुणयुक्त होते हैं और सन्तान और शिष्य लोग भी ताडऩा से प्रसन्न और लाडऩ से अप्रसन्न सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईष्र्या, द्वेष से ताडऩ न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रक्खें।
ध्यातव्य— इसी प्रकार माता-पिता आदि का ग्रहण करके भी अन्य प्रकार के आधिभौतिक भाष्य भी किये जा सकते हैं।
आध्यात्मिक भाष्य— (पवमाना:, स्वर्दृश:) यम-नियमों से पवित्र हुआ योगी ब्रह्म का साक्षात् करने वाला (अपघ्नन्त:, अराव्ण:) सभी प्रकार के दोषों का परित्याग न कर पाने की अनिष्ट चित्तवृत्तियों को दूर करता है अर्थात् वह योगी पुरुष सभी प्रकार की अनिष्ट वृत्तियों को शनै:-शनै: निरुद्ध करता चला जाता है। जब उसकी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं, तब (ऋतस्य, योनौ, सीदत) वह योगी पुरुष सब सत्य विद्याओं केमूल परब्रह्म परमात्मा में विराजमान हो जाता है अर्थात् वह ब्रह्मसाक्षात्कार कर लेता है।
भावार्थ— जब कोई योगाभ्यासी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे यमों एवं शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान जैसे नियमों से स्वयं को पवित्र बना लेता है, तब उसकी चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध होने लगती हैं, जिससे वह ब्रह्मसाक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है।
यहाँ यह स्पष्ट होता है कि बिना यम-नियमों के पालन किये कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता।
आक्षेप–१ का समाधान समाप्त----------------------------------- 6...तो क्या दुष्ट की पूजा करें!
आक्षेप संख्या—२
यहाँ सुलेमान रजवी ने ऋग्वेद ७.६.३ के दो भाष्य निम्र प्रकार उद्धृत किये हैं— Rig Veda 7.6.3 “May the fire divine chase away those infidels, who do not perform worship and who are uncivil in speech. They are niggards, unbelievers, say no tribute to fire divine and offer no homage. The fire divine turns those godless people far away who institute no sacred ceremonies.” –Tr. Satya Prakash Saraswati पदार्थ — हे राजन् (अग्नि:) अग्नि के तुल्य तेजोमय! आप (अक्रतून) निर्बुद्धि (ग्रथिन:) अज्ञान से बंधे (मृध्रवाच:) हिंसक वाणी वाले (अयज्ञान्) सङ्गादि वा अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान से रहित (अश्रद्धान्) श्रद्धारहित (अवृधान्) हानि करने हारे (तान्) उन (दस्यून्) दुष्ट साहसी चोरों को (प्रप्र, विवाय) अच्छे प्रकार दूर पहुँचाइये (पूर्व:) प्रथम से प्रवृत्त हुए आप (अपरान्) अन्य (अयज्यून्) विद्वानों के सत्कार के विरोधियों को (पणीन्) व्यवहार वाले (निश्चकार) निरन्तर करते हैं। भावार्थ — इस मन्त्र में वाचकलु०— हे विद्वानो! तुम लोग सत्य के उपदेश और शिक्षा से सब अविद्वानों को बोधित करो, जिससे ये अन्यों को भी विद्वान् करें। पदार्थ — (नि) (अक्रतून्) निर्बुद्धीन् (ग्रथिन:) अज्ञानेन बद्धान् (मृध्रवाच:) मृध्रा हिंस्रा अनृता वाग्येषान्ते (पणीन्) व्यवहारिण: (अश्रद्धान्) श्रद्धारहितान् (अवृधान्) अवर्धकान् हानिकरान् (अयज्ञान्) सङ्गाद्यग्निहोत्राद्यनुष्ठानरहितान् (प्रप्र) (तान्) (दस्यून्) दुष्टान् साहसिकाँश्चोरान् (अग्नि:) अग्निरिव राजा (विवाय) दूरं गमयति (पूर्व:) आदिम: (चकार) करोति (अपरान्) अन्यान् (अयज्यून्) विद्वत्सत्कारविरोधिन:। भावार्थ — अत्र वाचकलु०— हे विद्वांसो यूयं सत्योपदेशशिक्षाभ्यां सर्वानविदुषो बोधयन्तु यत एतेऽपरानपि विदुष: कुर्य्यु:। यहाँ आक्षेपकर्त्ता ने अपने शब्दों में इन भाष्यों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, परन्तु स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती के अंग्रेजी अनुवाद के कुछ वाक्यों को रेखांकित अवश्य किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस पर आक्षेपकर्त्ता के वही आक्षेप हैं, जो आक्षेप क्रमांक १ में दर्शाए गए हैं। जो भी पाठक हमारे आक्षेप क्रमांक १ के उत्तर को समझ लेंगे, उन्हें इस आक्षेप का भी उत्तर स्वयं मिल जाएगा। निश्चित ही स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती का अंग्रेजी अनुवाद न तो उचित है, न पर्याप्त है और न स्पष्ट ही। स्वामी जी की समस्या यह भी हो सकती है कि अंग्रेजी भाषा में हिन्दी वा संस्कृत भाषा के गम्भीर भावों के समान कोई शब्द ही नहीं है। इस कारण से वेदादि शास्त्रों का किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना, विशेषकर अंग्रेजी आदि निर्धन भाषाओं में अनुचित और संकटपूर्ण है। स्वामी जी को चाहिए था कि वे अंग्रेजी भाषा में ऋषि दयानन्द के भाष्य की व्याख्या करते। जहाँ उपयुक्त शब्द नहीं मिलते हैं, वहाँ और भी अधिक स्पष्ट व्याख्या की आवश्यकता होती है। दूसरा भाष्य आक्षेपकर्त्ता ने ऋषि दयानन्द का दिया है, जिस पर कोई भी आक्षेप नहीं किया गया है और हमें यही लगता कि ऋषि दयानन्द के इस भाष्य पर कोई भी बुद्धिमान् मानवतावादी असहमत हो सकता है। अब हम इस मन्त्र पर विचार करते हैं। वह मन्त्र इस प्रकार है— न्यक्रतून्ग्रथिनो मृध्रवाच: पणीँरश्रद्धाँ अवृधाँ अयज्ञान्। प्रप्रतान्दस्यूँरग्निर्विवाय पूर्वश्चकारापराँ अयज्यून्॥ [ऋ.७.६.३] आधिदैविक भाष्य– यह पाठकों के लिए पुस्तक रूप में ही भविष्य में उपलब्ध हो सकेगा। आधिभौतिक भाष्य— यह भाष्य आपने उद्धृत किया ही है और इस पर आपकी कोई टिप्पणी भी नहीं है। अविद्याग्रस्त अर्थात् मूढ़ मति, हिंसा के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले, समाज में विघटन पैदा करने वाले, अग्निहोत्रादि से पर्यावरण को शुद्ध न करने वाले, विद्या एवं मानवता पर श्रद्धा न रखने वाले, हानिकारक दुष्ट अपराधियों को राजा यदि दूर नहीं करेगा, उन्हें सन्मार्ग पर नहीं लाएगा, तो क्या उनकी पूजा करेगा, उनको दूर करने से ही किसी भी राष्ट्र वा समाज का हित हो सकता है, अन्यथा राष्ट्र और विश्व में अराजकता ही फैलेगी। इसलिए ऋषि दयानन्द का भाष्य सर्वथा उचित और कल्याणकारी है। आध्यात्मिक भाष्य— (अग्नि:) शरीरस्थ विद्युदग्नि (अक्रतून्) [क्रतु:=कर्मनाम (निघं.२.१), प्रज्ञानाम (निघं.३.९)] जो कोशिका आदि पदार्थ निष्क्रिय वा मृत हो जाते हैं, (ग्रथिन:) जो पदार्थ विकृत वा अनिष्ट बन्धनों से युक्त होते हैं (मृध्रवाच:) [वाक्= वागेवाऽग्नि: (श.३.२.२.१३)] अनिष्टकारी अग्नि अर्थात् जिस विकृत अग्नि के द्वारा शरीर में नाना रोग हो सकते हैं (अयज्ञान्) ऐसे अवशिष्ट पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते (अश्रद्धान्) [श्रद्धा = तेज एवं श्रद्धा (श.११.३.१.१)] जो पदार्थ तेजहीन वा दुर्बल हो चुके हैं (अवृधान्) जो पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक हैं अर्थात् विजातीय पदार्थ (तान्, दस्यून्) वे ऐसे सभी पदार्थ शरीर को क्षीण करने वाले होते हैं, उन सभी हानिकारक पदार्थों को (प्र, प्र, विवाय) बहिर्गत अथवा नष्ट करता रहता है। ऐसे सभी पदार्थ ही अवशिष्ट रूप होकर मल-मूत्र, स्वेद, कफ, श्वास आदि के द्वारा निरन्तर नि:सृत होते रहते हैं। (पूर्व:) इन सब पदार्थों की उत्पत्ति से पूर्व से विद्यमान वह शरीरस्थ अग्नि (अपरान्) अन्य पदार्थों को (अयज्यून्) जो पदार्थ सप्तधातुओं में परिणत नहीं हो रहे, उनको (पणीन्, नि, चकार) सम्यक् क्रियाओं और बलों से निरन्तर युक्त करता रहता है। भावार्थ— शरीर में रहने वाले विद्युत् एवं अग्नि पदार्थ शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करने में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। विद्युत् और ऊष्मा के कारण ही शरीर में अनेक छेदन और भेदन की क्रियाएँ चलती रहती हैं। भोजन के अवयवों का सूक्ष्म भागों में टूटना, पाचक रसों का निकलना, उनसे नाना प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का होना, रसरूप हुए भोजन का आँतों के द्वारा अवशोषित होना, फुफ्फुस, हृदय और मस्तिष्क के साथ-साथ सभी नाडिय़ों और नसों का क्रियाशील होना, उत्सर्जन आदि सभी तन्त्रों का कार्य करना, बाहर से आए जीवाणुओं और विषाणुओं को रक्त के श्वेत अणुओं द्वारा नष्ट किया जाना, शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा की उत्पत्ति होना ये सभी कार्य विद्युत् और ऊष्मा के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। जिन-जिन मन्त्रों में भी आपने हिंसा के आरोप लगाये हैं, उन-उन मन्त्रों का इसी प्रकार उत्तर समझना चाहिए। हिंसक, चोर, डाकू, ज्ञान के शत्रु, ज्ञानी व परोपकारियों को दु:ख देने वाले, कंजूस, सामर्थ्य होने पर भी परोपकार न करने वाले, आतंकवादी एवं निर्बलों को सताने वाले जैसे लोगों को दण्ड देना ङ्क्षहसा नहीं, बल्कि सच्ची अहिंसा है, जिससे सभी प्राणी सुखी रह सकें। इस कारण हम हिंसा आदि दोषों से आरोपित अन्य मन्त्रों पर कोई भी उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते।
विशेष वक्तव्य हम यहाँ वेद के कुछ उन मन्त्रों को उद्धृत करते हैं, जिनमें केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु प्राणिमात्र के प्रति अत्यन्त प्रेम और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार की बात की गई है।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। (यजु.36.18) अर्थात् प्राणिमात्र के प्रति मित्र के समान व्यवहार करें।
समानी प्रपा सह वोऽन्नभाग:। (अथर्व.3.30.6) अर्थात् हम सब मनुष्यों के खान-पान समान होवें।
यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्। (यजु.32.8) अर्थात् हम सब पृथिवीवासी परस्पर इस प्रकार रहें, जैसे घोंसले में पक्षी का परिवार परस्पर प्रेम से रहता है।
समानो मन्त्र: समिति: समानी समानं मन: सह चित्तमेषाम्। (ऋ.10.191.3) अर्थात् हम सब मनुष्यों के विचार, हमारी सामाजिक परम्पराएँ, हमारे चित्त और भावनाएँ सब समान होवें।
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास:। (ऋ.5.60.5) अर्थात् हम मनुष्यों में कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है अर्थात् सभी एक पिता परमात्मा की सन्तान हैं।
इस प्रकार के उदात्त उपदेशों के रहते कोई अज्ञानी व्यक्ति ही वेदों में हिंसा, छुआछूत, ऊँच-नीच, शोषण जैसे पापों का आरोप लगा सकता है। बुद्धिमान् तो कभी इस प्रकार का विचार मन में भी नहीं ला सकता। इस कारण इस प्रकरण को हम यहाँ समाप्त करते हैं। वैदिक ईश्वर को न मानने वाला दोषी क्यों?
सुलेमान रजवी के आरोपों में अनेक मन्त्रों पर यह आरोप है कि उसमें नास्तिकों को दण्ड देने का प्रावधान है। सर्वप्रथम तो हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि सत्यप्रकाश सरस्वती के अनुवाद अथवा अन्य जिसने भी अनुवाद किये हैं, वे वेद के वास्तविक एवं सम्पूर्ण आशय को व्यक्त करने में नितान्त असमर्थ हैं। वेद का भाष्य करने की शैली वही होनी चाहिए, जो हमने दो मन्त्रों का भाष्य करके पूर्व में दर्शायी है। वेद का मूल अर्थ तो आधिदैविक ही होता है, अन्य दोनों प्रकार के अर्थ मूल अर्थ के साथ कहीं न कहीं संगत रहते हैं। मूल अर्थ सार्वदेशिक व शाश्वत होता है, जबकि आधिभौतिक अर्थ भिन्न-भिन्न लोकों के मननशील प्राणियों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकता है, परन्तु आध्यात्मिक अर्थ भी शाश्वत और सार्वदेशिक होता है। सारांशत: वेद का आधिदैविक भाष्य किये बिना अथवा उसे जाने बिना अन्य दोनों प्रकार के भाष्य संदिग्ध ही रहते हैं। ऋषि दयानन्द ने समयाभाव के कारण आधिदैविक भाष्य बहुत कम मन्त्रों के किये हैं। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय, सामाजिक और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए मनुष्यों को आध्यात्मिक बनाने के साथ-साथ लौकिक व्यवहार में भी कुशल और सर्वहितैषी बनाने की भावना से प्राय: आधिभौतिक और आध्यात्मिक अर्थ ही किये हैंं। उन्होंने केवल संस्कृत भाषा में ही अपने भाष्य किये हैं, हिन्दी भाषा उनके सहयोगी पण्डितों ने बनायी है। इस कारण उस हिन्दी भाषा में अनेकत्र त्रुटियाँ भी रह गयी हैं। कहीं त्रुटियाँ अनजाने में हुई हैं, तो कहीं जानबूझकर भी की हुई प्रतीत होती हैं।
वेद के अन्य आर्यसमाजी भाष्यकारों ने ऋषि दयानन्द की शैली का यथाशक्ति अनुसरण करने का प्रयास किया है, परन्तु जहाँ वे ऐसा नहीं कर सके, वहाँ वे आचार्य सायण आदि का अनुसरण करने को ही विवश हुए हैं। इस कारण अनेकत्र भारी दोष आ गये हैं। यह सब कहने का अर्थ यह भी नहीं है कि कोई भी अनाड़ी व्यक्ति वेद पर आक्रमण करने का अधिकारी हो गया। कमजोर काँच के महल में रहने वाले पत्थरों के बने महलों में रहने वालों पर पत्थर फेंकने का दुस्साहस करें, यह हास्यास्पद ही है। इतने पर भी हम इनके इन आक्षेपों के विषय में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहते हैं, उनमें प्रथम यह है कि नास्तिक किसे कहते हैं? भगवान् मनु के अनुसार— ‘नास्तिको वेदनिन्दक:’ अर्थात् जो वेद की निन्दा करता है, ज्ञान-विज्ञान की निन्दा करता है, ज्ञानियों का शत्रु है, ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करता है, लोगों को अन्धविश्वासी बनाता है, विद्या का विरोधी बनाता है, जो स्वयं सत्य से दूर रहता और दूसरों को सत्य से दूर करने का प्रयास करता है, उसे नास्तिक कहते हैं। वेद सत्यासत्य के विचार बिना किसी बात को बलात् स्वीकार करने का उपदेश नहींं करता, बल्कि वह सत्य और असत्य को जानकर ही सम्पूर्ण लोकव्यवहार करने का उपदेश करता है। प्राणिमात्र के प्रति मैत्री करने और दुष्टों को दण्ड देने का उपदेश करता है। सम्पूर्ण सृष्टि के वैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन करता है। वेद कोई साम्प्रदायिक अथवा किसी वर्ग व देश का ग्रन्थ नहीं है, बल्कि यह ब्रह्माण्डीय ग्रन्थ है। इसका विरोध करने का अर्थ यह है कि विरोध करने वाला व्यक्ति सम्पूर्ण सृष्टि के ज्ञान-विज्ञान का विरोधी है। अब कोई भी बुद्धिमान् व्यक्ति विचार करे कि ऐसे महान् ज्ञान-विज्ञान के ग्रन्थ वेद का विरोध करने वाला मानवता का हितैषी होगा वा शत्रु होगा। निश्चित ही वह मानवता का प्रबल शत्रु होगा। तब मानवता के प्रबल शत्रु को दण्ड क्यों नहीं देना चाहिए? इसी प्रकार हम ईश्वर का विरोध करने के आक्षेप पर भी विचार करते हैं।
वेदोक्त ईश्वर विभिन्न सम्प्रदायों में वर्णित कल्पित ईश्वर नहीं है, वह सातवें आसमान अथवा चौथे आसमान पर तख्त पर बैठा हुआ ईश्वर नहीं है, जिसे उठाने केे लिए फरिश्तों की आवश्यकता पड़े। वह मनुष्य और मनुष्य केे बीच फूट डालने व हिंसा कराने वाला ईश्वर नहींं है। वह अपने-अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अकारण ही गुमराह करने वा राह बताने वाला ईश्वर नहीं है। वह अपनी ही सन्तानरूप पशु-पक्षियों को मारकर खाने का उपदेश करने वाला ईश्वर नहीं है। वह सृष्टि के विषय में नितान्त काल्पनिक एवं हास्यास्पद कहानियाँ सुनाने वाला ईश्वर नहींं है। वह कैलाश पर्वत, क्षीर सागर आदि में रहने वाला शरीरधारी भी ईश्वर नहीं है, बल्कि वेदोक्त ईश्वर ऐसी सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमती, सर्वकल्याणकारिणी एवं निराकार चेतना का नाम है, जो सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पदार्थों में पूर्णतया व्याप्त है, जो जीवमात्र का कल्याण करने के लिए ही सृष्टि की रचना करता है और ऐसा ही सब मनुष्यों को उपदेश करता है। उस ऐसे सर्वोच्च सामर्थ्यवान् ईश्वर की पूजा का अर्थ यह नहीं है कि उसे मन्दिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया जाये, न ही यह है कि मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में जाकर नाना प्रकार के कर्मकाण्ड किये जायें, बल्कि ईश्वर पूजा का अर्थ है कि यम-नियमों का पालन करते हुए अर्थात् पूर्ण सत्यवादी, जीवमात्र से प्रेम करने वाले, अपनी इन्द्रियों को वश में करने वाले एवं सृष्टि का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने वाले होकर निरन्तर परोपकार करने का प्रयत्न किया जाये और ऐसा करते हुए ही ध्यान, उपासना आदि किया जाता है। जब तक ऐसा नहीं होता अथवा जो ऐसा करने का प्रयास नहीं करता, उसे ईश्वर की पूजा करने वाला नहीं मानना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही दुष्ट और अधार्मिक होता है। आज ऐसे ही व्यक्तियों की संख्या संसार में बहुत अधिक है, इसलिए सारा संसार दु:खी है। पूजा-नमाज और प्रार्थना के आडम्बर बहुत हो रहे हैं, कल्पित ईश्वरों पर भाषण बहुत दिये जा रहे हैं, परन्तु सत्य से इन लोगों ने सम्बन्ध तोड़ दिया है। क्या ऐसे लोग दण्डनीय नहीं होने चाहिए?
वस्तुत: ईश्वर, पूजा एवं वेद इन तीनों के सत्य स्वरूप को न समझने के कारण ही आप वेद के विषय में नितान्त भ्रान्त हैं अथवा अपनी कुरान में वर्णित हिंसादि पापों को सही ठहराने के लिए ही दुर्भावनावश वेद पर भी ऐसे आरोप लगा रहे हैं। एक ओर तो भाष्यकारों और अनुवादकों का दोष, दूसरी ओर पूर्वाग्रह और दुर्भावनावश इन भाष्यों और अनुवादों को पढ़ने वालों का दोष, इस प्रकार कोढ़ में ही खाज हो गयी है। यदि कोई वास्तव में सत्य का जिज्ञासु है, तब वह हमारे इन दो भाष्यों को पढक़र ही वास्तविकता को जान जायेगा और वेद का अनुयायी हो जायेगा, परन्तु बुद्धिहीन और पूर्वाग्रही व्यक्ति के लिए कोई औषधि संसार में नहीं है।
आक्षेप संख्या—३
Atharva Veda 5.21.3 ‘Let this war drum made of wood, muffled with leather straps, dear to all the persons of human race and bedewed with ghee, speak terror to our foemen.” Tr. Vaidyanath Shastri
वानस्पत्य: संभृत उस्रियाभिर्विश्वगोत्र्य:।
प्रत्रासममित्रेभ्यो वदाज्येनाभिघारित:॥
भाष्य— हे दुन्दुभे! नक्कारे! तू जिस प्रकार (वानस्पत्य:) लकड़ी का बना हुआ होकर भी (उस्रियाभि: संभृत:) चाम के तस्मों से जकड़ा हुआ (विश्वगोत्र्य:) समस्त जन का बन्धु है। वह (अमित्रेभ्य:) शत्रुओं के लिये। (आज्येन अभि-घारित:) घृत द्वारा अभिषिक्त होकर (प्रत्रासं वद) भय और आतंक बतला।
आक्षेप का उत्तर—
यह मन्त्र इस प्रकार है—
वानस्पत्य: संभृत उस्रियाभिर्विश्वगोत्र्य:।
प्रत्रासममित्रेभ्यो वदाज्येनाभिघारित:॥ (अथर्व.५.२१.३)
इस मन्त्र से उपर्युक्त भाष्यकारों ने शत्रुओं को आतंकित करने का वर्णन किया है। यद्यपि यह भाष्य नहीं है, अपितु मात्र सरल अनुवाद है, जो मन्त्र के अभिप्राय को उचित रीति से दर्शाने में सक्षम नहीं है। हम पूर्ववत् यहाँ फिर कहना चाहेंगे कि वेद का अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समुचित भाष्य किया जाना चाहिए। पुनरपि इसमें आपको क्या आपत्ति प्रतीत होती है? जब दो सेनाओं में युद्ध होता है, तब शत्रु को आतंकित करने की बात तो क्या, उसे तो नष्ट ही किया जाता है। इसी का नाम युद्ध है, जो धर्मात्माओं और पापियों के बीच सदा से चलता आया है। यहाँ महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि किसे अपना शत्रु मानना चाहिए?
महर्षि दयानन्द ने स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में मनुष्यत्व का लक्षण बताते हुए लिखा है—
मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्यों के सुख-दु:ख और हानि-लाभ को समझे। अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं— कि चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुणरहित क्यों न हों— उनकी रक्षा उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान् और गुणवान् भी हो, तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहाँ तक हो सके, वहाँ तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दु:ख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म से पृथक् कभी न होवें।
अब कोई बताये कि मनुष्य की इससे अधिक न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं कल्याणकारिणी परिभाषा और क्या हो सकती है? जो व्यक्ति अपने बल के अहंकार में जनसाधारण अथवा विभिन्न पशु-पक्षियों को दु:ख देता है, उसको कोई भी सज्जन व्यक्ति अपना शत्रु क्यों न समझे? ऐसे दुष्ट व्यक्ति ही सम्पूर्ण विश्व में अराजकता फैलाते हैं। इनको जितना अधिक सहन किया जायेगा अथवा इनके प्रति जितना अधिक तटस्थ रहा जायेगा, उतनी ही अधिक इस समाज, राष्ट्र वा विश्व में हिंसा, अराजकता और अशान्ति फैलेगी। इस कारण ऐसे बर्बर लोगों को शान्ति और मानवता की स्थापना करने के लिए अवश्य ही नष्ट कर देना चाहिए। तब यदि ऐसे शत्रुओं को दण्ड देने की प्रार्थना वेद में हो, तो उसकी निन्दा कोई अराजक और उपद्रवी तत्त्व ही कर सकता है। अब हम इस मन्त्र का अपना अर्थ प्रस्तुत करते हैं।
इसका भाष्य इस प्रकार है—
आधिदैविक भाष्य— यह पाठकों के लिए पुस्तक रूप में ही भविष्य में उपलब्ध हो सकेगा।
आधिभौतिक भाष्य— (वानस्पत्य:) [वनम् = रश्मिनाम (निघं.१.५), यह पद ‘वन शब्दे’, ‘वन संभक्तौ’ एवं ‘वनु याचने’ धातुओं से व्युत्पन्न है। वनस्पतिरेव वानस्पत्य:] प्रजा द्वारा वाञ्छित अन्न-धनादि पदार्थों का राष्ट्र में समुचित वितरण करने वाला, विद्या के प्रकाश से प्रकाशित सत्योपदेष्टा राजा (विश्वगोत्र्य:) राष्ट्र की प्रजा के सभी कुलों में अपने हितकारी कार्यों द्वारा सदैव विद्यमान अर्थात् समस्त प्रजा का हितचिन्तक (उस्रियाभि:, संभृत:) गौ आदि उपकारी पशुओं के द्वारा तथा नाना प्रकार की निरापद किरणों वा ऊर्जा के द्वारा राष्ट्र को सम्यक् रूप से धारण करने वाला (अमित्रेभ्य:, प्रत्रासम्, वद) राष्ट्रविरोधी तत्त्वों और समाज कण्टकों के विरुद्ध कठोर दण्ड का आदेश देवे। (आज्येन, अभिधारित:) जैसे घृत से सिंचित समिधाएँ जलकर नष्ट हो जाती है, वैसे ही तेजस्वी राजा हिंसक और क्रूर अपराधियों को नष्ट कर दे।
भावार्थ— वेदविद्या का महान् ज्ञाता राजा अपनी प्रजा के लिए अन्न-धन आदि पदार्थों के न्याय-संगत वितरण की व्यवस्था करता है। सुख चाहने वाला कोई भी राष्ट्र गौ आदि उपकारी पशुओं को अपना आर्थिक आधार बनाता है और इसी क्रम में सबसे निरापद और शुद्ध पेशीय ऊर्जा का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त उस ऊर्जा का ही उपयोग करता है, जो पूर्णत: निरापद हो। राजा अपनी प्रजा के लिए माता-पिता के समान हितकारी होना चाहिए, जो प्रजा के लिए भय का कारण बने, उसे राजा नष्ट कर देवे। वह राजा पर्यावरण शोधनार्थ गोघृत आदि उत्तम पदार्थों से नित्य यज्ञ भी करने और कराने वाला हो एवं जिस प्रकार घृत की आहुति से अग्नि तेजस्वी होने लगता है, उसी प्रकार राजा भी ब्रह्मचर्यादि व्रतों और योगाभ्यास आदि से तेजयुक्त होवे।
आध्यात्मिक भाष्य— (वानस्पत्य:) प्राणविद्या का ज्ञाता और प्राणों को वश में रखने वाला योगाभ्यासी (उस्रियाभि:, संभृत:) वेद की ऋचाओं के द्वारा स्वयं को सम्यक् रूप से पुष्ट करता है और वह निरन्तर वेद की ऋचाओं में ही स्थित होता है। (विश्वगोत्र्य:) वह किसी कुल वा वंश विशेष का न होकर प्राणिमात्र के हित में ही लगा रहता है। (अमित्रेभ्य:, प्रत्रासम्, वद) वह योगी योगसाधना में बाधक चित्त वृत्तियों को अपनी अन्तश्चेतना द्वारा प्रतिबन्धित रहने का आदेश दे अर्थात् मन में आने वाले विकारों को बलपूर्वक प्रतिबन्धित करने का प्रयास करे। (आज्येन, अभिधारित:) [आज्यम् = प्राणो वा आज्यम् (तै.३.८.१५.२३), यज्ञो वा आज्यम् (तै.३.३.४.१)] ऐसा योगी अपने प्राणायामादि तपों के द्वारा प्राण बल को बढ़ाता हुआ परब्रह्म परमात्मा के साथ संगत होने का प्रयत्न करते हुए परहित की भावना से स्वयं को निरन्तर सिंचित करता रहे अथवा वह यज्ञस्वरूप परब्रह्म परमात्मा के प्रति प्रीति भावना से स्वयं को निरन्तर सिंचित करता रहे।
भावार्थ— प्राण को वशीभूत करने वाला योगी सदैव वेद की ऋचाओं में रमण करता है। वह प्राणिमात्र के आत्मा निरन्तर ईश्वर का वास अनुभव करता हुआ सदैव उनका हितचिंतन करता है। उसके मन में जब भी कोई विकार उत्पन्न होने वाला होता है, तब वह अपने मन को आदेश देकर बुरे विचारों को बाहर ही धकेल देता है। योगी का आत्मबल बहुत प्रबल होता है, क्योंकि वह सदैव ही स्वयं को ईश्वराधीन अनुभव करता है।
इन भाष्यों को पढक़र कोई भी वेदविरोधी यह बताये कि उसको इन भाष्यों पर क्या आपत्ति है?
Rig Veda 1.103.6 “…The Hero, watching like a thief in ambush, goes parting the possessions of the godless.” Tr. Ralph T.H. Griffith
आक्षेप का उत्तर—
यहाँ ये महाशय वैदिक ईश्वर को चोर बता रहे हैं और उसके लिए ग्रिफिथ के द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे ग्रिफिथ कोई वेदों का बहुत बड़ा विद्वान् हो। जिन विदेशी भाष्यकारों का उद्देश्य ही वेद को बदनाम करना हो, उसे प्रमाण रूप में प्रस्तुत करना दुर्भावना का ही परिचायक है। आप लोगों को अपने चौथे और सातवें आसमान पर रहने वाले ईश्वर की लीलाएँ तो दिखती नहीं, इधर आरोप लगाने चले। जहाँ तक स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती के अनुवाद का प्रश्न है, तो उन्होंने ईश्वर को नास्तिक और जनता के शोषक अर्थात् चोर, डाकू और ज्ञान के शत्रु से धन छीनकर ईमानदार लोगों को देने की बात कही है, उसको आपने चोरी कैसे बता दिया? मुस्लिम और ईसाई आक्रान्ता भारतवर्ष का धन लूटकर ले गये, क्या वह आपकी दृष्टि में अच्छा था? और दुुष्ट से धन लेकर सज्जन को देना चोरी कैसे हो गया? ये संस्कार आपके हो सकते हैं, हमारे नहीं। अब हम यहाँ ऋषि दयानन्द का भाष्य प्रस्तुत करते हैं—
भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमम्। य आदृत्या परिपन्थीव शूरोऽयज्वनो विभजन्नेति वेद: ॥ (ऋ.1.103.6)
पदार्थ: — (भूरिकर्मणे) बहुकर्मकारिणे (वृषभाय) श्रेष्ठाय (वृष्णे) सुखप्रापकाय (सत्यशुष्माय) नित्यबलाय (सुनवाम) निष्पादयेम (सोमम्) ऐश्वर्य्यसमूहम् (य:) (आदृत्य) आदरं कृत्वा (परिपन्थीव) यथा दस्युस्तथा चौराणां प्राणपदार्थहर्त्ता (शूर:) निर्भय: (अयज्वन:) यज्ञविरोधिन: (विभजन्) विभागं कुर्वन् (एति) प्राप्नोति (वेद:) धनम्।
भावार्थ: — अत्रोपमालङ्कार:। मनुष्यैर्यो दस्युवत् प्रगल्भ: साहसी सन् चौराणां सर्वस्वं हृत्वा सत्कर्मणामादरं विधाय पुरुषार्थी बलवानुत्तमो वर्त्तते, स एव सेनापति: कार्य्य:।
पदार्थ — हम लोग (य:) जो (शूर:) निडर शूरवीर पुरुष (आदृत्य) आदर सत्कार कर (परिपन्थीव) जैसे सब प्रकार से मार्ग में चले हुए डाकू दूसरे का धन आदि सर्वस्व हर लेते हैं, वैसे चोरों के प्राण और उनके पदार्थों को छीन कर हरने वाला, (विभजन्) विभाग अर्थात् श्रेष्ठ और दुष्ट पुरुषों को अलग-अलग करता हुआ, उनमें से (अयज्वन:) जो यज्ञ नहीं करते उनके (वेद:) धन को (एति) छीन लेता, उस (भूरिकर्मणे) भारी काम के करने वाले (वृषभाय) श्रेष्ठ (वृष्णे) सुख पहुँचाने वाले (सत्यशुष्माय) नित्य बली सेनापति के लिये जैसे (सोमम्) ऐश्वर्य्य समूह को (सुनवाम) उत्पन्न करें, वैसे तुम भी करो।
भावार्थ — इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो ऐसा ढीठ है कि जैसे डाकू आदि होते है और साहस करता हुआ चोरों के धन आदि पदार्थों को हर सज्जनों का आदर कर पुरुषार्थी बलवान् उत्तम से उत्तम हो, उसी को सेनापति करें।
हम यहाँ कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम तो आप यज्ञ शब्द का अर्थ समझ लेवें, जिसे हम पूूर्व में समझा चुके हैं। यहाँ कहा गया है कि जैसे कोई चोर बलपूर्वक किसी पथिक का धन लूट लेता है, वैसे ही वीर पुरुष को चाहिए कि वह चोर-डाकूओं के धन को बलपूर्वक छीन लेवे और जो परोपकारी सज्जन लोग हैं, उनका आदर करे और ऐसा वीर पुरुष ही सेनापति होवे। वर्तमान में भी तो न्यायप्रिय शासक चोरों के द्वारा चोरी किये गये धन का हरण करके जिसका धन चोरी हुआ है, उसको देते ही हैं अथवा वह धन राजकोष में उपयोग होता है और ऐसा अवश्य ही होना चाहिए। जब तक चोरों के धन को छीना नहीं जाएगा, तब तक चोरी-डाके जैसे अपराध बन्द भी नहीं होंगे। यहाँ यज्ञकर्म न करने वाले एवं यज्ञविरोधी से धन छीनने की बात कही गयी है, वह उचित ही है, क्योंकि जो परोपकार नहीं करता अथवा राज्य को कर नहीं देता, वह चोर ही है, तब उसका धन राजा वा सेनापति छीन ले, तो यह उचित ही है, जिससे उस धन का राष्ट्रहित में उपयोग हो सके।
हाँ, कोई चोर व्यक्ति अवश्य ही वेद के इस आदेश का विरोध करेगा। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए?
Rig Veda 1.103.6 “…The Hero, watching like a thief in ambush, goes parting the possessions of the godless.” Tr. Ralph T.H. Griffith
अग्नीषोमा चेति तद्वीर्यं वां यदमुष्णीतमवसं पणिं गा:। अवातिरतं बृसयस्य शेषोऽविन्दतञ्ज्योतिरेकं बहुभ्य:॥
हे अग्निदेव और सोमदेव! आपका वह पराक्रम उस समय ज्ञात हुआ, जब आपने ‘पणि’ से गौओं का हरण किया और ‘बृसय’ के शेष रक्षकों को क्षत-विक्षत किया। असंख्यों के लिये सूर्य प्रकाश का प्राकट्य किया।
आक्षेप का उत्तर—
यहाँ आपने जिनका भाष्य उद्धृत किया है, उनका आपने नाम नहीं लिया। ये दोनों ही भाष्यकार अग्नि और सोम से गायों की चोरी करवा रहे हैं। एक ओर तो ये भाष्यकार अग्नि और सोम देव के द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकट होना बताते हैं, उसी सूर्य को प्रकट करने वाले से गाय की चोरी करवाते हैं। इसमें तो रजवी आपको भी बुद्धि से सोचना चाहिए। गायों को चुराने वाला कोई मनुष्य तो हो सकता है, कोई मांसाहारी जानवर भी हो सकता है, परन्तु सूर्य को बनाने वाली सर्वशक्तिमती सत्ता गायों की चोरी करेगी, किसी के भोजन की चोरी करेगी, ऐसा तो कोई गम्भीर मानसिक रोगी ही सोच सकता है। अब हम इसका ऋषि दयानन्द का भाष्य यहाँ प्रस्तुत करते हैं—
पदार्थ: — (अग्नीषोमा) वायुविद्युतौ (चेति) विज्ञातं प्रख्यातमस्ति (तत्) (वीर्यम्) पृथिव्यादिलोकानां बलम् (वाम्) ययो: (यत्) (अमुष्णीतम्) चोरवद्धरतम् (अवसम्) रक्षणादिकम् (पणिम्) व्यवहारम् (गा:) किरणान् (अव) (अतिरतम्) तमो हिंस्त:। अवतिरतिरिति वधकर्मा.॥ निघं.२.१९॥ (बृसयस्य) आच्छादकस्य। वस आच्छादन इत्यस्मात् पृषोदरादित्वादिष्टसिद्धि:। (शेष:) अवशिष्टो भाग: (अविन्दतम्) लम्भयतम् (ज्योति:) दीप्तिम् (एकम्) असहायम् (बहूभ्य:) अनेकेभ्य: पदार्थेभ्य:।
भावार्थ: — मनुष्यैर्यावत्प्रसिद्धं तमस आच्छादकं सर्वंलोकप्रकाशकं तेजो जायते तावत्सर्वं कारणभूतयोर्वायुविद्युतो: सकाशाद्भवतीति बोध्यम्।
पदार्थ — जो (अग्नीषोमा) वायु और विद्युत् (यत्) जिस (अवसम्) रक्षा आदि (पणिम्) व्यवहार को (अमुष्णीतम्) चोरते प्रसिद्धाप्रसिद्ध ग्रहण करते (गा:) सूर्य्य की किरणों का विस्तार कर (अवातिरतम्) अन्धकार का विनाश करते (बहुभ्य:) अनेकों पदार्थों से (एकम्) एक (ज्योति:) सूर्य के प्रकाश को (अविन्दतम्) प्राप्त कराते हैं, जिनके (बृसयस्य) ढांपने वाले सूर्य का (शेष:) अवशेष भाग लोकों को प्राप्त होता है (वाम्) इनका (तत्) वह (वीर्य्यम्) पराक्रम (चेति) विदित है सब कोई जानते हैं।
भावार्थ — मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि जितना प्रसिद्ध अन्धकार को ढांप देने और सब लोकों को प्रकाशित करने हारा तेज होता है, उतना सब कारणरूप पवन और बिजुली की उत्तेजना से होता है।
यहाँ ऋषि दयानन्द ने वायु और विद्युत् के गुणों का वर्णन किया है। वस्तुत: यह वर्णन वेद में है। सूर्य अथवा किसी भी तारे के प्रकाश का मूल कारण वायु और विद्युत् है। इस बात को ऋषि दयानन्द के समय में संसार के बड़े-२ भौतिक वैज्ञानिक भी नहीं जानते होंगे। यहाँ वायु से तात्पर्य उस सूक्ष्म तत्त्व से है, जिससे फोटोन तथा मूल कणों का निर्माण होता है। वर्तमान विज्ञान की भाषा में इस पदार्थ की कुछ तुलना वैक्यूम एनर्जी और डार्क एनर्जी से कर सकते हैं। अब कोई वेद पर आक्षेप लगाने वाला अथवा ऋषि दयानन्द का उपहास करने वाला मुझे बताए कि वह प्रकाश की उत्पत्ति और उत्सर्जन वा अवशोषण आदि में वैक्यूम एनर्जी और विद्युत् की भूमिका के बारे में कितना ज्ञान रखता है? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप अथवा कोई भी वेदविरोधी शायद ही कुछ जानते हों। अब संसार भर के कथित धर्मग्रन्थों को मानने वाले बतायें कि उनके धर्मग्रन्थों में इस प्रकार की गम्भीर विद्या का कोई संकेत भी है? यहाँ ‘अमुष्णीतम्’ पद देखकर चोरी अर्थ ग्रहण कर लिया। ऋषि दयानन्द ने इसका अर्थ ‘चोरवद्धर्त्तम्’ किया है, जिसका अर्थ है— जैसे चोर चुपचाप किसी की वस्तु को उठाता है और किसी को उसका ज्ञान भी नहीं होता, वैसे ही सूर्यादि लोकों में विद्युत् और वायु रश्मियों की क्रियाएँ इस प्रकार से होती हैं कि उनको हम स्पष्टत: जान भी नहीं सकते। इसलिए इस प्रकार की उपमा दी गई है। आप आरोप लगाने से पहले थोड़ा तो बुद्धि से काम लेते, परन्तु क्या करें बुद्धि से काम तो बुद्धिमान् ही ले सकता है।
आपने इसी प्रकार के कुछ ओर उद्धरण दिये हैं, उनका उत्तर भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं।
संसार भर के वेदविरोधी वा भ्रान्त पाठकगण! मेरे इन तीन श्रेणी के कुल पाँच भाष्यों को पढक़र बतायें कि इस मन्त्र में हिंसा का विधान नहीं, बल्कि किसी भी राष्ट्र, समाज वा विश्व के कल्याण का सुन्दर उपाय सूत्र रूप में दर्शाया है। वास्तविक एवं बुद्धिमान् जिज्ञासु इस एक आक्षेप पर ही मेरे समाधान से वेद पर आक्षेपकर्ताओं की भावनाओं तथा भाष्यकारों की कमियों को समझ जायेंगे, पुनरपि मैं अन्य आक्षेपों का उत्तर भी शनै:-२ देता रहूँगा।


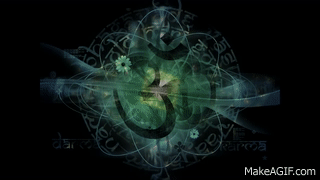




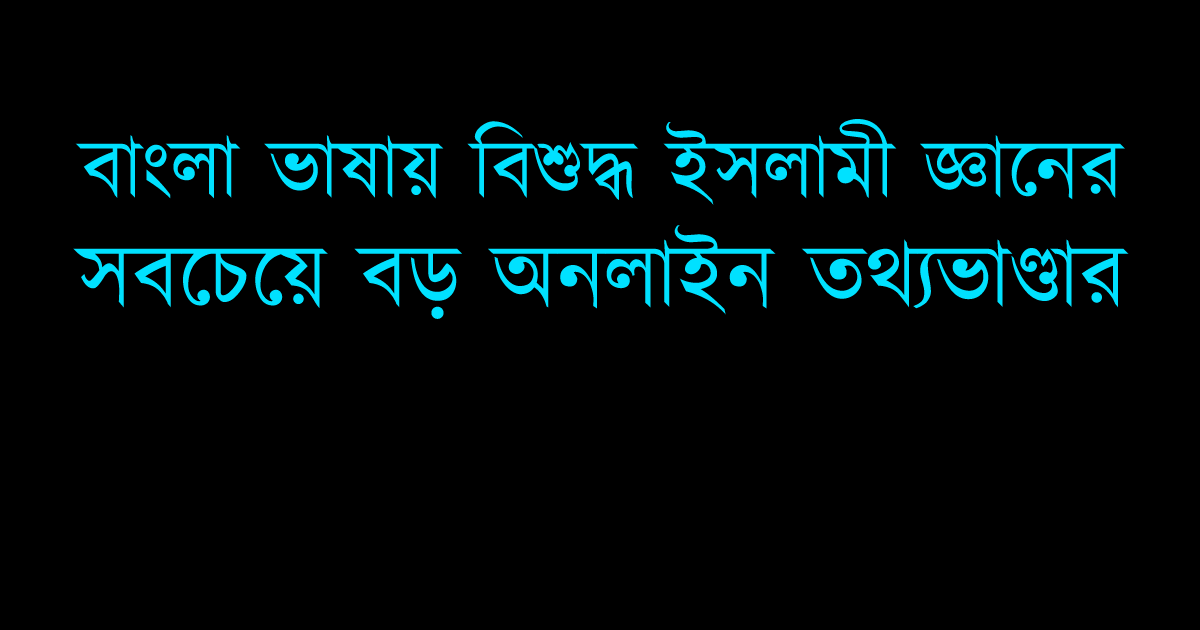


















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ