স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে মনুস্মৃতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন বৃ্হস্পতিস্মৃতিতে বলা হয়েছে-
মনুস্মৃতি অধ্যায় ১ (সৃষ্টি ও ধর্ম্ম উৎপত্তি বিষয়)
মনুমেকাগ্রমাসীনমভিগম্য মহর্ষযঃ ।
প্রতিপূজ্য যথান্যাযমিদং বচনমঅব্রুবন্ ।। মনু ১।১
(महर्षयः) महर्षि लोग( एकाग्रम् आसीनम्) एकाग्रतापूर्वक बैठे हुए (मनुम्) मनु के (अभिगम्य) पास जाकर, और उनका (यथान्यायम् )यथोचित (प्रतिपूज्य) सत्कार करके (इदम् )यह वचनम् वचन (अब्रुवन्) बोले । महर्षियों का मनु से वर्णाश्रम धर्मों के विषय में प्रश्न -
Commentary by: पण्डित राजवीर शास्त्री जी
অন্তরপ্রভবানাং চ ধর্মান্নো বক্তুম অর্হসি ।। মনু ১।২
(भगवन्) हे भगवन्! आप (सर्ववर्णानाम्) सब वर्णों - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र,( च) और (अन्तरप्रभवाणाम्) सभी वर्णों के अन्दर होने वाले अर्थात् आश्रमों - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के (वर्णानां अन्तरे प्रभवः )- उत्पत्ति; , स्थितिः (येषां ते अन्तरप्रभवाः - आश्रमाः धर्मान्) धर्म - कत्र्तव्यों को यथावत् ठीक - ठीक रूप से( अनुपूर्वशः) और क्रमानुसार अर्थात् वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय , वैश्य और शूद्र के क्रम से तथा आश्रमों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के क्रम से( नः) हमें (वक्तुम्) बतलाने में (अर्हसि) समर्थ हो ।
टिप्पणी :
मनुस्मृति की भूमिका में - कूल्लूकभट्टादि टीकाकारों द्वारा अन्यथा व्याख्यात प्रक्षेप - रहित श्लोक १. (१।२) श्लोक के ‘अन्तरप्रभवाणाम्’ पद की व्याख्या मेधातिथि, कुल्लूकभट्टादि टीकाकारों ने ‘संकीर्णजातियाँ या वर्णसंकर’ किया है । यह उनकी व्याख्या सर्वथा असंगत, मनु के आशय से विरूद्ध तथा अविवेकपूर्ण है । इसका अर्थ ‘आश्रम’ होना चाहिये । क्यों कि मनु ने वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों का ही मनुस्मृति में वर्णन किया है और जो वर्णों से पतित हो गये हैं, चाहे वे वर्णसंकर हों अथवा संकीर्णजातियाँ, उनके अशास्त्रीय कर्मों को धर्म शब्द से कहा ही नहीं जा सकता । ‘धर्मो धारयते प्रजाः’ ‘धारणाद् धर्म इत्याहुः’ इत्यादि वचनों के अनुसार प्रजा को धारण - व्यवस्थित रखने वाले श्रेष्ठ गुणों को ही धर्म शब्द से ग्रहण किया जाता है । अतः इस श्लोक में धर्म शब्द के साथ वर्ण - संकरादि अर्थ की क्या संगति हो सकती है ? और महर्षियों को उनके धर्म - विरूद्ध कार्यों को पूछने का क्या प्रयोजन हो सकता है ? और श्लोक के ‘अन्तरप्रभव’ शब्द से ‘आश्रम’ धर्म की अभिव्यक्ति भी हो रही है । ‘‘अन्तरे - वर्णानां मध्ये प्रभव उत्पत्तिर्येषां ते अन्तरप्रभवा आश्रमाः ।’’ क्यों कि ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों की उत्पत्ति वर्णों के मध्य ही है, अतः इन्हें ‘अन्तरप्रभव’ कहते हैं । और यदि यह अर्थ किसी को स्वीकार करने में कुछ संकोच होता है तो उसे विचार करना चाहिये कि महर्षियों के प्रश्नों के अनुरूप ही तो मनु जी को उत्तर देना चाहिये था, फिर आश्रमों के कर्मों (धर्मों) का वर्णन मनु जी ने क्यों किया ? अतः मनु के वण्र्यविषय के अनुसार भी ‘आश्रम’ अर्थ ही सुसंगत होता है । इसकी पुष्टि में कुछ और तथ्य देखिये - (क) ‘अन्तरप्रभव’ शब्द का दूसरा पर्यायवाची शब्द मनु जी ने ‘सान्तरालं’ प्रयुक्त किया है । (१।१३७/२ ।१८) श्लोक में (१।२) श्लोक की भांति कहा है - ‘वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ।’ सदाचार की परिभाषा वर्णों और सान्तरालों - आश्रमों के आचार को ही माना है । यदि ‘सान्तराल’ शब्द का अर्थ मनु जी को वर्णसंकरादि अभीष्ट होता तो उनके आचार को सदाचार कभी नहीं कहते । क्यों कि वर्णसंकरादि के आचार को दशम अध्याय में निन्दनीय कहा गया है , जिसका यहाँ पृथक् वर्णन पाठक पढ़ सकते हैं । अतः ‘सान्तराल’ शब्द की भांति ‘अन्तरप्रभव’ का अर्थ भी ‘आश्रम’ ही करना चाहिये । यद्यपि टीकाकारों ने (२।१८) श्लोक में भी वर्णसंकरादि असंगत अर्थ किया है, किन्तु उसकी वहाँ लेशमात्र भी संगति नह होने से टीकाकारों की भ्रान्त - व्याख्या ही कहनी चाहिये । क्यों कि मनु जी ने जिस ब्रह्मावत्र्त देश में रहने वाले ब्राह्मणों से विश्व को चरित्र की शिक्षा लेने का आदेश दिया है, वह उत्तम सदाचार वर्णसंकरों का कदापि नहीं हो सकता । क्यों कि मनु जी ने वर्णसंकरों के आचरण को निन्दनीय बताया है । उसके कुछ प्रमाण देखिये - ‘मातृदोषविगर्हितान्’ (१०।७) माता के दोष से निन्दित । ‘क्रू राचारविहारवान्’ (१०।९) क्रूर आचार - व्यवहार वाले । ‘अधमो नृणाम्’ (१०।१२) मनुष्यों में नीच । ‘अव्रतांस्तु यान्’ (१०।२०) व्रत - हीन । ‘पापात्मा भूर्जकण्टकः’ (१०।२१) पापी आत्मा वाले । इसी प्रकार संकीर्ण जातियों को ‘अपसद - नीच’ ‘अपध्वंसज’ पतितोत्पन्न आदि शब्दों से कहा गया है । अतः इनका आचरण न तो धर्म कहा जा सकता और नहीं सदाचार । (ख) मनुस्मृति के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें वर्णों के धर्मों के साथ - साथ आश्रमों के धर्मों का ही कथन है, वर्णसंकरों का नहीं । द्वितीयाध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम का, तृतीयाध्याय से पंच्चमाध्याय तक गृहस्थाश्रम का, षष्ठाध्याय में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का वर्णन है । साथ - साथ वर्णधर्मों का वर्णन भी किया है । अतः ‘अन्तर - प्रभव’ या ‘सान्तराल’ आश्रम - धर्म ही हैं । (ग) मनुस्मृति में वर्णों के साथ - साथ आश्रमों के वर्णन की ही प्रवृत्ति दिखाई देती है । जैसे - ‘चातुर्वण्र्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्’ (१२।९७) । ‘वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टो ऽभिरक्षिता (७।३५) यहां राजा को वर्णों तथा आश्रमों का रक्षक कहा है । वर्णों के साथ वर्णसंकरों का उल्लेख नहीं है । जैसे - सुख - दुःख, लाभ - हानि, जय - पराजयादि एक दूसरे से विपरीत हैं, वैसे ही वर्ण तथा वर्णसंकर भी हैं । एक से राष्ट्र की रक्षा या व्यवस्था होती है, तो दूसरे से राष्ट्र की हानि । एक से मानव उन्नत होकर सुखी होता है, तो दूसरे से मानव का पतन तथा दुःखवृद्धि । अतः परस्पर विरोधियों को पूछने का न तो ऋषियों का अभिप्राय ही था और नहीं मनु को ही अभिप्रेत है । और जैसे धर्म को जानने से अधर्म का, शुभकर्मों को जानने से अशुभकर्मों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है, वैसे ही वर्ण से वर्णसंकर का ग्रहण हो जाता , फिर पृथक् से पूछने की आवश्यकता भी क्या थी ?’ (घ) वर्णसंकरों के विषय में मनुस्मृति की अन्तःसाक्षी देखिये - मनु० १०।२४. अर्थात् वर्णों के व्यभिचार से, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने से और अपने कत्र्तव्य - कर्मों के त्यागपूर्वक उत्पन्न सन्तान ‘वर्णसंकर’ कहलाती हैं । मनु० १०।२५. और संकीर्ण योनियाँ वे होती हैं - जो अवैध रूप से मिश्रित वर्णों से उत्पन्न होती हैं, उनकी उत्पत्ति प्रतिलोम - अनुलोम तथा पारस्परिक संबंध से होती है, उनको सम्पूर्णता से कहता हूँ । इन वर्णसंकरों और संकीर्ण - जातियों के होने से राष्ट्र की क्या दशा हो जाती है - मनु० १।६१. अर्थात् जिस राष्ट्र में वर्ण - कर्मों से पतित होकर ये वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं, वह राष्ट्र राष्ट्र - निवासियों के साथ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । मनु० १०।४५ अर्थ - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन की क्रियाओं का लोपादि करने से जो बहिष्कृत जातियाँ - वर्णसंकर या संकीर्ण जातियाँ हो जाती हैं, वे चाहे म्लेच्छभाषा बोलती हो या आर्यभाषा, सब दस्यु कहलाती हैं । मनु० १०।५३ अर्थ - धर्मभीरू व्यक्ति को चाहिये कि इन वर्णसंकर या संकीर्णजातियों से संपर्क करने की इच्छा भी न करे । अतः निन्दनीय या गर्हित कर्म वाले एवं राष्ट्र - नाशक वर्णसंकरों के कर्मों को धर्म मानने एवं उनका वर्णन पूछने का ऋषियों का कदापि आशय नहीं था । इसलिये इस पद की वर्णसंकर - परक व्याख्या भ्रान्तिवश असंगत की है । कहीं - कहीं तो ‘संकरप्रभवाणाम्’ ही पाठ - भेद भ्रान्तिवश किया गया मिलता है । जो भ्रान्तव्याख्याओं के कारण ही पाठ - भेद किया गया है । २. (१।३) यह दुर्भाग्य की बात रही है कि मनुस्मृति जैसे प्रामाणिक धर्मशास्त्र के कुल्लूकभट्टादि समस्त टीकाकारों ने १।३ श्लोकों के ‘अस्य सर्वस्य’ पदों का अर्थ विधानस्य - वेद के साथ मिलाकर किया है, किन्तु यह अर्थ असंगत - अपूर्ण तथा अविवेकपूर्ण है । इसी अर्थ के कारण यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई कि ऋषियों का प्रश्न वेद - विषयक था, तो उत्तर सृष्टि - उत्पत्ति विषयक क्यों ? इन प्रश्न - उत्तरों की संगति टीकाकार नहीं लगा सके हैं । अतः इसका ‘अस्य - सर्वस्य - इस प्रत्यक्ष विद्यमान जगत् का’ ही अर्थ करना उचित है । ‘इदम्’ सर्वनाम इस अर्थ को घोषित कर रहा है । इस सर्वनाम से प्रत्यक्ष वस्तु का ही निर्देश किया जाता है । ‘सर्व और विश्व’ शब्द पर्यायवाची हैं । जब ये सबके वाचक हैं तब ही इनका नाम सर्वनाम है, जगदादि अर्थों में नहीं । अतः ‘सर्वस्य’ का अर्थ ‘जगतः’ करना चाहिये । मनु जी ने इस बात का स्पष्टीकरण उत्तर में कहे निम्न श्लोक से दिया है - मनु० १।५. इस श्लोक में स्पष्ट रूप से यद्यपि ‘जगत्’ शब्द नहीं पठित है, और नहीं ऊपर से ही अनुवृत्ति आ रही है, पुनरपि सभी टीकाकारों ने इस श्लोक की जगत् - परक व्याख्या की है, इसी प्रकार इस (१।३) श्लोक में भी ‘जगत्’ अर्थ करने में कैसे असंगति हो सकती है ? ‘अस्य’ और ‘इदम्’ दोनों ही एक शब्द के रूप हैं । यदि ‘इदम्’ शब्द से जगत् का परामर्श हो सकता है, तो ‘अस्य’ से क्यों नहीं ? और इस श्लोक के ‘कार्यतत्त्चसर्थवित्’ शब्द से भी इस अर्थ की संगति हो रही है । यह पद समस्त है । यहाँ मनु जी को कार्यतत्त्वों तथा अर्थों को जानने वाला कहा है । इसकी संगति श्लोक में इस तरह लगती है कि अस्य सर्वस्य - इस जगत् के कार्यतत्त्व - कारण से बने स्थूल पदार्थों के तत्त्व - सूक्ष्म - कारण प्रकृति महत्तत्त्वादि को आप जानते हैं और सनातन परमात्मा का जो विधान - वेद है, उसके गहन अर्थों को भी आप जानते हैं । शेष ‘अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य’ पद दोनों के साथ लग सकते हैं । वेद - परक तो इन पदों की सबने व्याख्या मानी ही है और जगत् - परक स्वयं मनु जी ने (१।५) में ‘अतक्र्यम् अविज्ञेयम्’ कहकर कर दी है । और जगत् - परक व्याख्या में वेद का भी प्रमाण है - अर्थात् यह सब जगत् सृष्टि से पहिले अन्धकार से आवृत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य ......................................................................था । और जैसे वेद जगत् का विधान है और वेद को मनुस्मृति में - मनु० १२।९४ चक्षुः - ‘चक्षिड् व्यक्तायां वाचि अयं दर्शनेऽपि’ इस धात्वर्थ के अनुसार वेद समस्त विधान को स्पष्ट तथा निभ्र्रान्त रूप से बताता है, वैसे ‘जगत्’ भी बताता है । जगत् तथा वेद क्रमशः परमेश्वर की रचना तथा ज्ञान हैं, अतः वेदान्त - दर्शन के अनुसार ‘तत्तु समन्वयात्’ वेद और जगत् में समन्वय है । ‘विष्णोः कर्माणि पश्यत’ इत्यादि वेद - प्रमाणों से स्पष्ट है कि परमात्मा की रचना को देखकर परमेश्वर का ज्ञान होता है, अतः यह जगत् भी चक्षु - परमात्मा की व्याख्या व सिद्धि करता है । और इस श्लोक के कार्यतत्त्वार्थवित् पद को भी कुल्लूकभट्टादि समझने में सर्वथा ही असमर्थ रहे हैं । उन्होंने इस पद के ‘कार्य’ शब्द का ‘अग्निष्टोमादि यज्ञ’ और ‘तत्त्व’ शब्द का ‘ब्रह्म’ अर्थ किया है । यह उनका अर्थ असंगत तथा त्रुटिपूर्ण है । उनकी व्याख्या में निम्नदोष हैं - (क) महर्षियों ने जिस विषय का प्रश्न किया था, उसी को जानने वाला मनु जी को कहना उचित है । प्रश्न तो किया गया है वर्ण व आश्रमों के धर्मों का और मनु जी के लिये विशेषण दिया जाये यज्ञ तथा ब्रह्म को जानने का, इनमें परस्पर कोई संगति नहीं है । और कार्यतत्त्व तथा वेदार्थवित् कहना इस लिये संगत है कि वेद ही सब धर्मों का मूल है । ‘धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः’ आदि कहकर मनु जी ने इसे स्पष्ट किया है । और ‘अस्य सर्वस्य कार्यतत्त्वार्थवित्’ कहकर ऋषियों ने सृष्टि - उत्पत्ति की भी परोक्षरूप में जिज्ञासा प्रकट की और मनु जी ने उसका उत्तर दिया है । (ख) ‘कार्य’ शब्द का यज्ञ तथा ‘तत्त्व’ शब्द का ब्रह्म अर्थ है, इसमें जहाँ प्रकरण से विरोध है, वहाँ इस अर्थ में कोई प्रमाण भी नहीं है । कारण से जो बने उसे कार्य कहते हैं, अथवा करणीय कर्मों को कार्य कहते हैं । यद्यपि ‘यज्ञ’ भी एक कत्र्तव्य कर्म है, किन्तु यज्ञ ही कत्र्तव्य नहीं है और नहीं इस शास्त्र में यज्ञों का ही वर्णन माना जा सकता है । यज्ञ तो एक अंग हैं, अंगी नहीं । (ग) और श्लोक - पठित ‘कार्यतत्त्व’ शब्द का पृथक् - पृथक् करके अर्थ भी विद्वदभिनन्दनीय नहीं हो सकता । क्यों कि ‘तत्त्व’ शब्द सामेक्ष है , जो ‘कार्य’ शब्द के बिना पूर्ण - अर्थ का बोधक नहीं हो सकता । और ‘कार्यतत्त्वार्थवित्’ शब्द के ‘अर्थ’ शब्द तो इनकी व्याख्या में निरर्थक ही हो जाता है । (घ) मनुस्मृति के इन कुल्लूकभट्टादि व्याख्या करने वालों पर पौराणिक भाष्यकार सायणाचार्य की मान्यता का यह प्रभाव था कि वेद यज्ञ के लिये हैं । वेदों में यज्ञों का ही प्रतिपादन है । इसलिये उन्होंने क्लिष्ट - कल्पना करके ‘कार्य’ शब्द का यज्ञ अर्थ कर दिया है । वास्तव में यह एक मिथ्या और मनुस्मृति के विरूद्ध कल्पना मात्र ही है । वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है । इसमें कतिपय मनुस्मृति के ही प्रमाण देखिये - (१।२४) श्लोक में लिखा है - वेदों से ही समस्त पदार्थों का नाम रखे गये और सब मनुष्यों के कर्मों तथा पृथक् व्यवस्थाओं का निर्धारण किया गया । (१२।९७) में चारों वर्णों, आश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से माना है । (१२।९८) शब्द, स्पशट आदि सूक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों के द्वारा मानी है । (१२।९९) में जगत् के समस्त व्यवहारों का सर्वोपरि साधक वेद को माना है । (७।४३,१२,१००) में राजनीति की शिक्षा देने वाला, (१२।१०९-११३) में धर्माधर्म का ज्ञान देने वाला, (१।२४) और (१।२१) में जगत् के श्रेष्ठ व्यवहारों का साधक वेद को माना है । (१२।९४) में पितर, देव तथा मनुष्यों को समस्त ज्ञान - विज्ञान आदि दर्शाने के कारण वेद को ‘चक्षुः’ शब्द से कहा गया है । (ड) और मनुस्मृति के इन टीकाकारों की व्याख्या प्रसंग के विरूद्ध भी है । ऋषियों ने मनु जी के पास आकर वर्णों और आश्रमों के धर्म के बारे में प्रश्न किया था । उन्हें धर्म के मूलाकरण वेदार्थवेत्ता कहना तो संगत है, यज्ञादि का वेत्ता कहना प्रसंगविरूद्ध है । प्रसंगानुकूल ही विशेषणों से विशेषित करना उचित है । और जो वेदार्थवेत्ता है, वही धर्मोपदेश करने में समर्थ हो सकता है, यह स्वयं मनु जी ने १२वें अध्याय के १०८ - ११४ श्लोंकों में कहा है । इस प्रकार कुल्लूकभट्टादि का किया अर्थ सर्वथा असंगत, युक्तिविरूद्ध, अव्यावहारिक तथा मनु जी के आशय से विरूद्ध होने से मान्य नहीं हो सकता । ३. मनुस्मृति के इन (१-४) प्रथम चार श्लोकों के विषय में भी कुछ टीकाकारों की यह भ्रान्त धारणा है कि मनुस्मृति का प्रारम्भ पांचवें श्लोक से होता है, ये प्रथम चार श्लोक भृगु अथवा किसी शिष्य के बनाये हुए हैं । यद्यपि १-४ श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की भांति मौलिक नहीं हैं, तथापि इनकी शैली, घटना और प्रश्नों के आधार पर इन्हें मौलिक मानने में संकोच नहीं करना चाहिये । क्यों कि मनु जी के किसी शिष्य ने तत्कालीन घटना तथा भावों के अनुरूप ही भूमिका के रूप में इन श्लोकों का संकलन किया है । घटना तथा प्रश्न दोनों ही यथार्थता को लिये हुए हैं । जिन शिष्यों ने सम्पूर्ण प्रवचनरूप मनुस्मृति का संकलन किया है, उन्होंने ही इन भूमिका के श्लोकों का संकलन किया है । अतः दूसरे मौलिक श्लोकों की भांति इन्हें भी संगत मानना उचित है । और इनके बिना प्रकरण की संगति भी नहीं लग पाती । और कुछ टीकाकारों ने इन चार श्लोकों की शैली के आधार पर मध्य - मध्य में किये प्रक्षिप्त - श्लोकों को भी, (जैसे - मनुरब्रवीत् ।। (८।३३९) मनुना परिकीर्तितः ।। (१।१२६) उक्तवान् मनुः ।। (१।११८) इत्यादि को मौलिक मानने का प्रयत्न किया है । किन्तु उनकी यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है । क्यों कि मनुस्मृति एक प्रवचन किया हुआ ग्रन्थ है । इसका संकलन मात्र ही शिष्यों ने किया है, किन्तु मनु के भावों को लेकर श्लोकों को नहीं बनाया गया है । संकलन में संकलयिता अपनी ओर से कुछ नहीं लिख सकता, किन्तु भावानुरूप भाषा से श्लोक बनाने में स्वंय भी कुछ लिख सकता है । यह मनुस्मृति की अन्तः साक्षी से स्पष्ट हो जाता कि मनु द्वारा प्रवचन किये श्लोकों के अनुरूप ही संकलन किया गया है । यह बात ‘श्रूयताम्’ ‘निबोधत’ आदि क्रियाओं से परिपुष्ट हो जाती है । यदि यह भावानुरूप बाद की रचना होती, तो ऐसी क्रियाओं का प्रयोग कैसे हो सकता है ? अतः मनु आदि शब्दों को लेकर अर्वाचीन श्लोकों को मौलिक सिद्ध नहीं किया जा सकता ।)
Commentary by: पण्डित राजवीर शास्त्री जी
ত্বমেকো হ্যস্য সর্বস্য বিধানস্য স্বযংভুবঃ ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেযস্য কার্যতত্ত্বার্থবিত্ প্রভো ।। মনু০ ১।৩
(हि) क्यों कि प्रभो हे भगवन्! (अस्य सर्वस्य) इस सब प्रलय समय( ‘अचिन्त्यस्य अप्रमेस्य’) अर्थात् अविज्ञ जगत् के ‘कार्यतत्त्व’ कारण से बने स्थूल पदार्थों के तत्त्व सूक्ष्म कारण प्रकृतिमय तत्त्वादि को आप जानते हैं । तथा (स्मयम्भुवः) स्वयम्भू जो सनातन विधानस्य विधानरूप वेद हैं (अचिन्त्यस्य) जिनमें असत्य कुछ भी नहीं अथवा जिनका चिन्तन से पार नहीं पाया जा सकता (अप्रमेयस्य) जिनमें सब अर्थात् अपरिमित सत्यविद्याओं का विधान है उनमें विहित और अर्थवित् उनके अर्थों को जानने वाले( एकः त्वम्) केवल आप ही हैं ।
टिप्पणी :
मनुस्मृति की भूमिका में - कूल्लूकभट्टादि टीकाकारों द्वारा अन्यथा व्याख्यात प्रक्षेप - रहित श्लोक १. (१।२) श्लोक के ‘अन्तरप्रभवाणाम्’ पद की व्याख्या मेधातिथि, कुल्लूकभट्टादि टीकाकारों ने ‘संकीर्णजातियाँ या वर्णसंकर’ किया है । यह उनकी व्याख्या सर्वथा असंगत, मनु के आशय से विरूद्ध तथा अविवेकपूर्ण है । इसका अर्थ ‘आश्रम’ होना चाहिये । क्यों कि मनु ने वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों का ही मनुस्मृति में वर्णन किया है और जो वर्णों से पतित हो गये हैं, चाहे वे वर्णसंकर हों अथवा संकीर्णजातियाँ, उनके अशास्त्रीय कर्मों को धर्म शब्द से कहा ही नहीं जा सकता । ‘धर्मो धारयते प्रजाः’ ‘धारणाद् धर्म इत्याहुः’ इत्यादि वचनों के अनुसार प्रजा को धारण - व्यवस्थित रखने वाले श्रेष्ठ गुणों को ही धर्म शब्द से ग्रहण किया जाता है । अतः इस श्लोक में धर्म शब्द के साथ वर्ण - संकरादि अर्थ की क्या संगति हो सकती है ? और महर्षियों को उनके धर्म - विरूद्ध कार्यों को पूछने का क्या प्रयोजन हो सकता है ? और श्लोक के ‘अन्तरप्रभव’ शब्द से ‘आश्रम’ धर्म की अभिव्यक्ति भी हो रही है । ‘‘अन्तरे - वर्णानां मध्ये प्रभव उत्पत्तिर्येषां ते अन्तरप्रभवा आश्रमाः ।’’ क्यों कि ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों की उत्पत्ति वर्णों के मध्य ही है, अतः इन्हें ‘अन्तरप्रभव’ कहते हैं । और यदि यह अर्थ किसी को स्वीकार करने में कुछ संकोच होता है तो उसे विचार करना चाहिये कि महर्षियों के प्रश्नों के अनुरूप ही तो मनु जी को उत्तर देना चाहिये था, फिर आश्रमों के कर्मों (धर्मों) का वर्णन मनु जी ने क्यों किया ? अतः मनु के वण्र्यविषय के अनुसार भी ‘आश्रम’ अर्थ ही सुसंगत होता है । इसकी पुष्टि में कुछ और तथ्य देखिये - (क) ‘अन्तरप्रभव’ शब्द का दूसरा पर्यायवाची शब्द मनु जी ने ‘सान्तरालं’ प्रयुक्त किया है । (१।१३७/२ ।१८) श्लोक में (१।२) श्लोक की भांति कहा है - ‘वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ।’ सदाचार की परिभाषा वर्णों और सान्तरालों - आश्रमों के आचार को ही माना है । यदि ‘सान्तराल’ शब्द का अर्थ मनु जी को वर्णसंकरादि अभीष्ट होता तो उनके आचार को सदाचार कभी नहीं कहते । क्यों कि वर्णसंकरादि के आचार को दशम अध्याय में निन्दनीय कहा गया है , जिसका यहाँ पृथक् वर्णन पाठक पढ़ सकते हैं । अतः ‘सान्तराल’ शब्द की भांति ‘अन्तरप्रभव’ का अर्थ भी ‘आश्रम’ ही करना चाहिये । यद्यपि टीकाकारों ने (२।१८) श्लोक में भी वर्णसंकरादि असंगत अर्थ किया है, किन्तु उसकी वहाँ लेशमात्र भी संगति नह होने से टीकाकारों की भ्रान्त - व्याख्या ही कहनी चाहिये । क्यों कि मनु जी ने जिस ब्रह्मावत्र्त देश में रहने वाले ब्राह्मणों से विश्व को चरित्र की शिक्षा लेने का आदेश दिया है, वह उत्तम सदाचार वर्णसंकरों का कदापि नहीं हो सकता । क्यों कि मनु जी ने वर्णसंकरों के आचरण को निन्दनीय बताया है । उसके कुछ प्रमाण देखिये - ‘मातृदोषविगर्हितान्’ (१०।७) माता के दोष से निन्दित । ‘क्रू राचारविहारवान्’ (१०।९) क्रूर आचार - व्यवहार वाले । ‘अधमो नृणाम्’ (१०।१२) मनुष्यों में नीच । ‘अव्रतांस्तु यान्’ (१०।२०) व्रत - हीन । ‘पापात्मा भूर्जकण्टकः’ (१०।२१) पापी आत्मा वाले । इसी प्रकार संकीर्ण जातियों को ‘अपसद - नीच’ ‘अपध्वंसज’ पतितोत्पन्न आदि शब्दों से कहा गया है । अतः इनका आचरण न तो धर्म कहा जा सकता और नहीं सदाचार । (ख) मनुस्मृति के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें वर्णों के धर्मों के साथ - साथ आश्रमों के धर्मों का ही कथन है, वर्णसंकरों का नहीं । द्वितीयाध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम का, तृतीयाध्याय से पंच्चमाध्याय तक गृहस्थाश्रम का, षष्ठाध्याय में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का वर्णन है । साथ - साथ वर्णधर्मों का वर्णन भी किया है । अतः ‘अन्तर - प्रभव’ या ‘सान्तराल’ आश्रम - धर्म ही हैं । (ग) मनुस्मृति में वर्णों के साथ - साथ आश्रमों के वर्णन की ही प्रवृत्ति दिखाई देती है । जैसे - ‘चातुर्वण्र्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्’ (१२।९७) । ‘वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टो ऽभिरक्षिता (७।३५) यहां राजा को वर्णों तथा आश्रमों का रक्षक कहा है । वर्णों के साथ वर्णसंकरों का उल्लेख नहीं है । जैसे - सुख - दुःख, लाभ - हानि, जय - पराजयादि एक दूसरे से विपरीत हैं, वैसे ही वर्ण तथा वर्णसंकर भी हैं । एक से राष्ट्र की रक्षा या व्यवस्था होती है, तो दूसरे से राष्ट्र की हानि । एक से मानव उन्नत होकर सुखी होता है, तो दूसरे से मानव का पतन तथा दुःखवृद्धि । अतः परस्पर विरोधियों को पूछने का न तो ऋषियों का अभिप्राय ही था और नहीं मनु को ही अभिप्रेत है । और जैसे धर्म को जानने से अधर्म का, शुभकर्मों को जानने से अशुभकर्मों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है, वैसे ही वर्ण से वर्णसंकर का ग्रहण हो जाता , फिर पृथक् से पूछने की आवश्यकता भी क्या थी ?’ (घ) वर्णसंकरों के विषय में मनुस्मृति की अन्तःसाक्षी देखिये - मनु० १०।२४. अर्थात् वर्णों के व्यभिचार से, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने से और अपने कत्र्तव्य - कर्मों के त्यागपूर्वक उत्पन्न सन्तान ‘वर्णसंकर’ कहलाती हैं । मनु० १०।२५. और संकीर्ण योनियाँ वे होती हैं - जो अवैध रूप से मिश्रित वर्णों से उत्पन्न होती हैं, उनकी उत्पत्ति प्रतिलोम - अनुलोम तथा पारस्परिक संबंध से होती है, उनको सम्पूर्णता से कहता हूँ । इन वर्णसंकरों और संकीर्ण - जातियों के होने से राष्ट्र की क्या दशा हो जाती है - मनु० १।६१. अर्थात् जिस राष्ट्र में वर्ण - कर्मों से पतित होकर ये वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं, वह राष्ट्र राष्ट्र - निवासियों के साथ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । मनु० १०।४५ अर्थ - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन की क्रियाओं का लोपादि करने से जो बहिष्कृत जातियाँ - वर्णसंकर या संकीर्ण जातियाँ हो जाती हैं, वे चाहे म्लेच्छभाषा बोलती हो या आर्यभाषा, सब दस्यु कहलाती हैं । मनु० १०।५३ अर्थ - धर्मभीरू व्यक्ति को चाहिये कि इन वर्णसंकर या संकीर्णजातियों से संपर्क करने की इच्छा भी न करे । अतः निन्दनीय या गर्हित कर्म वाले एवं राष्ट्र - नाशक वर्णसंकरों के कर्मों को धर्म मानने एवं उनका वर्णन पूछने का ऋषियों का कदापि आशय नहीं था । इसलिये इस पद की वर्णसंकर - परक व्याख्या भ्रान्तिवश असंगत की है । कहीं - कहीं तो ‘संकरप्रभवाणाम्’ ही पाठ - भेद भ्रान्तिवश किया गया मिलता है । जो भ्रान्तव्याख्याओं के कारण ही पाठ - भेद किया गया है । २. (१।३) यह दुर्भाग्य की बात रही है कि मनुस्मृति जैसे प्रामाणिक धर्मशास्त्र के कुल्लूकभट्टादि समस्त टीकाकारों ने १।३ श्लोकों के ‘अस्य सर्वस्य’ पदों का अर्थ विधानस्य - वेद के साथ मिलाकर किया है, किन्तु यह अर्थ असंगत - अपूर्ण तथा अविवेकपूर्ण है । इसी अर्थ के कारण यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई कि ऋषियों का प्रश्न वेद - विषयक था, तो उत्तर सृष्टि - उत्पत्ति विषयक क्यों ? इन प्रश्न - उत्तरों की संगति टीकाकार नहीं लगा सके हैं । अतः इसका ‘अस्य - सर्वस्य - इस प्रत्यक्ष विद्यमान जगत् का’ ही अर्थ करना उचित है । ‘इदम्’ सर्वनाम इस अर्थ को घोषित कर रहा है । इस सर्वनाम से प्रत्यक्ष वस्तु का ही निर्देश किया जाता है । ‘सर्व और विश्व’ शब्द पर्यायवाची हैं । जब ये सबके वाचक हैं तब ही इनका नाम सर्वनाम है, जगदादि अर्थों में नहीं । अतः ‘सर्वस्य’ का अर्थ ‘जगतः’ करना चाहिये । मनु जी ने इस बात का स्पष्टीकरण उत्तर में कहे निम्न श्लोक से दिया है - मनु० १।५. इस श्लोक में स्पष्ट रूप से यद्यपि ‘जगत्’ शब्द नहीं पठित है, और नहीं ऊपर से ही अनुवृत्ति आ रही है, पुनरपि सभी टीकाकारों ने इस श्लोक की जगत् - परक व्याख्या की है, इसी प्रकार इस (१।३) श्लोक में भी ‘जगत्’ अर्थ करने में कैसे असंगति हो सकती है ? ‘अस्य’ और ‘इदम्’ दोनों ही एक शब्द के रूप हैं । यदि ‘इदम्’ शब्द से जगत् का परामर्श हो सकता है, तो ‘अस्य’ से क्यों नहीं ? और इस श्लोक के ‘कार्यतत्त्चसर्थवित्’ शब्द से भी इस अर्थ की संगति हो रही है । यह पद समस्त है । यहाँ मनु जी को कार्यतत्त्वों तथा अर्थों को जानने वाला कहा है । इसकी संगति श्लोक में इस तरह लगती है कि अस्य सर्वस्य - इस जगत् के कार्यतत्त्व - कारण से बने स्थूल पदार्थों के तत्त्व - सूक्ष्म - कारण प्रकृति महत्तत्त्वादि को आप जानते हैं और सनातन परमात्मा का जो विधान - वेद है, उसके गहन अर्थों को भी आप जानते हैं । शेष ‘अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य’ पद दोनों के साथ लग सकते हैं । वेद - परक तो इन पदों की सबने व्याख्या मानी ही है और जगत् - परक स्वयं मनु जी ने (१।५) में ‘अतक्र्यम् अविज्ञेयम्’ कहकर कर दी है । और जगत् - परक व्याख्या में वेद का भी प्रमाण है - अर्थात् यह सब जगत् सृष्टि से पहिले अन्धकार से आवृत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य ......................................................................था । और जैसे वेद जगत् का विधान है और वेद को मनुस्मृति में - मनु० १२।९४ चक्षुः - ‘चक्षिड् व्यक्तायां वाचि अयं दर्शनेऽपि’ इस धात्वर्थ के अनुसार वेद समस्त विधान को स्पष्ट तथा निभ्र्रान्त रूप से बताता है, वैसे ‘जगत्’ भी बताता है । जगत् तथा वेद क्रमशः परमेश्वर की रचना तथा ज्ञान हैं, अतः वेदान्त - दर्शन के अनुसार ‘तत्तु समन्वयात्’ वेद और जगत् में समन्वय है । ‘विष्णोः कर्माणि पश्यत’ इत्यादि वेद - प्रमाणों से स्पष्ट है कि परमात्मा की रचना को देखकर परमेश्वर का ज्ञान होता है, अतः यह जगत् भी चक्षु - परमात्मा की व्याख्या व सिद्धि करता है । और इस श्लोक के कार्यतत्त्वार्थवित् पद को भी कुल्लूकभट्टादि समझने में सर्वथा ही असमर्थ रहे हैं । उन्होंने इस पद के ‘कार्य’ शब्द का ‘अग्निष्टोमादि यज्ञ’ और ‘तत्त्व’ शब्द का ‘ब्रह्म’ अर्थ किया है । यह उनका अर्थ असंगत तथा त्रुटिपूर्ण है । उनकी व्याख्या में निम्नदोष हैं - (क) महर्षियों ने जिस विषय का प्रश्न किया था, उसी को जानने वाला मनु जी को कहना उचित है । प्रश्न तो किया गया है वर्ण व आश्रमों के धर्मों का और मनु जी के लिये विशेषण दिया जाये यज्ञ तथा ब्रह्म को जानने का, इनमें परस्पर कोई संगति नहीं है । और कार्यतत्त्व तथा वेदार्थवित् कहना इस लिये संगत है कि वेद ही सब धर्मों का मूल है । ‘धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः’ आदि कहकर मनु जी ने इसे स्पष्ट किया है । और ‘अस्य सर्वस्य कार्यतत्त्वार्थवित्’ कहकर ऋषियों ने सृष्टि - उत्पत्ति की भी परोक्षरूप में जिज्ञासा प्रकट की और मनु जी ने उसका उत्तर दिया है । (ख) ‘कार्य’ शब्द का यज्ञ तथा ‘तत्त्व’ शब्द का ब्रह्म अर्थ है, इसमें जहाँ प्रकरण से विरोध है, वहाँ इस अर्थ में कोई प्रमाण भी नहीं है । कारण से जो बने उसे कार्य कहते हैं, अथवा करणीय कर्मों को कार्य कहते हैं । यद्यपि ‘यज्ञ’ भी एक कत्र्तव्य कर्म है, किन्तु यज्ञ ही कत्र्तव्य नहीं है और नहीं इस शास्त्र में यज्ञों का ही वर्णन माना जा सकता है । यज्ञ तो एक अंग हैं, अंगी नहीं । (ग) और श्लोक - पठित ‘कार्यतत्त्व’ शब्द का पृथक् - पृथक् करके अर्थ भी विद्वदभिनन्दनीय नहीं हो सकता । क्यों कि ‘तत्त्व’ शब्द सामेक्ष है , जो ‘कार्य’ शब्द के बिना पूर्ण - अर्थ का बोधक नहीं हो सकता । और ‘कार्यतत्त्वार्थवित्’ शब्द के ‘अर्थ’ शब्द तो इनकी व्याख्या में निरर्थक ही हो जाता है । (घ) मनुस्मृति के इन कुल्लूकभट्टादि व्याख्या करने वालों पर पौराणिक भाष्यकार सायणाचार्य की मान्यता का यह प्रभाव था कि वेद यज्ञ के लिये हैं । वेदों में यज्ञों का ही प्रतिपादन है । इसलिये उन्होंने क्लिष्ट - कल्पना करके ‘कार्य’ शब्द का यज्ञ अर्थ कर दिया है । वास्तव में यह एक मिथ्या और मनुस्मृति के विरूद्ध कल्पना मात्र ही है । वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है । इसमें कतिपय मनुस्मृति के ही प्रमाण देखिये - (१।२४) श्लोक में लिखा है - वेदों से ही समस्त पदार्थों का नाम रखे गये और सब मनुष्यों के कर्मों तथा पृथक् व्यवस्थाओं का निर्धारण किया गया । (१२।९७) में चारों वर्णों, आश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से माना है । (१२।९८) शब्द, स्पशट आदि सूक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों के द्वारा मानी है । (१२।९९) में जगत् के समस्त व्यवहारों का सर्वोपरि साधक वेद को माना है । (७।४३,१२,१००) में राजनीति की शिक्षा देने वाला, (१२।१०९-११३) में धर्माधर्म का ज्ञान देने वाला, (१।२४) और (१।२१) में जगत् के श्रेष्ठ व्यवहारों का साधक वेद को माना है । (१२।९४) में पितर, देव तथा मनुष्यों को समस्त ज्ञान - विज्ञान आदि दर्शाने के कारण वेद को ‘चक्षुः’ शब्द से कहा गया है । (ड) और मनुस्मृति के इन टीकाकारों की व्याख्या प्रसंग के विरूद्ध भी है । ऋषियों ने मनु जी के पास आकर वर्णों और आश्रमों के धर्म के बारे में प्रश्न किया था । उन्हें धर्म के मूलाकरण वेदार्थवेत्ता कहना तो संगत है, यज्ञादि का वेत्ता कहना प्रसंगविरूद्ध है । प्रसंगानुकूल ही विशेषणों से विशेषित करना उचित है । और जो वेदार्थवेत्ता है, वही धर्मोपदेश करने में समर्थ हो सकता है, यह स्वयं मनु जी ने १२वें अध्याय के १०८ - ११४ श्लोंकों में कहा है । इस प्रकार कुल्लूकभट्टादि का किया अर्थ सर्वथा असंगत, युक्तिविरूद्ध, अव्यावहारिक तथा मनु जी के आशय से विरूद्ध होने से मान्य नहीं हो सकता । ३. मनुस्मृति के इन (१-४) प्रथम चार श्लोकों के विषय में भी कुछ टीकाकारों की यह भ्रान्त धारणा है कि मनुस्मृति का प्रारम्भ पांचवें श्लोक से होता है, ये प्रथम चार श्लोक भृगु अथवा किसी शिष्य के बनाये हुए हैं । यद्यपि १-४ श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की भांति मौलिक नहीं हैं, तथापि इनकी शैली, घटना और प्रश्नों के आधार पर इन्हें मौलिक मानने में संकोच नहीं करना चाहिये । क्यों कि मनु जी के किसी शिष्य ने तत्कालीन घटना तथा भावों के अनुरूप ही भूमिका के रूप में इन श्लोकों का संकलन किया है । घटना तथा प्रश्न दोनों ही यथार्थता को लिये हुए हैं । जिन शिष्यों ने सम्पूर्ण प्रवचनरूप मनुस्मृति का संकलन किया है, उन्होंने ही इन भूमिका के श्लोकों का संकलन किया है । अतः दूसरे मौलिक श्लोकों की भांति इन्हें भी संगत मानना उचित है । और इनके बिना प्रकरण की संगति भी नहीं लग पाती । और कुछ टीकाकारों ने इन चार श्लोकों की शैली के आधार पर मध्य - मध्य में किये प्रक्षिप्त - श्लोकों को भी, (जैसे - मनुरब्रवीत् ।। (८।३३९) मनुना परिकीर्तितः ।। (१।१२६) उक्तवान् मनुः ।। (१।११८) इत्यादि को मौलिक मानने का प्रयत्न किया है । किन्तु उनकी यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है । क्यों कि मनुस्मृति एक प्रवचन किया हुआ ग्रन्थ है । इसका संकलन मात्र ही शिष्यों ने किया है, किन्तु मनु के भावों को लेकर श्लोकों को नहीं बनाया गया है । संकलन में संकलयिता अपनी ओर से कुछ नहीं लिख सकता, किन्तु भावानुरूप भाषा से श्लोक बनाने में स्वंय भी कुछ लिख सकता है । यह मनुस्मृति की अन्तः साक्षी से स्पष्ट हो जाता कि मनु द्वारा प्रवचन किये श्लोकों के अनुरूप ही संकलन किया गया है । यह बात ‘श्रूयताम्’ ‘निबोधत’ आदि क्रियाओं से परिपुष्ट हो जाती है । यदि यह भावानुरूप बाद की रचना होती, तो ऐसी क्रियाओं का प्रयोग कैसे हो सकता है ? अतः मनु आदि शब्दों को लेकर अर्वाचीन श्लोकों को मौलिक सिद्ध नहीं किया जा सकता ।)
স তৈঃ পৃষ্টস্তথা সম্যগমিতোজা মহাত্মভিঃ ।
প্রত্যুবাচার্চ্য তান্ সর্বান্ মহর্ষীংশ্রূযতামিতি ।। মনু০ ১।৪
(सः) वह मनु (तैः) उनके द्वारा (पृष्ट) पूछा गया (तथा) इस प्रकार (सम्यक) भलीभाॅति (अमित ओजाः) अपार तेज बाला (महात्मभिः) महात्माओ द्वारा (प्रत्वयुवाच) उत्तर दिया (अच्र्य) सत्कार करके (तान सर्वान महर्षीन) उन सब महर्षियो का (श्रूयताम इति) सूनिये । जब इन महात्माओं ने इन महान तेजस्वी मनु जी से ऐसा प्रसन्न किया तो मनु जी ने उन सब महषियों का सत्कार करके उत्तर दिया आप सुनिये (मै कहता हूॅ)
Commentary by : पण्डित गंगा प्रसाद उपाध्याय
আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেযং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ।। মনু০ ১।৫
Commentary by: पण्डित राजवीर शास्त्री जी
-(इदम्) यह सब जगत् (तमोभूतम्) सृष्टि के पहले प्रलय में अन्धकार से आवृत्त - आच्छादित था ।................... उस समय (अविज्ञेयम्) न किसी के जानने (अप्रतक्र्यम्) न तर्क में लाने और (अलक्षणम् अप्रज्ञातम्) न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा । किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है । (स० प्र० अष्टम स०) (सर्वतः) सब ओर (प्रसुप्तम् इव) सोया हुआ - सा पड़ा था ।
ততঃ স্বযংভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জযন্নিদম্ ।
মহাভূতাদি বৃত্তোজাঃ প্রাদুরাসীত্ তমোনুদঃ ।। মনু০ ১।৬
Commentary by : पण्डित राजवीर शास्त्री जी
-(ततः) तब (स्वयम्भूः )अपने कार्यों को करने में स्वंय समर्थ, किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा न रखने वाला (अव्यक्तः) स्थूल रूप में प्रकट न होने वाला (तमोनुदः) ‘तम’ रूप प्रकृति का प्रेरक - प्रकटावस्था की ओर उन्मुख करने वाला (महाभूतादि वृत्तौजाः) अग्नि, वायु आदि महाभूतों को आदि शब्द से महत् अहंकार आदि को भी (१।१४-१५) उत्पन्न करने की महान! शक्तिवाला (भगवान्) परमात्मा (इदम्) इस समस्त संसार को (व्यंज्जयन्) प्रकटावस्था में लाते हुए ही (प्रादुरासीत्) प्रकट हुआ।
যোঽসাবতীন্দ্রিযগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ ।
সর্বভূতমযোঽচিন্ত্যঃ স এব স্বযমুদ্বভৌ ।। মনু০ ১।৭ (প্রক্ষিপ্ত শ্লোক)
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by: स्वामी दर्शनानंद जी
जो मुक्त जीव इन्द्रियों से अलग, सूक्ष्म और सदा निश्चिन्त और सब सृष्टि के प्राण हैं, वे स्वयं ही साकल्पिक शरीरों में प्रविष्ट हुए।
সোঽভিধ্যায শরীরাত্ স্বাত্ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীর্যমবাসৃজত্ ।। মনু০ ১।৮ (প্রক্ষিপ্ত শ্লোক)
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
और जब उनके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि अपने शरीर से एक प्रकार की सृष्टि पैदा करनी चाहिए तो उन्होंने सबसे प्रथम पानी अर्थात् रज को उत्पन्न किया। फिर उस पानी में बीज डाला।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ।
তস্মিঞ্জজ্ঞে স্বযং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ।। মনু০ ১।৯ (প্রক্ষিপ্ত শ্লোক)
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by: स्वामी दर्शनानंद जी
तब वह बीज स्वर्ण और सू्य्र्य के समान अष्ठाकार बन गया, फिर उससे ब्रह्माजी अर्थात् वेदों के ज्ञाता अयोनिज ऋषि जो समग्र सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, अपने आप उत्पन्न हुए।
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ ।
তা যদস্যাযনং পূর্বং তেন নারাযণঃ স্মৃতঃ ।। মনু০ ১।১০ (প্রক্ষিপ্ত শ্লোক)
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by: पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार
जीव ‘नारा’ कहलाते हैं, क्योंकि वे नर (नायक परमात्मा) से प्रेरित होने के कारण उसके सूनु अर्थात् पुत्र हैं। यतः, ये ‘नारा’ नामक जीव इस नर के प्रथम अयन अर्थात् उत्तम निवास स्थान हैं, अतः सब जीवों में व्यापक होने से परमात्मा का नाम नारायण है।१ १. नाराः जीवाः अयनं निवासस्थानं अस्य सः नारायणः जीवेषु व्यापकः। -स०प्र०, स० १
যত্ তত্ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্ ।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মৈতি কীর্ত্যতে ।। মনু০ ১।১১ (প্রক্ষিপ্ত শ্লোক)
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
Commentary by: स्वामी दर्शनानंद जी
जो परमात्मा जगत् का उपादान है और छिपा हुआ है और नित्य सत्-असत् का कत्र्ता है, उसने जिस मनुष्य को संसार में सबसे पहिले चारों वेदों का ज्ञाता उत्पन्न किया, उसी को सब लोग ’ब्रह्मा’ कहते हैं।
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् ।स्वयं एवात्मनो ध्यानात्तदण्डं अकरोद्द्विधा
তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবত্সরম্ ।
স্বযমেবাত্মনো ধ্যানাত্ তদণ্ডমকরোদ্ দ্বিধা ।। মনু০ ১।১২ (প্রক্ষিপ্ত শ্লোক)
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ।मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् ।
তাভ্যাং স শকলাভ্যাং চ দিবং ভূমিং চ নির্মমে ।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানং চ শাশ্বতম্ ।। মনু০ ১।১৩ (প্রক্ষিপ্ত শ্লোক)
यह श्लोक प्रक्षिप्त है अतः मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है
উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্ ।
মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্ ।। মনু০ ১।১৪
মহান্তমেব চাত্মানং সর্বাণি ত্রিগুণানি চ ।
বিষযাণাং গ্রহীতৄণি শনৈঃ পঞ্চৈন্দ্রিযাণি চ ।। মনু০ ১।১৫
তেষাং ত্ববযবান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্ ।
সংনিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্বভূতানি নির্মমে ।। মনু০ ১।১৬
যন্ মূর্ত্যবযবাঃ সূক্ষ্মাস্তানীমান্যাশ্রযন্তি ষট্ ।
তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্তিং মনীষিণঃ ।। মনু০ ১।১৭
তদাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্মভিঃ ।
মনশ্চাবযবৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্বভূতকৃদব্যযম্ ।। মনু০ ১।১৮
তেষামিদং তু সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাম্ ।
সূক্ষ্মাভ্যো মূর্তিমাত্রাভ্যঃ সংভবত্যব্যযাদ্ ব্যযম্ ।। মনু০ ১।১৯
আদ্যাদ্যস্য গুণং ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ ।
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্ গুণঃ স্মৃতঃ ।। মনু০ ১।২০
সর্বেষাং তু স নামানি কর্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্ ।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্মমে ।। মনু০ ১।২১
কর্মাত্মনাং চ দেবানাং সোঽসৃজত্ প্রাণিনাং প্রভুঃ ।
সাধ্যানাং চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞং চৈব সনাতনম্ ।। মনু০ ১।২২
অগ্নিবাযুরবিভ্যস্তু ত্রযং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋচ্.যজুস্.সামলক্ষণম্ ।। মনু০ ১।২৩
কালং কালবিভক্তীশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা ।
সরিতঃ সাগরান্ শৈলান্ সমানি বিষমানি চ ।। মনু০ ১।২৪
তপো বাচং রতিং চৈব কামং চ ক্রোধমেব চ ।
সৃষ্টিং সসর্জ চৈবৈমাং স্রষ্টুমিচ্ছন্নিমাঃ প্রজাঃ ।। মনু০ ১।২৫
কর্মণাং চ বিবেকার্থং ধর্মাধর্মৌ ব্যবেচযত্ ।
দ্বন্দ্বৈরযোজযচ্চৈমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ ।। মনু০ ১।২৬
অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্ধানাং তু যাঃ স্মৃতাঃ ।
তাভিঃ সার্ধমিদং সর্বং সংভবত্যনুপূর্বশঃ ।। মনু০ ১।২৭
যং তু কর্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্ক্ত প্রথমং প্রভুঃ ।
স তদেব স্বযং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।। মনু০১।২৮
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্মাধর্মাবৃতানৃতে ।
যদ্ যস্য সোঽদধাত্ সর্গে তত্ তস্য স্বযমাবিশত্ ।। মনু০১।২৯
যথর্তুলিঙ্গান্যর্তবঃ স্বযমেবর্তুপর্যযে ।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্মাণি দেহিনঃ ।। মনু০১।৩০
লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিযং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্তযত্ ।। মনু০।১।৩১
দ্বিধা কৃত্বাঽত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবত্ ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজত্ প্রভুঃ ।। মনু০১।৩২
তপস্তপ্ত্বাঽসৃজদ্ যং তু স স্বযং পুরুষো বিরাট্ ।
তং মাং বিত্তাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ ।। মনু০।১।৩৩
অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্ ।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ ।। মনু০১।৩৪
मरीचिं अत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् ।प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदं एव च
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
প্রচেতসং বসিষ্ঠং চ ভৃগুং নারদমেব চ ।। মনু০১।৩৫
Commentary by: पण्डित राजवीर शास्त्री जी
टिप्पणी :
१।३२ -४१ तक दश श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं - वर्तमान मनुस्मृति में सृष्टि - उत्पत्ति का वर्णन दो प्रकार से किया है । एक - परमात्मा ने अव्यक्त प्रकृति से सूक्ष्म से स्थूल करते - करते कारण - कार्यभाव से सृष्टि को बनाया । यह मान्यता तो सब शास्त्रों की होने से मान्य है किन्तु ब्रह्मा से उत्पत्ति मौलिक नहीं हो सकती । क्यों कि प्रथम तो दोनों में परस्पर विरोध है, और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम मेल नहीं खाता । ब्रह्मा से उत्पत्ति का वर्णन कल्पना पर आश्रित होने से अविश्वसनीय है, जैसे ब्रह्मा के आधे देह से १।३२ मे पुरूष और आधे देह से नारी की उत्पत्ति लिखी है । और इन श्लोकों की संगति पूर्वापर श्लोकों के क्रम को भंग करने से नहीं लगती । जैसे १।३१ श्लोक तथा उससे पूर्व श्लोकों में कर्मानुसार वर्णन किया है और १।४२ वें श्लोक में भी वही क्रम चल रहा है । अतः इनके मध्य के ये श्लोक अप्रासंगिक हैं । १।१४-२३ श्लोकों में जगदुत्पत्ति का वर्णन पूर्ण होने से पुनः स्थावर - जंगम जगत् की उत्पत्ति ब्रह्मा से दिखलाना स्पष्ट ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करता है । और १।३२-४१ श्लोकों को मानने में अन्तर्विरोध भी है । १।७-१३ में परमात्मा को सृष्टि - कर्ता माना है, अब ब्रह्मा से मान कर १।३४-४१ श्लोकों में दशप्रजापतियों को सृष्टि - कर्ता माना है । एक लेखक की पुस्तक में ऐसा पारस्परिक विरोध कदापि नहीं हो सकता । और १।३५-४१ श्लोकों में दश प्रजापतियों से सात मनु उत्पन्न हुए, और उन्होंने स्थावर - जंगम जगत् बनाया । क्या यह समस्त जगत् ऋषि बना सकते हैं ? और सप्त मनुओं ने यक्ष, पिशाच, नाग, सर्प, वानर, मृग, कृमि, कीट, पतंगादि को बनाया, यह कथन तो आश्चर्यजनक ही है ।
এতে মনূংস্তু সপ্তান্ যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ ।
দেবান্ দেবনিকাযাংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতোজসঃ ।। মনু০১।৩৬
যক্ষরক্ষঃ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরান্ ।
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৄণাংশ্চ পৃথগ্গণম্ ।। মনু০১।৩৭
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতৈন্দ্রধনূংষি চ ।
উল্কানির্ঘাতকেতূংশ্চ জ্যোতীংষ্যুচ্চাবচানি চ ।। মনু০১।৩৮
কিন্নরান্ বানরান্ মত্স্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্ ।
পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভযতোদতঃ ।। মনু০১।৩৯
কৃমিকীটপতঙ্গাংশ্চ যূকামক্ষিকমত্কুণম্ ।
সর্বং চ দংশমশকং স্থাবরং চ পৃথগ্বিধম্ ।। মনু০১।৪০
এবমেতৈরিদং সর্বং মন্নিযোগান্ মহাত্মভিঃ ।
যথাকর্ম তপোযোগাত্ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্ ।। মনু০১।৪১
যেষাং তু যাদৃশং কর্ম ভূতানামিহ কীর্তিতম্ ।
তত্ তথা বোঽভিধাস্যামি ক্রমযোগং চ জন্মনি ।। মনু০১।৪২
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভযতোদতঃ ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরাযুজাঃ ।। মনু০১।৪৩
অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মত্স্যাশ্চ কচ্ছপাঃ ।
যানি চৈবং.প্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানি চ ।। মনু০১।৪৪
স্বেদজং দংশমশকং যূকামক্ষিকমত্কুণম্ ।
ঊষ্মণশ্চোপজাযন্তে যচ্চান্যত্ কিং চিদীদৃশম্ ।। মনু০১।৪৫
উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ ।। মনু০১।৪৬
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতযঃ স্মৃতাঃ ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভযতঃ স্মৃতাঃ ।। মনু০১।৪৭
গুচ্ছগুল্মং তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতযঃ ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ ।। মনু০১।৪৮
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা ।
অন্তস্সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ।। মনু০১।৪৯
এতদন্তাস্তু গতযো ব্রহ্মাদ্যাঃ সমুদাহৃতাঃ ।
ঘোরেঽস্মিন্ ভূতসংসারে নিত্যং সততযাযিনি ।। মনু০১।৫০
এবং সর্বং স সৃষ্ট্বৈদং মাং চাচিন্ত্যপরাক্রমঃ ।
আত্মন্যন্তর্দধে ভূযঃ কালং কালেন পীডযন্ ।। মনু০১।৫১
যদা স দেবো জাগর্তি তদেবং চেষ্টতে জগত্ ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্বং নিমীলতি ।। মনু০১।৫২
তস্মিন্ স্বপিতি তু স্বস্থে কর্মাত্মানঃ শরীরিণঃ ।
স্বকর্মভ্যো নিবর্তন্তে মনশ্চ গ্লানিমৃচ্ছতি ।। মনু০১।৫৩
যুগপত্ তু প্রলীযন্তে যদা তস্মিন্ মহাত্মনি ।
তদাঽযং সর্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ ।। মনু০১।৫৪
তমোঽযং তু সমাশ্রিত্য চিরং তিষ্ঠতি সৈন্দ্রিযঃ ।
ন চ স্বং কুরুতে কর্ম তদোত্ক্রামতি মূর্তিতঃ ।। মনু০১।৫৫
যদাঽণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাণু চরিষ্ণু চ ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্তিং বিমুঞ্চতি ।। মনু০১।৫৬
এবং স জাগ্রত্স্বপ্নাভ্যামিদং সর্বং চরাচরম্ ।
সঞ্জীবযতি চাজস্রং প্রমাপযতি চাব্যযঃ ।। মনু০১।৫৭
ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাঽসৌ মামেব স্বযমাদিতঃ ।
বিধিবদ্ গ্রাহযামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্ ।। মনু০১।৫৮
এতদ্ বোঽযং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবযিষ্যত্যশেষতঃ ।
এতদ্ হি মত্তোঽধিজগে সর্বমেষোঽখিলং মুনিঃ ।। মনু০১।৫৯
ততস্তথা স তেনোক্তো মহর্ষিমনুনা ভৃগুঃ ।
তানব্রবীদ্ ঋষীন্ সর্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূযতামিতি ।। মনু০১।৬০
স্বাযংভুবস্যাস্য মনোঃ ষড্বংশ্যা মনবোঽপরে ।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ ।। মনু০১।৬১
স্বারোচিষশ্চোত্তমশ্চ তামসো রৈবতস্তথা ।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বত্সুত এব চ ।। মনু০১।৬২
স্বাযংভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরিতেজসঃ ।
স্বে স্বেঽন্তরে সর্বমিদমুত্পাদ্যাপুশ্চরাচরম্ ।। মনু০১।৬৩
নিমেষা দশ চাষ্টৌ চ কাষ্ঠা ত্রিংশত্ তু তাঃ কলা ।
ত্রিংশত্ কলা মুহূর্তঃ স্যাদহোরাত্রং তু তাবতঃ ।। মনু০১।৬৪
অহোরাত্রে বিভজতে সূর্যো মানুষদৈবিকে ।
রাত্রিঃ স্বপ্নায ভূতানাং চেষ্টাযৈ কর্মণামহঃ ।। মনু০১।৬৫
পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষযোঃ ।
কর্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায শর্বরী ।। মনু০১।৬৬
দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তযোঃ পুনঃ ।
অহস্তত্রোদগযনং রাত্রিঃ স্যাদ্ দক্ষিণাযনম্ ।। মনু০১।৬৭
ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যত্ প্রমাণং সমাসতঃ ।
একৈকশো যুগানাং তু ক্রমশস্তন্নিবোধত ।। মনু০১।৬৮
চত্বার্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তত্ কৃতং যুগম্ ।
তস্য তাবত্শতী সংধ্যা সংধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ।। মনু০১।৬৯
ইতরেষু সসংধ্যেষু সসংধ্যাংশেষু চ ত্রিষু ।
একাপাযেন বর্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ।। মনু০১।৭০
যদেতত্ পরিসঙ্খ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগম্ ।
এতদ্ দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ।। মনু০১।৭১
দৈবিকানাং যুগানাং তু সহস্রং পরিসঙ্খ্যযা ।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেযং তাবতীং রাত্রিমেব চ ।। মনু০১।৭২
তদ্ বৈ যুগসহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ ।
রাত্রিং চ তাবতীমেব তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ।। মনু০১।৭৩
তস্য সোঽহর্নিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে ।
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকম্ ।। মনু০১।৭৪
মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষযা ।
আকাশং জাযতে তস্মাত্ তস্য শব্দং গুণং বিদুঃ ।। মনু০১।৭৫
আকাশাত্ তু বিকুর্বাণাত্ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ ।
বলবাঞ্জাযতে বাযুঃ স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ ।। মনু০১।৭৬
বাযোরপি বিকুর্বাণাদ্ বিরোচিষ্ণু তমোনুদম্ ।
জ্যোতিরুত্পদ্যতে ভাস্বত্ তদ্ রূপগুণমুচ্যতে ।। মনু০১।৭৭
জ্যোতিষশ্চ বিকুর্বাণাদাপো রসগুণাঃ স্মৃতাঃ ।
অদ্ভ্যো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ ।। মনু০১।৭৮
যদ্ প্রাগ্ দ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগম্ ।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ।। মনু০১।৭৯
মন্বন্তরাণ্যসঙ্খ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ ।
ক্রীডন্নিবৈতত্ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ ।। মনু০১।৮০
চতুষ্পাত্ সকলো ধর্মঃ সত্যং চৈব কৃতে যুগে ।
নাধর্মেণাগমঃ কশ্চিন্ মনুষ্যান্ প্রতি বর্ততে ।। মনু০১।৮১
ইতরেষ্বাগমাদ্ ধর্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ ।
চৌরিকানৃতমাযাভির্ধর্মশ্চাপৈতি পাদশঃ ।। মনু০১।৮২
অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্বর্ষশতাযুষঃ ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামাযুর্হ্রসতি পাদশঃ ।। মনু০১।৮৩
বেদোক্তমাযুর্মর্ত্যানামাশিষশ্চৈব কর্মণাম্ ।
ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাম্ ।। মনু০১।৮৪
অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতাযাং দ্বাপরেঽপরে ।
অন্যে কলিযুগে নৄণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ।। মনু০১।৮৫
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতাযাং জ্ঞানমুচ্যতে ।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ।। মনু০১।৮৬
সর্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহুরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্মাণ্যকল্পয়ৎ।। মনু০ ১।৮৭
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।। মনু০ ১/৮৮
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েম্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।। মনু০ ১/৮৯
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।। মনু০ ১/৯০
এতমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।। মনু০১।৯১
ঊর্ধ্বং নাভের্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্তিতঃ ।
তস্মান্ মেধ্যতমং ত্বস্য মুখমুক্তং স্বযংভুবা ।। মনু০ ১।৯২
উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্ জ্যেষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাত্ ।
সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ।। মনু০ ১।৯৩
তং হি স্বযংভূঃ স্বাদাস্যাত্ তপস্তপ্ত্বাঽদিতোঽসৃজত্ ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায সর্বস্যাস্য চ গুপ্তযে ।। মনু০ ১।৯৪
যস্যাস্যেন সদাঽশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিং ভূতমধিকং ততঃ ।। মনু০ ১।৯৫
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ ।
বুদ্ধিমত্সু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ।। মনু০ ১।৯৬
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বত্সু কৃতবুদ্ধযঃ ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ।। মনু০১।৯৭
উত্পত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্তির্ধর্মস্য শাশ্বতী ।
স হি ধর্মার্থমুত্পন্নো ব্রহ্মভূযায কল্পতে ।। মনু০ ১।৯৮
ব্রাহ্মণো জাযমানো হি পৃথিব্যামধিজাযতে ।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোশস্য গুপ্তযে ।। মনু০ ১/৯৯
সর্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যত্ কিং চিত্জগতীগতম্ ।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি ।। মনু০ ১/১০০
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ ।। মনু০ ১/১০১
তস্য কর্মবিবেকার্থং শেষাণামনুপূর্বশঃ ।
স্বাযংভুবো মনুর্ধীমানিদং শাস্ত্রমকল্পযত্ ।। মনু০ ১।১০২
বিদুষা ব্রাহ্মণেনৈদমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ ।
শিশ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যগ্ নান্যেন কেন চিত্ ।। মনু০১।১০৩
ইদং শাস্ত্রমধীযানো ব্রাহ্মণঃ শংসিতব্রতঃ ।
মনোবাক্দেহজৈর্নিত্যং কর্মদোষৈর্ন লিপ্যতে ।। মনু০১।১০৪
পুনাতি পঙ্ক্তিং বংশ্যাংশ্চ ? ? সপ্তসপ্ত পরাবরান্ ।
পৃথিবীমপি চৈবেমাং কৃত্স্নামেকোঽপি সোঽর্হতি ।। মনু০১।১০৫
ইদং স্বস্ত্যযনং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধিবিবর্ধনম্ ।
ইদং যশস্যমাযুষ্যং ইদং নিঃশ্রেযসং পরম্ ।। মনু০১।১০৬
অস্মিন্ ধর্মেঽখিলেনোক্তৌ গুণদোষৌ চ কর্মণাম্ ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শাশ্বতঃ ।। মনু০১।১০৭
আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যোক্তঃ স্মার্ত এব চ ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ।। মনু০১।১০৮
আচারাদ্ বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে ।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেত্ ।। মনু০১।১০৯
এবমাচারতো দৃষ্ট্বা ধর্মস্য মুনযো গতিম্ ।
সর্বস্য তপসো মূলমাচারং জগৃহুঃ পরম্ ।। মনু০১।১১০
জগতশ্চ সমুত্পত্তিং সংস্কারবিধিমেব চ ।
ব্রতচর্যৌপচারং চ স্নানস্য চ পরং বিধিম্ ।। মনু০১।১১১
দারাধিগমনং চৈব বিবাহানাং চ লক্ষণম্ ।
মহাযজ্ঞবিধানং চ শ্রাদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্ ।। মনু০১।১১২
বৃত্তীনাং লক্ষণং চৈব স্নাতকস্য ব্রতানি চ ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যং চ শৌচং চ দ্রব্যাণাং শুদ্ধিমেব চ ।। মনু০১।১১৩
স্ত্রীধর্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সংন্যাসমেব চ ।
রাজ্ঞশ্চ ধর্মমখিলং কার্যাণাং চ বিনির্ণযম্ ।। মনু০১।১১৪
সাক্ষিপ্রশ্নবিধানং চ ধর্মং স্ত্রীপুংসযোরপি ।
বিভাগধর্মং দ্যূতং চ কণ্টকানাং চ শোধনম্ ।। মনু০১।১১৫
বৈশ্যশূদ্রোপচারং চ সঙ্কীর্ণানাং চ সংভবম্ ।
আপদ্ধর্মং চ বর্ণানাং প্রাযশ্চিত্তবিধিং তথা ।। মনু০ ১।১১৬
সংসারগমনং চৈব ত্রিবিধং কর্মসংভবম্ ।
নিঃশ্রেযসং কর্মণাং চ গুণদোষপরীক্ষণম্ ।। মনু০ ১।১১৭
দেশধর্মান্জাতিধর্মান্ কুলধর্মাংশ্চ শাশ্বতান্ ।
পাষণ্ডগণধর্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ ।। মনু০ ১।১১৮
যথৈদমুক্তবাংশাস্ত্রং পুরা পৃষ্টো মনুর্মযা ।
তথৈদং যূযমপ্যদ্য মত্সকাশান্নিবোধত ।। মনু০ ১।১১৯ (প্রক্ষিপ্ত)


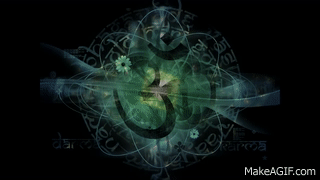




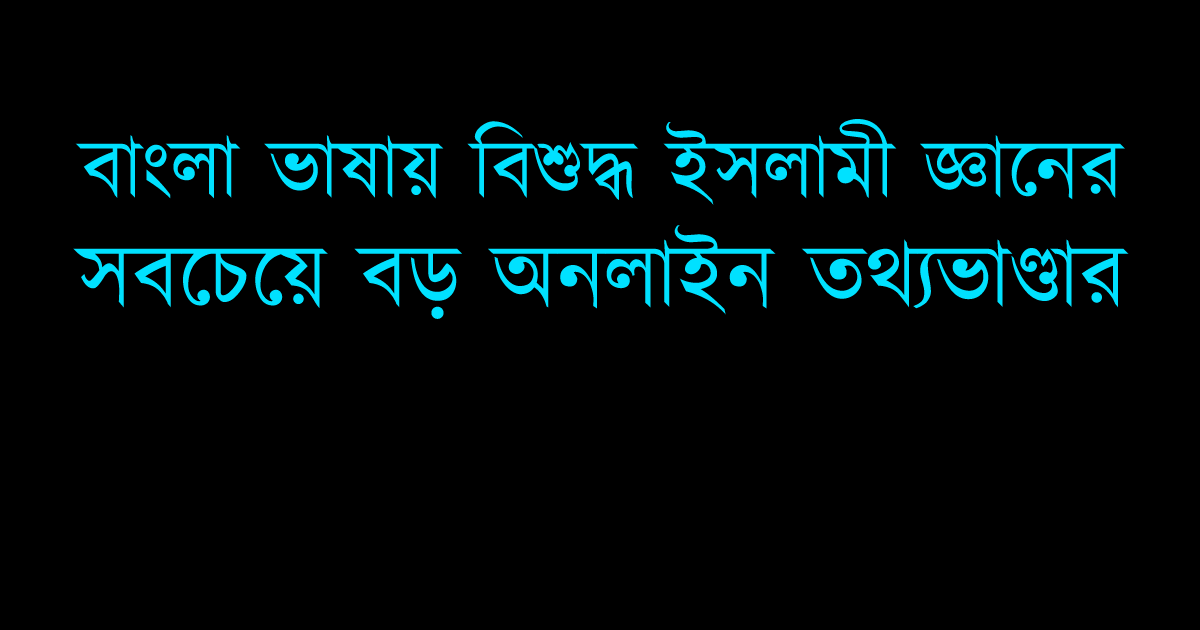
















No comments:
Post a Comment
ধন্যবাদ